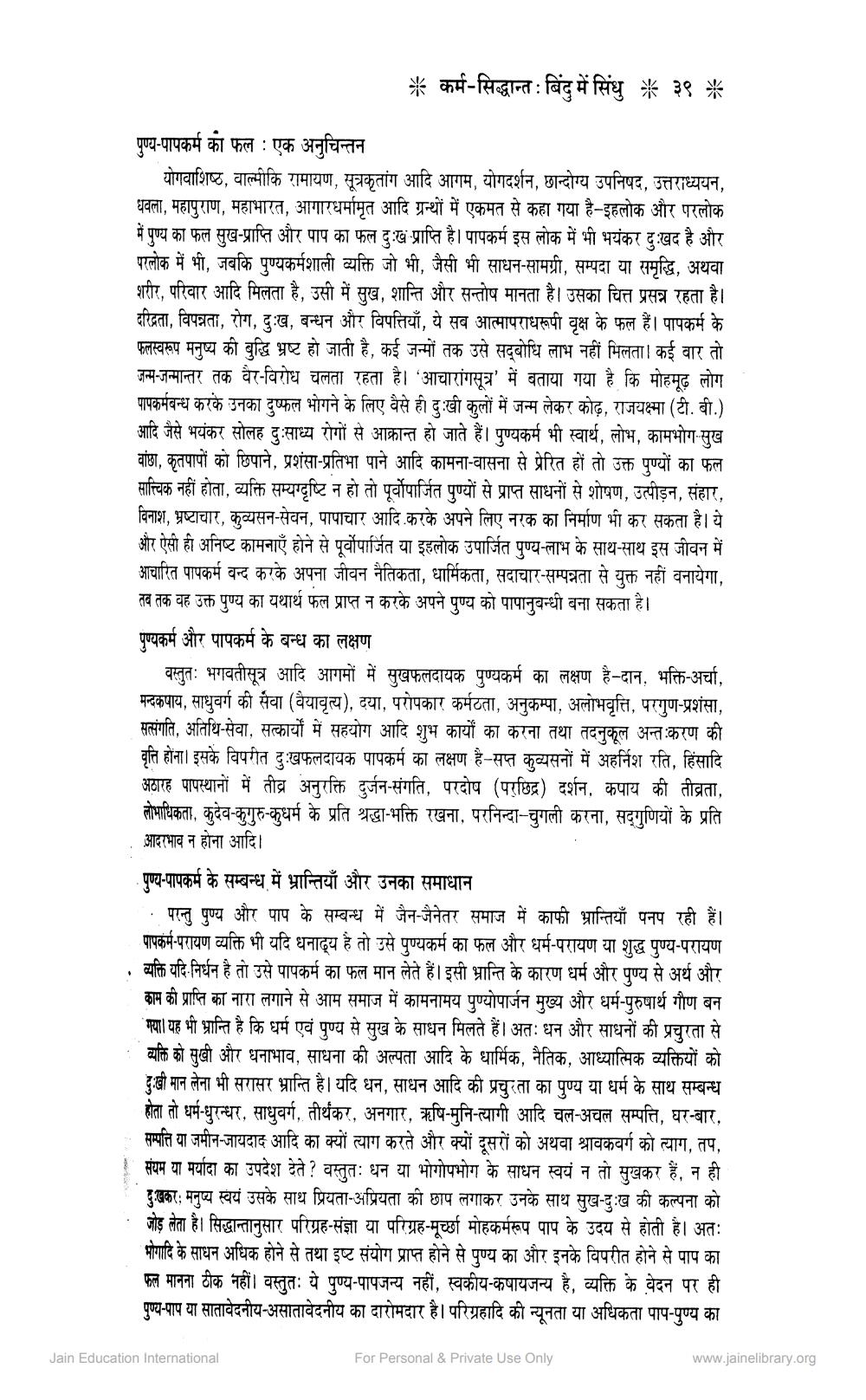________________
* कर्म-सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु * ३९ *
पुण्य-पापकर्म का फल : एक अनुचिन्तन
योगवाशिष्ठ, वाल्मीकि रामायण, सूत्रकृतांग आदि आगम, योगदर्शन, छान्दोग्य उपनिषद, उत्तराध्ययन, धवला, महापुराण, महाभारत, आगारधर्मामृत आदि ग्रन्थों में एकमत से कहा गया है-इहलोक और परलोक में पुण्य का फल सुख-प्राप्ति और पाप का फल दुःख प्राप्ति है। पापकर्म इस लोक में भी भयंकर दुःखद है और परलोक में भी, जबकि पुण्यकर्मशाली व्यक्ति जो भी, जैसी भी साधन-सामग्री, सम्पदा या समृद्धि, अथवा शरीर, परिवार आदि मिलता है, उसी में सुख, शान्ति और सन्तोष मानता है। उसका चित्त प्रसन्न रहता है। दरिद्रता, विपन्नता, रोग, दुःख, बन्धन और विपत्तियाँ, ये सब आत्मापराधरूपी वृक्ष के फल हैं। पापकर्म के फलस्वरूप मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कई जन्मों तक उसे सद्बोधि लाभ नहीं मिलता। कई वार तो जन्म-जन्मान्तर तक वैर-विरोध चलता रहता है। 'आचारांगसत्र' में बताया गया है कि मोहमढ लोग पापकर्मबन्ध करके उनका दुष्फल भोगने के लिए वैसे ही दःखी कलों में जन्म लेकर कोढ. राजयक्ष्मा (टी. बी.) आदि जैसे भयंकर सोलह दुःसाध्य रोगों से आक्रान्त हो जाते हैं। पुण्यकर्म भी स्वार्थ. लोभ. कामभोग-सख वांछा, कृतपापों को छिपाने, प्रशंसा-प्रतिभा पाने आदि कामना-वासना से प्रेरित हों तो उक्त पुण्यों का फल सात्त्विक नहीं होता, व्यक्ति सम्यग्दृष्टि न हो तो पूर्वोपार्जित पुण्यों से प्राप्त साधनों से शोषण, उत्पीड़न, संहार, विनाश, भ्रष्टाचार, कुव्यसन-सेवन, पापाचार आदि करके अपने लिए नरक का निर्माण भी कर सकता है। ये और ऐसी ही अनिष्ट कामनाएँ होने से पूर्वोपार्जित या इहलोक उपार्जित पुण्य-लाभ के साथ-साथ इस जीवन में आचारित पापकर्म बन्द करके अपना जीवन नैतिकता, धार्मिकता, सदाचार-सम्पन्नता से युक्त नहीं बनायेगा.
तब तक वह उक्त पुण्य का यथाथ फल प्राप्त न करके अपने पुण्य का पापानुबन्धा बना सकता है।
पुण्यकर्म और पापकर्म के बन्ध का लक्षण
वस्तुतः भगवतीसूत्र आदि आगमों में सुखफलदायक पुण्यकर्म का लक्षण है-दान, भक्ति-अर्चा, मन्दकपाय, साधुवर्ग की सेवा (वैयावृत्य), दया, परोपकार कर्मठता, अनुकम्पा, अलोभवृत्ति, परगुण-प्रशंसा, सत्संगति, अतिथि-सेवा, सत्कार्यों में सहयोग आदि शुभ कार्यों का करना तथा तदनुकूल अन्तःकरण की वृत्ति होना। इसके विपरीत दुःखफलदायक पापकर्म का लक्षण है-सप्त कुव्यसनों में अहर्निश रति, हिंसादि अठारह पापस्थानों में तीव्र अनुरक्ति दुर्जन-संगति, परदोष (पछिद्र) दर्शन, कपाय की तीव्रता, लोभाधिकता, कुदेव-कुगुरु-कुधर्म के प्रति श्रद्धा-भक्ति रखना, परनिन्दा-चुगली करना, सद्गुणियों के प्रति आदरभाव न होना आदि। पुण्य-पापकर्म के सम्बन्ध में भ्रान्तियाँ और उनका समाधान
. परन्तु पुण्य और पाप के सम्बन्ध में जैन-जैनेतर समाज में काफी भ्रान्तियाँ पनप रही हैं। पापकर्म-परायण व्यक्ति भी यदि धनाढ्य है तो उसे पुण्यकर्म का फल और धर्म-परायण या शुद्ध पुण्य-परायण • व्यक्ति यदि-निर्धन है तो उसे पापकर्म का फल मान लेते हैं। इसी भ्रान्ति के कारण धर्म और पुण्य से अर्थ और काम की प्राप्ति का नारा लगाने से आम समाज में कामनामय पुण्योपार्जन मुख्य और धर्म-पुरुषार्थ गौण बन गया। यह भी भ्रान्ति है कि धर्म एवं पुण्य से सुख के साधन मिलते हैं। अतः धन और साधनों की प्रचुरता से व्यक्ति को सुखी और धनाभाव, साधना की अल्पता आदि के धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक व्यक्तियों को दुःखी मान लेना भी सरासर भ्रान्ति है। यदि धन, साधन आदि की प्रचुरता का पुण्य या धर्म के साथ सम्बन्ध होता तो धर्म-धुरन्धर, साधुवर्ग, तीर्थंकर, अनगार, ऋषि-मुनि-त्यागी आदि चल-अचल सम्पत्ति, घर-बार,
सम्पत्ति या जमीन-जायदाद आदि का क्यों त्याग करते और क्यों दूसरों को अथवा श्रावकवर्ग को त्याग, तप, । संयम या मर्यादा का उपदेश देते ? वस्तुतः धन या भोगोपभोग के साधन स्वयं न तो सुखकर हैं, न ही
दुःखकर; मनुष्य स्वयं उसके साथ प्रियता-अप्रियता की छाप लगाकर उनके साथ सुख-दुःख की कल्पना को जोड़ लेता है। सिद्धान्तानुसार परिग्रह-संज्ञा या परिग्रह-मूर्छा मोहकर्मरूप पाप के उदय से होती है। अतः भोगादि के साधन अधिक होने से तथा इष्ट संयोग प्राप्त होने से पुण्य का और इनके विपरीत होने से पाप का फल मानना ठीक नहीं। वस्तुतः ये पुण्य-पापजन्य नहीं, स्वकीय-कषायजन्य है, व्यक्ति के वेदन पर ही पुण्य-पाप या सातावेदनीय-असातावेदनीय का दारोमदार है। परिग्रहादि की न्यूनता या अधिकता पाप-पुण्य का
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org