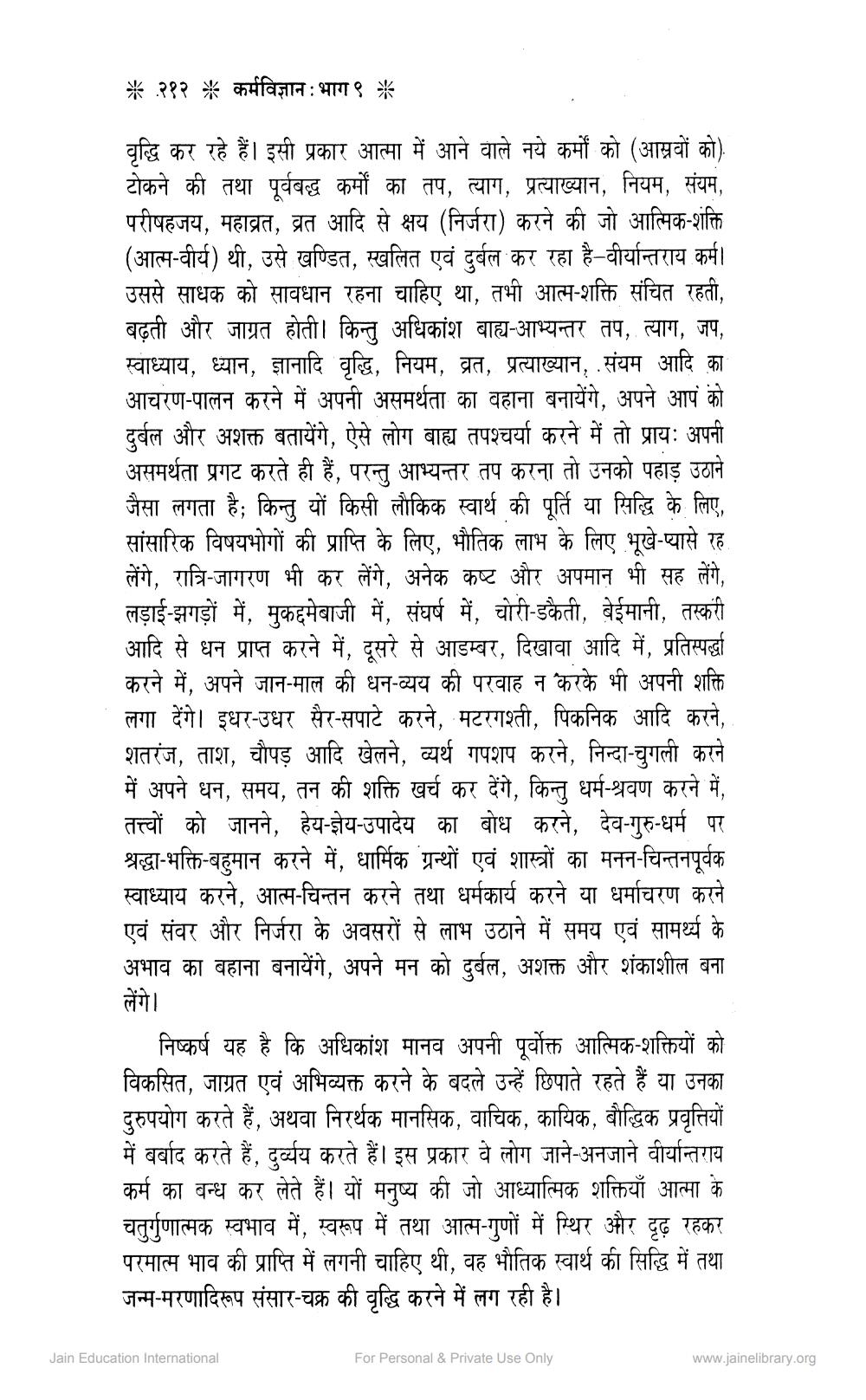________________
* २१२ * कर्मविज्ञान : भाग ९ *
वृद्धि कर रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा में आने वाले नये कर्मों को (आम्रवों को ) टोकने की तथा पूर्वबद्ध कर्मों का तप, त्याग, प्रत्याख्यान, नियम, संयम, परीषहजय, महाव्रत, व्रत आदि से क्षय (निर्जरा) करने की जो आत्मिक शक्ति ( आत्म-वीर्य) थी, उसे खण्डित, स्खलित एवं दुर्बल कर रहा है - वीर्यान्तराय कर्म । उससे साधक को सावधान रहना चाहिए था, तभी आत्म-शक्ति संचित रहती, बढ़ती और जाग्रत होती । किन्तु अधिकांश बाह्य - आभ्यन्तर तप, त्याग, जप, स्वाध्याय, ध्यान, ज्ञानादि वृद्धि, नियम, व्रत, प्रत्याख्यान, संयम आदि का आचरण- पालन करने में अपनी असमर्थता का बहाना बनायेंगे, अपने आप को दुर्बल और अशक्त बतायेंगे, ऐसे लोग बाह्य तपश्चर्या करने में तो प्रायः अपनी असमर्थता प्रगट करते ही हैं, परन्तु आभ्यन्तर तप करना तो उनको पहाड़ उठाने जैसा लगता है; किन्तु यों किसी लौकिक स्वार्थ की पूर्ति या सिद्धि के लिए, सांसारिक विषयभोगों की प्राप्ति के लिए, भौतिक लाभ के लिए भूखे-प्यासे रह. लेंगे, रात्रि जागरण भी कर लेंगे, अनेक कष्ट और अपमान भी सह लेंगे, लड़ाई-झगड़ों में, मुकद्दमेबाजी में, संघर्ष में, चोरी-डकैती, बेईमानी, तस्करी आदि से धन प्राप्त करने में, दूसरे से आडम्बर, दिखावा आदि में, प्रतिस्पर्द्धा करने में, अपने जान-माल की धन-व्यय की परवाह न करके भी अपनी शक्ति लगा देंगे। इधर-उधर सैर-सपाटे करने, मटरगश्ती, पिकनिक आदि करने, शतरंज, ताश, चौपड़ आदि खेलने, व्यर्थ गपशप करने, निन्दा - चुगली करने में अपने धन, समय, तन की शक्ति खर्च कर देंगे, किन्तु धर्म-श्रवण करने में, तत्त्वों को जानने, हेय- ज्ञेय - उपादेय का बोध करने, देव-गुरु-धर्म पर -भक्ति- क- बहुमान करने में, धार्मिक ग्रन्थों एवं शास्त्रों का मनन- चिन्तनपूर्वक स्वाध्याय करने, आत्म-चिन्तन करने तथा धर्मकार्य करने या धर्माचरण करने एवं संवर और निर्जरा के अवसरों से लाभ उठाने में समय एवं सामर्थ्य के अभाव का बहाना बनायेंगे, अपने मन को दुर्बल, अशक्त और शंकाशील बना लेंगे।
श्रद्धा-भ
निष्कर्ष यह है कि अधिकांश मानव अपनी पूर्वोक्त आत्मिक शक्तियों को विकसित, जाग्रत एवं अभिव्यक्त करने के बदले उन्हें छिपाते रहते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं, अथवा निरर्थक मानसिक, वाचिक, कायिक, बौद्धिक प्रवृत्तियों में बर्बाद करते हैं, दुर्व्यय करते हैं। इस प्रकार वे लोग जाने-अनजाने वीर्यान्तराय कर्म का बन्ध कर लेते हैं। यों मनुष्य की जो आध्यात्मिक शक्तियाँ आत्मा के चतुर्गुणात्मक स्वभाव में, स्वरूप में तथा आत्म- गुणों में स्थिर और दृढ़ रहकर परमात्म भाव की प्राप्ति में लगनी चाहिए थी, वह भौतिक स्वार्थ की सिद्धि में तथा जन्म-मरणादिरूप संसार-चक्र की वृद्धि करने में लग रही है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org