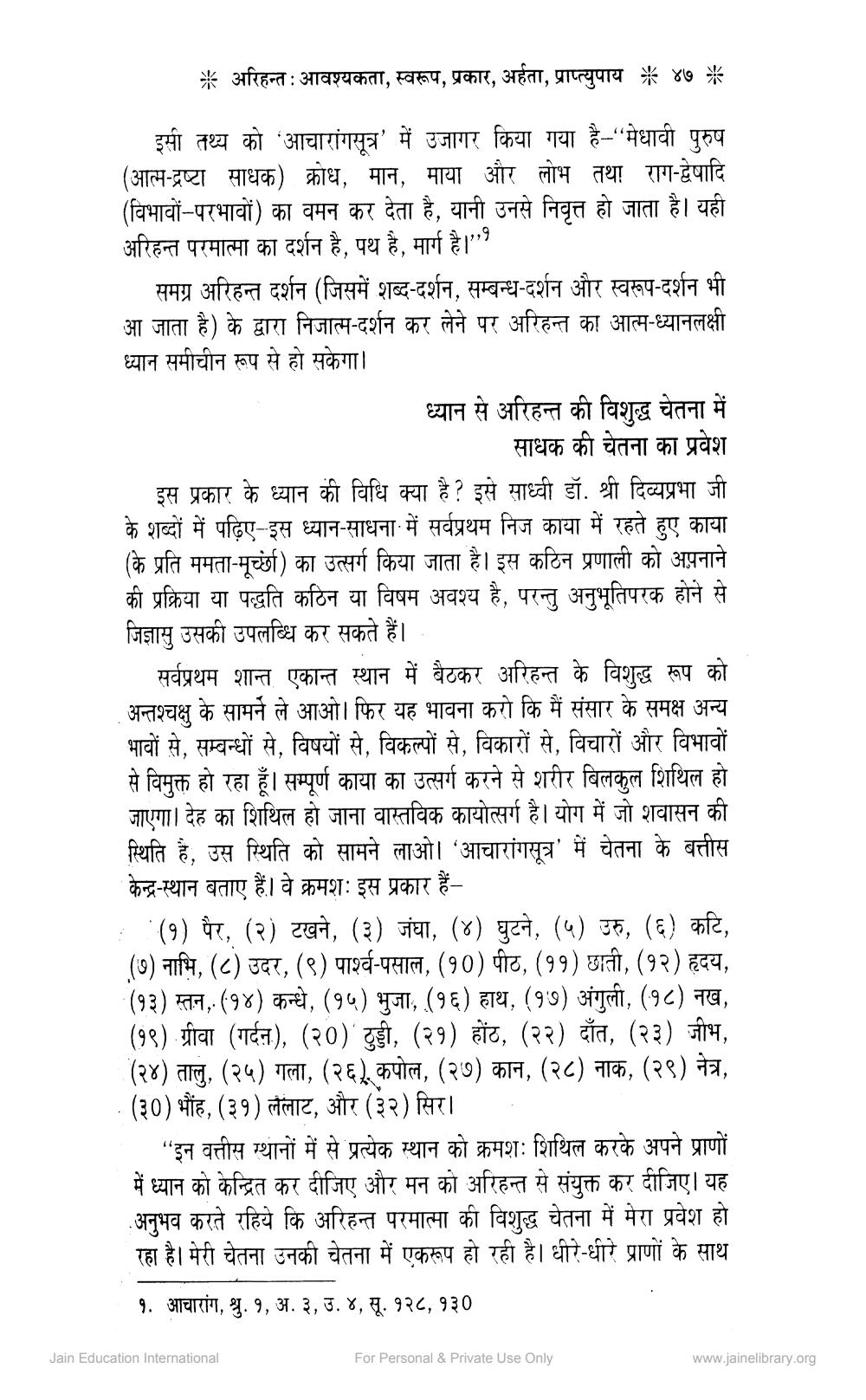________________
* अरिहन्त : आवश्यकता, स्वरूप, प्रकार, अर्हता, प्राप्त्युपाय * ४७ *
इसी तथ्य को ‘आचारांगसूत्र' में उजागर किया गया है-“मेधावी पुरुष (आत्म-द्रष्टा साधक) क्रोध, मान, माया और लोभ तथा राग-द्वेषादि (विभावों-परभावों) का वमन कर देता है, यानी उनसे निवृत्त हो जाता है। यही अरिहन्त परमात्मा का दर्शन है, पथ है, मार्ग है।''
समग्र अरिहन्त दर्शन (जिसमें शब्द-दर्शन, सम्बन्ध-दर्शन और स्वरूप-दर्शन भी आ जाता है) के द्वारा निजात्म-दर्शन कर लेने पर अरिहन्त का आत्म-ध्यानलक्षी ध्यान समीचीन रूप से हो सकेगा।
ध्यान से अरिहन्त की विशुद्ध चेतना में
साधक की चेतना का प्रवेश इस प्रकार के ध्यान की विधि क्या है ? इसे साध्वी डॉ. श्री दिव्यप्रभा जी के शब्दों में पढ़िए-इस ध्यान-साधना में सर्वप्रथम निज काया में रहते हुए काया (के प्रति ममता-मा) का उत्सर्ग किया जाता है। इस कठिन प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया या पद्धति कठिन या विषम अवश्य है, परन्तु अनुभूतिपरक होने से जिज्ञासु उसकी उपलब्धि कर सकते हैं।
सर्वप्रथम शान्त एकान्त स्थान में बैठकर अरिहन्त के विशुद्ध रूप को अन्तश्चक्षु के सामने ले आओ। फिर यह भावना करो कि मैं संसार के समक्ष अन्य भावों से, सम्बन्धों से, विषयों से, विकल्पों से, विकारों से, विचारों और विभावों से विमुक्त हो रहा हूँ। सम्पूर्ण काया का उत्सर्ग करने से शरीर बिलकुल शिथिल हो जाएगा। देह का शिथिल हो जाना वास्तविक कायोत्सर्ग है। योग में जो शवासन की स्थिति है, उस स्थिति को सामने लाओ। 'आचारांगसूत्र' में चेतना के बत्तीस केन्द्र-स्थान बताए हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं
(१) पैर, (२) टखने, (३) जंघा, (४) घुटने, (५) उरु, (६) कटि, (७) नाभि, (८) उदर, (९) पार्श्व-पसाल, (१०) पीठ, (११) छाती, (१२) हृदय, (१३) स्तन, (१४) कन्धे, (१५) भुजा, (१६) हाथ, (१७) अंगुली, (१८) नख, (१९) ग्रीवा (गर्दन), (२०) ठुड्डी, (२१) होंठ, (२२) दाँत, (२३) जीभ, (२४) तालु, (२५) गला, (२६). कपोल, (२७) कान, (२८) नाक, (२९) नेत्र, (३०) भौंह, (३१) ललाट, और (३२) सिर।। ___ "इन वत्तीस स्थानों में से प्रत्येक स्थान को क्रमशः शिथिल करके अपने प्राणों में ध्यान को केन्द्रित कर दीजिए और मन को अरिहन्त से संयुक्त कर दीजिए। यह अनुभव करते रहिये कि अरिहन्त परमात्मा की विशुद्ध चेतना में मेरा प्रवेश हो रहा है। मेरी चेतना उनकी चेतना में एकरूप हो रही है। धीरे-धीरे प्राणों के साथ
१. आचारांग, श्रु. १, अ. ३, उ. ४, सू. १२८, १३०
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org