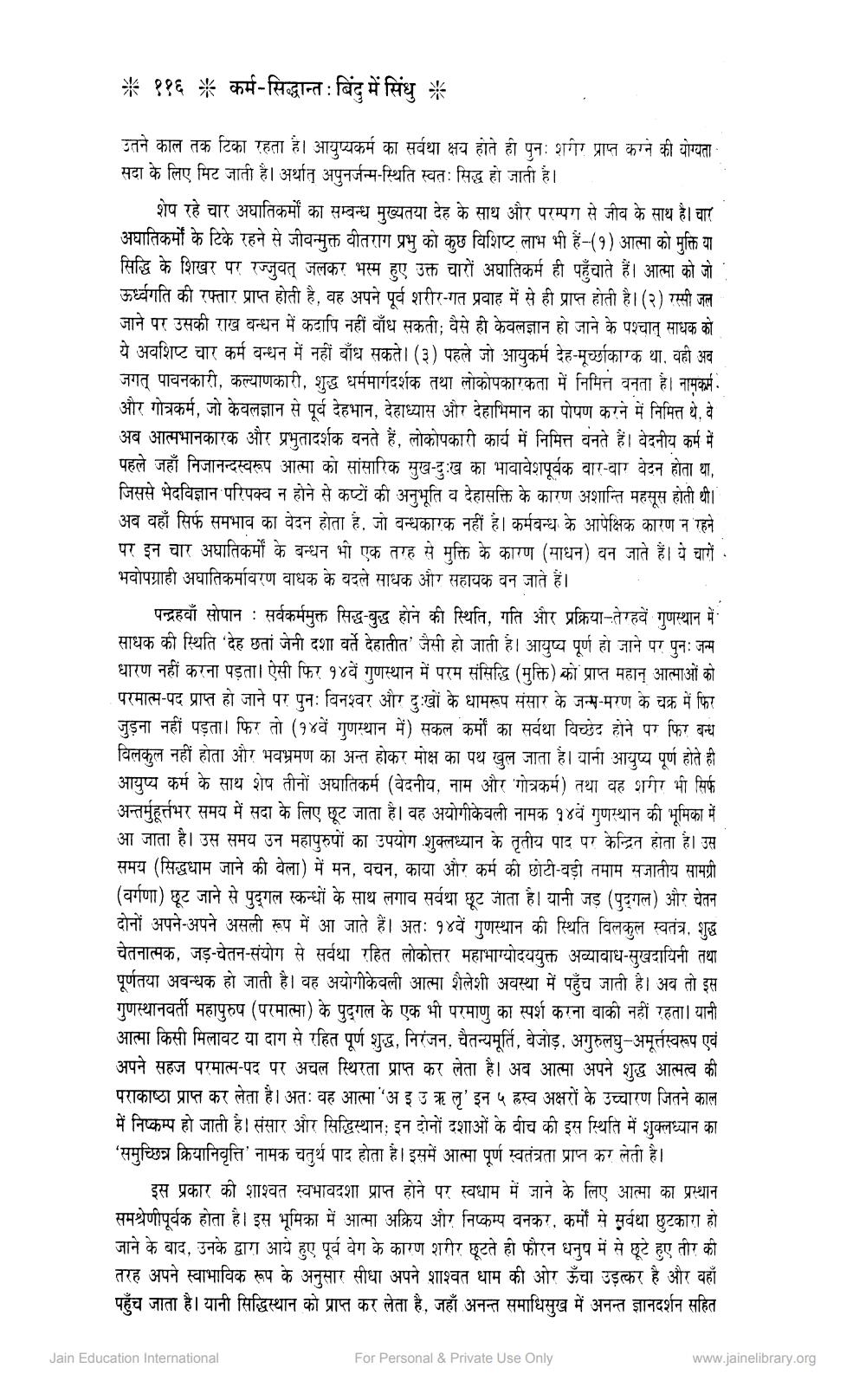________________
* ११६ * कर्म-सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु *
उतने काल तक टिका रहता है। आयुप्यकर्म का सर्वथा क्षय होते ही पुनः शरीर प्राप्त करने की योग्यता सदा के लिए मिट जाती है। अर्थात् अपुनर्जन्म-स्थिति स्वतः सिद्ध हो जाती है।
शेप रहे चार अघातिकर्मों का सम्बन्ध मुख्यतया देह के साथ और परम्पग से जीव के साथ है। चार अघातिकर्मों के टिके रहने से जीवन्मुक्त वीतराग प्रभु को कुछ विशिष्ट लाभ भी हैं-(१) आत्मा को मुक्ति या सिद्धि के शिखर पर रज्जुवत् जलकर भस्म हुए उक्त चारों अघातिकर्म ही पहुंचाते हैं। आत्मा को जो . ऊर्ध्वगति की रफ्तार प्राप्त होती है, वह अपने पूर्व शरीर-गत प्रवाह में से ही प्राप्त होती है। (२) रस्सी जल जाने पर उसकी राख बन्धन में कदापि नहीं वाँध सकती; वैसे ही केवलज्ञान हो जाने के पश्चात् साधक को ये अवशिष्ट चार कर्म बन्धन में नहीं बाँध सकते। (३) पहले जो आयकर्म देह-माकाग्क था. वही अब जगत् पावनकारी, कल्याणकारी, शुद्ध धर्ममार्गदर्शक तथा लोकोपकारकता में निमित्त बनता है। नामकर्म - और गोत्रकर्म, जो केवलज्ञान से पूर्व देहभान, देहाध्यास और देहाभिमान का पोपण करने में निमित्त थे, वे अब आत्मभानकारक और प्रभुतादर्शक बनते हैं, लोकोपकारी कार्य में निमित्त बनते हैं। वेदनीय कर्म में पहले जहाँ निजानन्दस्वरूप आत्मा को सांसारिक सुख-दुःख का भावावेशपूर्वक बार-बार वेदन होता था, जिससे भेदविज्ञान परिपक्व न होने से कप्टों की अनुभूति व देहासक्ति के कारण अशान्ति महसूस होती थी। अब वहाँ सिर्फ समभाव का वेदन होता है. जो बन्धकारक नहीं है। कर्मबन्ध के आपेक्षिक कारण न रहने पर इन चार अघातिकर्मों के बन्धन भी एक तरह से मुक्ति के कारण (साधन) बन जाते हैं। ये चारों . भवोपग्राही अघातिकर्मावरण वाधक के बदले साधक और सहायक बन जाते हैं।
पन्द्रहवाँ सोपान : सर्वकर्ममुक्त सिद्ध-बुद्ध होने की स्थिति, गति और प्रक्रिया-तेरहवें गुणस्थान में साधक की स्थिति ‘देह छतां जेनी दशा वर्ते देहातीत' जैसी हो जाती है। आयुष्य पूर्ण हो जाने पर पुनः जन्म धारण नहीं करना पडता। ऐसी फिर १४वें गणस्थान में परम संसिद्धि (मक्ति) को प्राप्त महान आत्माओं को परमात्म-पद प्राप्त हो जाने पर पुनः विनश्वर और दुःखों के धामरूप संसार के जन्म-मरण के चक्र में जुड़ना नहीं पड़ता। फिर तो (१४वें गुणस्थान में) सकल कर्मों का सर्वथा विच्छेद होने पर फिर बन्ध विलकुल नहीं होता और भवभ्रमण का अन्त होकर मोक्ष का पथ खुल जाता है। यानी आयुष्य पूर्ण होते ही आयुष्य कर्म के साथ शेष तीनों अघातिकर्म (वेदनीय, नाम और 'गोत्रकर्म) तथा वह शरीर भी सिर्फ अन्तर्मुहूर्तभर समय में सदा के लिए छूट जाता है। वह अयोगीकेवली नामक १४३ गुणस्थान की भूमिका में आ जाता है। उस समय उन महापुरुषों का उपयोग शुक्लध्यान के तृतीय पाद पर केन्द्रित होता है। उस समय (सिद्धधाम जाने की वेला) में मन, वचन, काया और कर्म की छोटी-बड़ी तमाम सजातीय सामग्री (वर्गणा) छूट जाने से पुद्गल स्कन्धों के साथ लगाव सर्वथा छूट जाता है। यानी जड़ (पुद्गल) और चेतन दोनों अपने-अपने असली रूप में आ जाते हैं। अतः १४वें गुणस्थान की स्थिति विलकुल स्वतंत्र, शुद्ध चेतनात्मक, जड़-चेतन-संयोग से सर्वथा रहित लोकोत्तर महाभाग्योदययुक्त अव्यावाध-सुखदायिनी तथा पूर्णतया अबन्धक हो जाती है। वह अयोगीकेवली आत्मा शैलेशी अवस्था में पहुँच जाती है। अब तो इस गुणस्थानवर्ती महापुरुष (परमात्मा) के पुद्गल के एक भी परमाणु का स्पर्श करना बाकी नहीं रहता। यानी आत्मा किसी मिलावट या दाग से रहित पूर्ण शुद्ध, निरंजन, चैतन्यमूर्ति, बेजोड़, अगुरुलघु-अमूर्तस्वरूप एवं अपने सहज परमात्म-पद पर अचल स्थिरता प्राप्त कर लेता है। अब आत्मा अपने शुद्ध आत्मत्व की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है। अतः वह आत्मा 'अ इ उ ऋ लु' इन ५ ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण जितने काल में निष्कम्प हो जाती है। संसार और सिद्धिस्थान; इन दोनों दशाओं के बीच की इस स्थिति में शुक्लध्यान का 'समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति' नामक चतुर्थ पाद होता है। इसमें आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेती है।
__इस प्रकार की शाश्वत स्वभावदशा प्राप्त होने पर स्वधाम में जाने के लिए आत्मा का प्रस्थान समश्रेणीपूर्वक होता है। इस भूमिका में आत्मा अक्रिय और निष्कम्प वनकर. कर्मों से सर्वथा छुटकारा हो जाने के बाद, उनके द्वारा आये हुए पूर्व वेग के कारण शरीर छूटते ही फौरन धनुष में से छूटे हुए तीर की तरह अपने स्वाभाविक रूप के अनुसार सीधा अपने शाश्वत धाम की ओर ऊँचा उड़कर है और वहाँ पहुँच जाता है। यानी सिद्धिस्थान को प्राप्त कर लेता है, जहाँ अनन्त समाधिसुख में अनन्त ज्ञानदर्शन सहित
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org