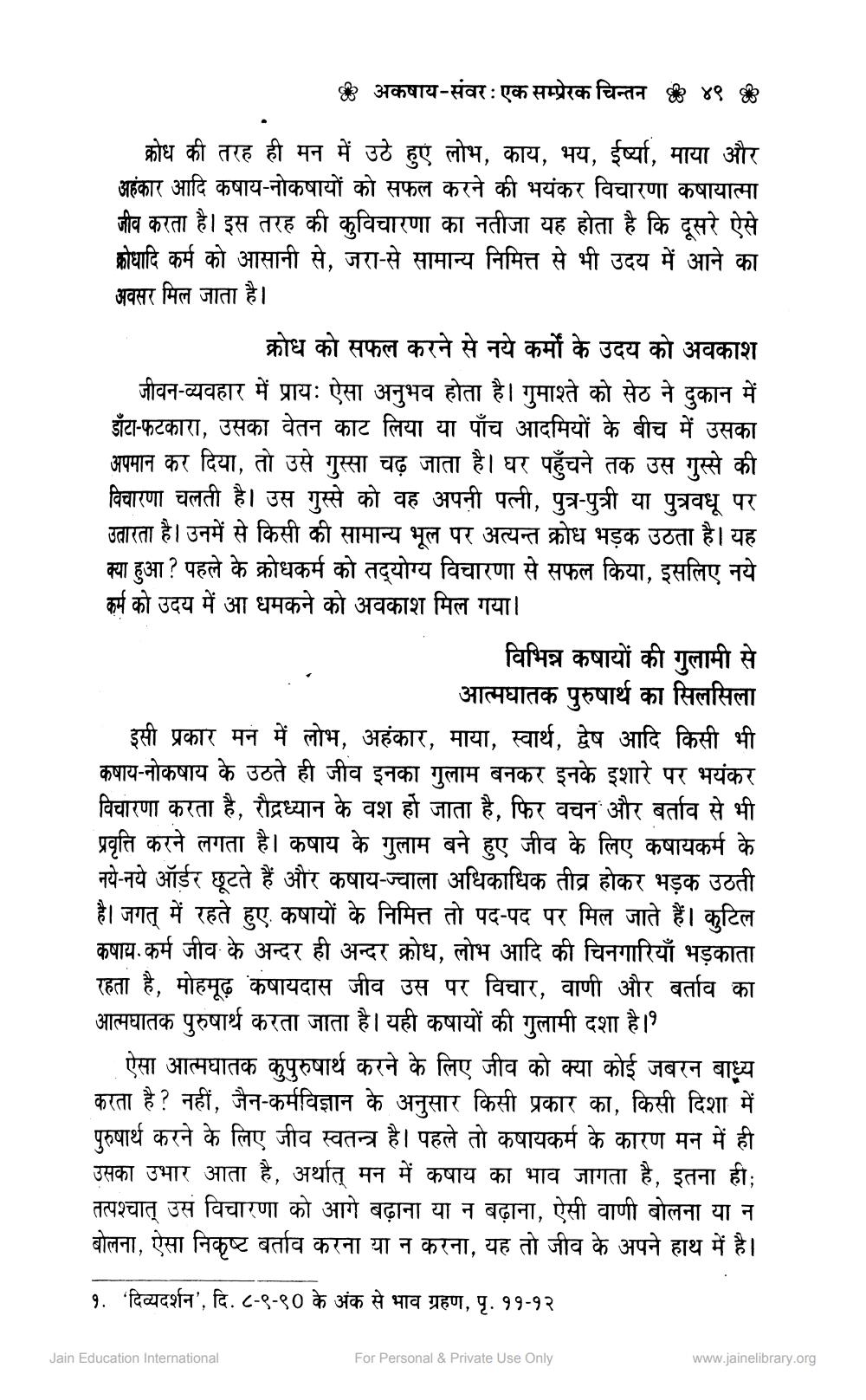________________
* अकषाय-संवर : एक सम्प्रेरक चिन्तन ॐ ४९ ॐ
क्रोध की तरह ही मन में उठे हुए लोभ, काय, भय, ईर्ष्या, माया और अहंकार आदि कषाय-नोकषायों को सफल करने की भयंकर विचारणा कषायात्मा जीव करता है। इस तरह की कुविचारणा का नतीजा यह होता है कि दूसरे ऐसे क्रोधादि कर्म को आसानी से, जरा-से सामान्य निमित्त से भी उदय में आने का अवसर मिल जाता है।
___ क्रोध को सफल करने से नये कर्मों के उदय को अवकाश __जीवन-व्यवहार में प्रायः ऐसा अनुभव होता है। गुमाश्ते को सेठ ने दुकान में डाँटा-फटकारा, उसका वेतन काट लिया या पाँच आदमियों के बीच में उसका अपमान कर दिया, तो उसे गुस्सा चढ़ जाता है। घर पहुँचने तक उस गुस्से की विचारणा चलती है। उस गुस्से को वह अपनी पत्नी, पुत्र-पुत्री या पुत्रवधू पर उतारता है। उनमें से किसी की सामान्य भूल पर अत्यन्त क्रोध भड़क उठता है। यह क्या हुआ? पहले के क्रोधकर्म को तद्योग्य विचारणा से सफल किया, इसलिए नये कर्म को उदय में आ धमकने को अवकाश मिल गया।
विभिन्न कषायों की गुलामी से
आत्मघातक पुरुषार्थ का सिलसिला इसी प्रकार मन में लोभ, अहंकार, माया, स्वार्थ, द्वेष आदि किसी भी कषाय-नोकषाय के उठते ही जीव इनका गुलाम बनकर इनके इशारे पर भयंकर विचारणा करता है, रौद्रध्यान के वश हो जाता है, फिर वचन और बर्ताव से भी प्रवृत्ति करने लगता है। कषाय के गुलाम बने हुए जीव के लिए कषायकर्म के नये-नये ऑर्डर छूटते हैं और कषाय-ज्वाला अधिकाधिक तीव्र होकर भड़क उठती है। जगत् में रहते हुए. कषायों के निमित्त तो पद-पद पर मिल जाते हैं। कुटिल कषाय कर्म जीव के अन्दर ही अन्दर क्रोध, लोभ आदि की चिनगारियाँ भड़काता रहता है, मोहमूढ़ कषायदास जीव उस पर विचार, वाणी और बर्ताव का आत्मघातक पुरुषार्थ करता जाता है। यही कषायों की गुलामी दशा है।
ऐसा आत्मघातक कुपुरुषार्थ करने के लिए जीव को क्या कोई जबरन बाध्य करता है? नहीं, जैन-कर्मविज्ञान के अनुसार किसी प्रकार का, किसी दिशा में पुरुषार्थ करने के लिए जीव स्वतन्त्र है। पहले तो कषायकर्म के कारण मन में ही उसका उभार आता है, अर्थात् मन में कषाय का भाव जागता है, इतना ही; तत्पश्चात् उस विचारणा को आगे बढ़ाना या न बढ़ाना, ऐसी वाणी बोलना या न बोलना, ऐसा निकृष्ट बर्ताव करना या न करना, यह तो जीव के अपने हाथ में है।
१. 'दिव्यदर्शन', दि. ८-९-९० के अंक से भाव ग्रहण, पृ. ११-१२
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org