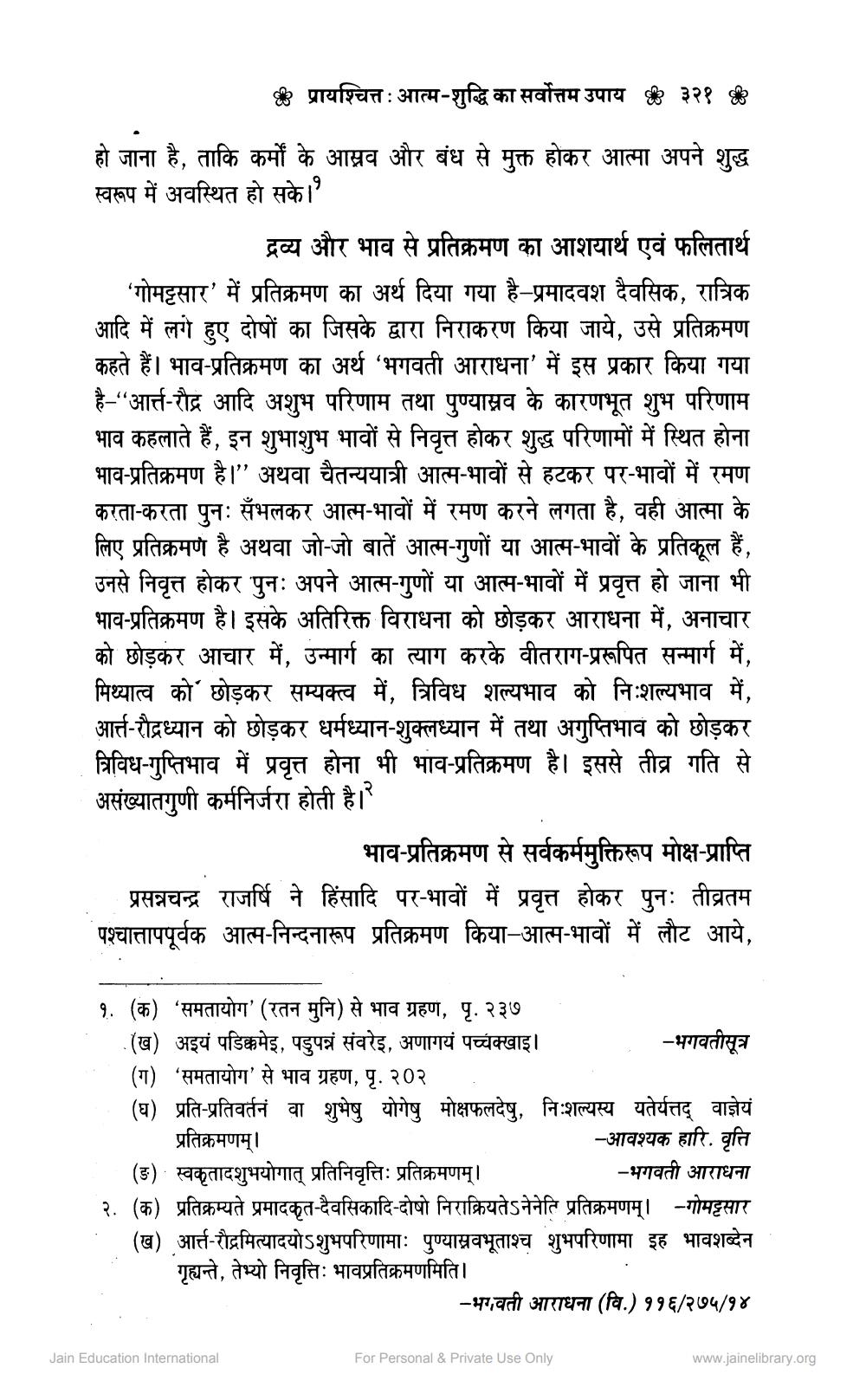________________
प्रायश्चित्त : आत्म-शुद्धि का सर्वोत्तम उपाय ॐ ३२१ 8
हो जाना है, ताकि कर्मों के आस्रव और बंध से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो सके।
द्रव्य और भाव से प्रतिक्रमण का आशयार्थ एवं फलितार्थ 'गोमट्टसार' में प्रतिक्रमण का अर्थ दिया गया है-प्रमादवश दैवसिक, रात्रिक आदि में लगे हुए दोषों का जिसके द्वारा निराकरण किया जाये, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। भाव-प्रतिक्रमण का अर्थ 'भगवती आराधना' में इस प्रकार किया गया है-"आर्त्त-रौद्र आदि अशुभ परिणाम तथा पुण्यास्रव के कारणभूत शुभ परिणाम भाव कहलाते हैं, इन शुभाशुभ भावों से निवृत्त होकर शुद्ध परिणामों में स्थित होना भाव-प्रतिक्रमण है।" अथवा चैतन्ययात्री आत्म-भावों से हटकर पर-भावों में रमण करता-करता पुनः सँभलकर आत्म-भावों में रमण करने लगता है, वही आत्मा के लिए प्रतिक्रमण है अथवा जो-जो बातें आत्म-गुणों या आत्म-भावों के प्रतिकूल हैं, उनसे निवृत्त होकर पुनः अपने आत्म-गुणों या आत्म-भावों में प्रवृत्त हो जाना भी भाव-प्रतिक्रमण है। इसके अतिरिक्त विराधना को छोड़कर आराधना में, अनाचार को छोड़कर आचार में, उन्मार्ग का त्याग करके वीतराग-प्ररूपित सन्मार्ग में, मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व में, त्रिविध शल्यभाव को निःशल्यभाव में, आत-रौद्रध्यान को छोड़कर धर्मध्यान-शुक्लध्यान में तथा अगुप्तिभाव को छोड़कर त्रिविध-गुप्तिभाव में प्रवृत्त होना भी भाव-प्रतिक्रमण है। इससे तीव्र गति से असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है।
भाव-प्रतिक्रमण से सर्वकर्ममुक्तिरूप मोक्ष-प्राप्ति प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ने हिंसादि पर-भावों में प्रवृत्त होकर पुनः तीव्रतम पश्चात्तापपूर्वक आत्म-निन्दनारूप प्रतिक्रमण किया-आत्म-भावों में लौट आये,
१. (क) 'समतायोग' (रतन मुनि) से भाव ग्रहण, पृ. २३७ (ख) अइयं पडिक्कमेइ, पडुपन्नं संवरेइ, अणागयं पच्चक्खाइ।
-भगवतीसूत्र (ग) “समतायोग' से भाव ग्रहण, पृ. २०२ (घ) प्रति-प्रतिवर्तनं वा शुभेषु योगेषु मोक्षफलदेषु, निःशल्यस्य यतेर्यत्तद् वाज्ञेयं प्रतिक्रमणम्।
-आवश्यक हारि. वृत्ति (ङ) स्वकृतादशुभयोगात् प्रतिनिवृत्तिः प्रतिक्रमणम्। ____ -भगवती आराधना २. (क) प्रतिक्रम्यते प्रमादकृत-दैवसिकादि-दोषो निराक्रियतेऽनेनेति प्रतिक्रमणम्। -गोमट्टसार (ख) आर्त-रौद्रमित्यादयोऽशुभपरिणामाः पुण्यासवभूताश्च शुभपरिणामा इह भावशब्देन गृह्यन्ते, तेभ्यो निवृत्तिः भावप्रतिक्रमणमिति।
-भगवती आराधना (वि.) ११६/२७५/१४
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org