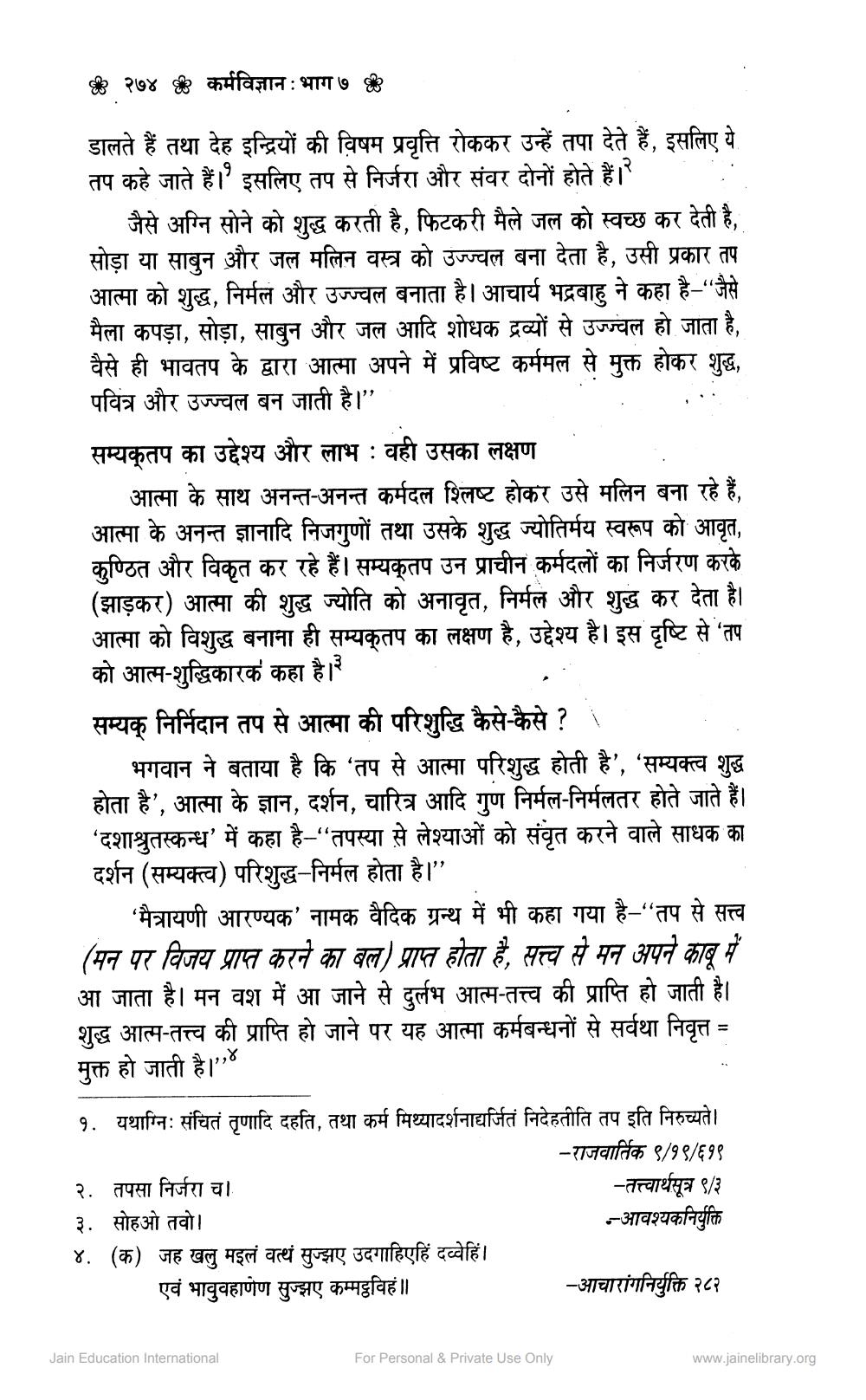________________
ॐ २७४ ® कर्मविज्ञान : भाग ७ *
डालते हैं तथा देह इन्द्रियों की विषम प्रवृत्ति रोककर उन्हें तपा देते हैं, इसलिए ये तप कहे जाते हैं। इसलिए तप से निर्जरा और संवर दोनों होते हैं। ____ जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, फिटकरी मैले जल को स्वच्छ कर देती है, सोड़ा या साबुन और जल मलिन वस्त्र को उज्ज्वल बना देता है, उसी प्रकार तप आत्मा को शुद्ध, निर्मल और उज्ज्वल बनाता है। आचार्य भद्रबाहु ने कहा है-"जैसे मैला कपड़ा, सोड़ा, साबुन और जल आदि शोधक द्रव्यों से उज्ज्वल हो जाता है, वैसे ही भावतप के द्वारा आत्मा अपने में प्रविष्ट कर्ममल से मुक्त होकर शुद्ध, पवित्र और उज्ज्वल बन जाती है।" सम्यक्तप का उद्देश्य और लाभ : वही उसका लक्षण
आत्मा के साथ अनन्त-अनन्त कर्मदल श्लिष्ट होकर उसे मलिन बना रहे हैं, आत्मा के अनन्त ज्ञानादि निजगुणों तथा उसके शुद्ध ज्योतिर्मय स्वरूप को आवृत, कुण्ठित और विकृत कर रहे हैं। सम्यक्तप उन प्राचीन कर्मदलों का निर्जरण करके (झाड़कर) आत्मा की शुद्ध ज्योति को अनावृत, निर्मल और शुद्ध कर देता है। आत्मा को विशुद्ध बनाना ही सम्यक्तप का लक्षण है, उद्देश्य है। इस दृष्टि से 'तप को आत्म-शुद्धिकारक कहा है। सम्यक् निर्निदान तप से आत्मा की परिशुद्धि कैसे-कैसे ? .
भगवान ने बताया है कि 'तप से आत्मा परिशुद्ध होती है', 'सम्यक्त्व शुद्ध होता है', आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुण निर्मल-निर्मलतर होते जाते हैं। ‘दशाश्रुतस्कन्ध' में कहा है-"तपस्या से लेश्याओं को संवृत करने वाले साधक का दर्शन (सम्यक्त्व) परिशुद्ध-निर्मल होता है।"
'मैत्रायणी आरण्यक' नामक वैदिक ग्रन्थ में भी कहा गया है-“तप से सत्त्व (मन पर विजय प्राप्त करने का बल) प्राप्त होता है, सत्त्व से मन अपने काबू में आ जाता है। मन वश में आ जाने से दुर्लभ आत्म-तत्त्व की प्राप्ति हो जाती है। शुद्ध आत्म-तत्त्व की प्राप्ति हो जाने पर यह आत्मा कर्मबन्धनों से सर्वथा निवृत्त = मुक्त हो जाती है।
१. यथाग्निः संचितं तृणादि दहति, तथा कर्म मिथ्यादर्शनाद्यर्जितं निदेहतीति तप इति निरुच्यते।
-राजवार्तिक ९/१९/६१९ २. तपसा निर्जरा च।
-तत्त्वार्थसूत्र ९/३ ३. सोहओ तवो।
-आवश्यकनियुक्ति ४. (क) जह खलु मइलं वत्थं सुज्झए उदगाहिएहिं दव्वेहिं । एवं भावुवहाणेण सुज्झए कम्मट्ठविहं॥
-आचारांगनियुक्ति २८२
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org