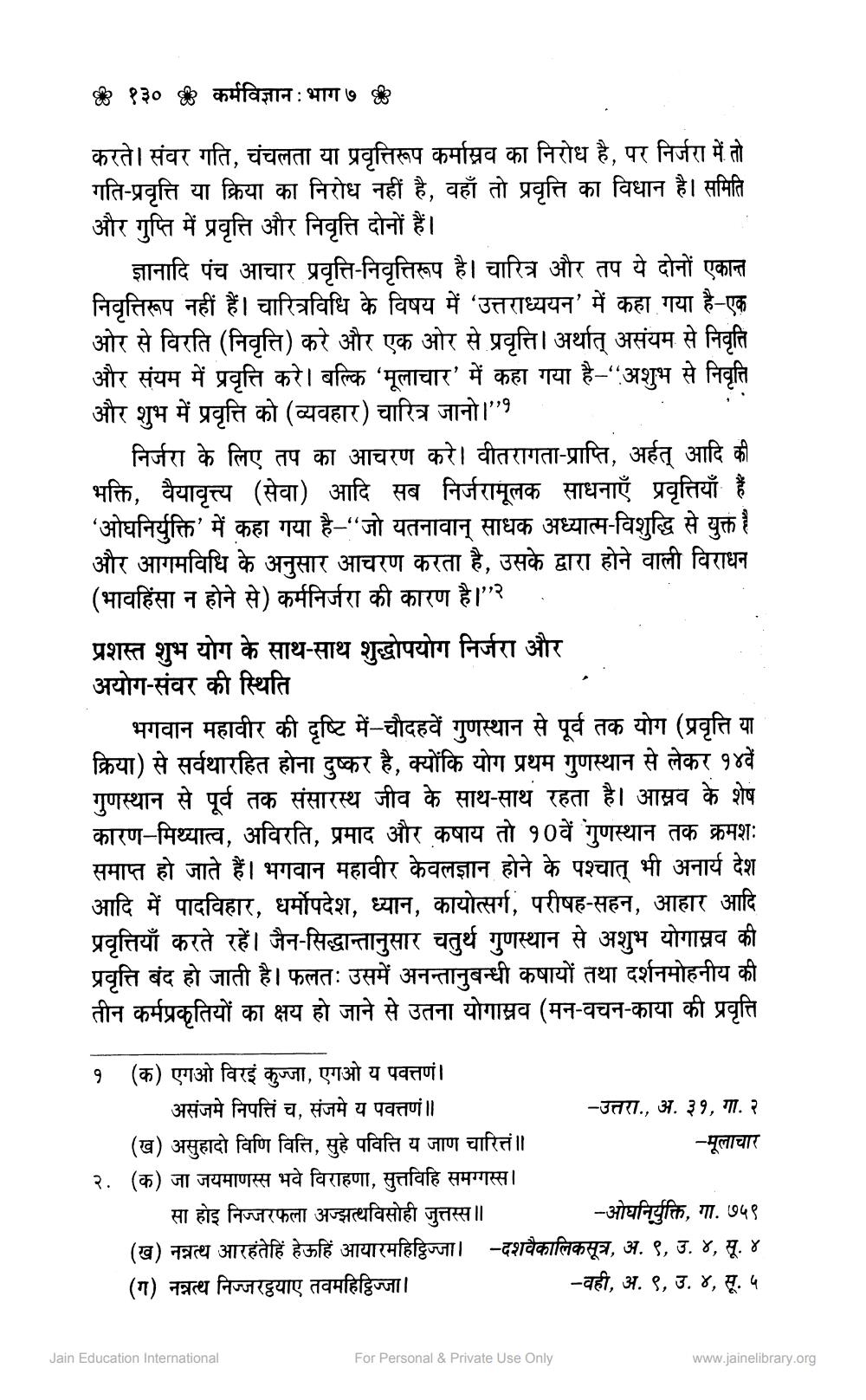________________
* १३० * कर्मविज्ञान : भाग ७ ॐ
करते। संवर गति, चंचलता या प्रवृत्तिरूप कर्मानव का निरोध है, पर निर्जरा में तो गति-प्रवृत्ति या क्रिया का निरोध नहीं है, वहाँ तो प्रवृत्ति का विधान है। समिति और गुप्ति में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों हैं।
ज्ञानादि पंच आचार प्रवत्ति-निवत्तिरूप है। चारित्र और तप ये दोनों एकान्त निवृत्तिरूप नहीं हैं। चारित्रविधि के विषय में 'उत्तराध्ययन' में कहा गया है-एक ओर से विरति (निवृत्ति) करे और एक ओर से प्रवृत्ति। अर्थात् असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति करे। बल्कि 'मूलाचार' में कहा गया है-"अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति को (व्यवहार) चारित्र जानो।"१
निर्जरा के लिए तप का आचरण करे। वीतरागता-प्राप्ति, अर्हत् आदि की भक्ति, वैयावृत्त्य (सेवा) आदि सब निर्जरामूलक साधनाएँ प्रवृत्तियाँ हैं ‘ओघनियुक्ति' में कहा गया है-"जो यतनावान् साधक अध्यात्म-विशुद्धि से युक्त है
और आगमविधि के अनुसार आचरण करता है, उसके द्वारा होने वाली विराधन (भावहिंसा न होने से) कर्मनिर्जरा की कारण है।"२ . प्रशस्त शुभ योग के साथ-साथ शुद्धोपयोग निर्जरा और अयोग-संवर की स्थिति
भगवान महावीर की दृष्टि में चौदहवें गुणस्थान से पूर्व तक योग (प्रवृत्ति या क्रिया) से सर्वथारहित होना दुष्कर है, क्योंकि योग प्रथम गुणस्थान से लेकर १४वें गुणस्थान से पूर्व तक संसारस्थ जीव के साथ-साथ रहता है। आसव के शेष कारण-मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय तो १0वें गुणस्थान तक क्रमशः समाप्त हो जाते हैं। भगवान महावीर केवलज्ञान होने के पश्चात् भी अनार्य देश आदि में पादविहार, धर्मोपदेश, ध्यान, कायोत्सर्ग, परीषह-सहन, आहार आदि प्रवृत्तियाँ करते रहें। जैन-सिद्धान्तानुसार चतुर्थ गुणस्थान से अशुभ योगासव की प्रवृत्ति बंद हो जाती है। फलतः उसमें अनन्तानुबन्धी कषायों तथा दर्शनमोहनीय की तीन कर्मप्रकृतियों का क्षय हो जाने से उतना योगासव (मन-वचन-काया की प्रवृत्ति
-मूलाचार
१ (क) एगओ विरइं कुज्जा, एगओ य पवत्तणं। असंजमे निपत्तिं च, संजमे य पवत्तणं॥
-उत्तरा., अ. ३१, गा.२ (ख) असुहादो विणि वित्ति, सुहे पवित्ति य जाण चारित्तं॥ २. (क) जा जयमाणस्स भवे विराहणा, सुत्तविहि समग्गस्स।
सा होइ निज्जरफला अज्झत्थविसोही जुत्तस्स॥ -ओघनियुक्ति, गा. ७५९ (ख) नन्नत्थ आरहंतेहिं हेऊहिं आयारमहिट्ठिज्जा। -दशवैकालिकसूत्र, अ. ९, उ. ४, सू. ४ (ग) नन्नत्थ निज्जरट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा।
-वही, अ. ९, उ. ४, सू. ५
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org