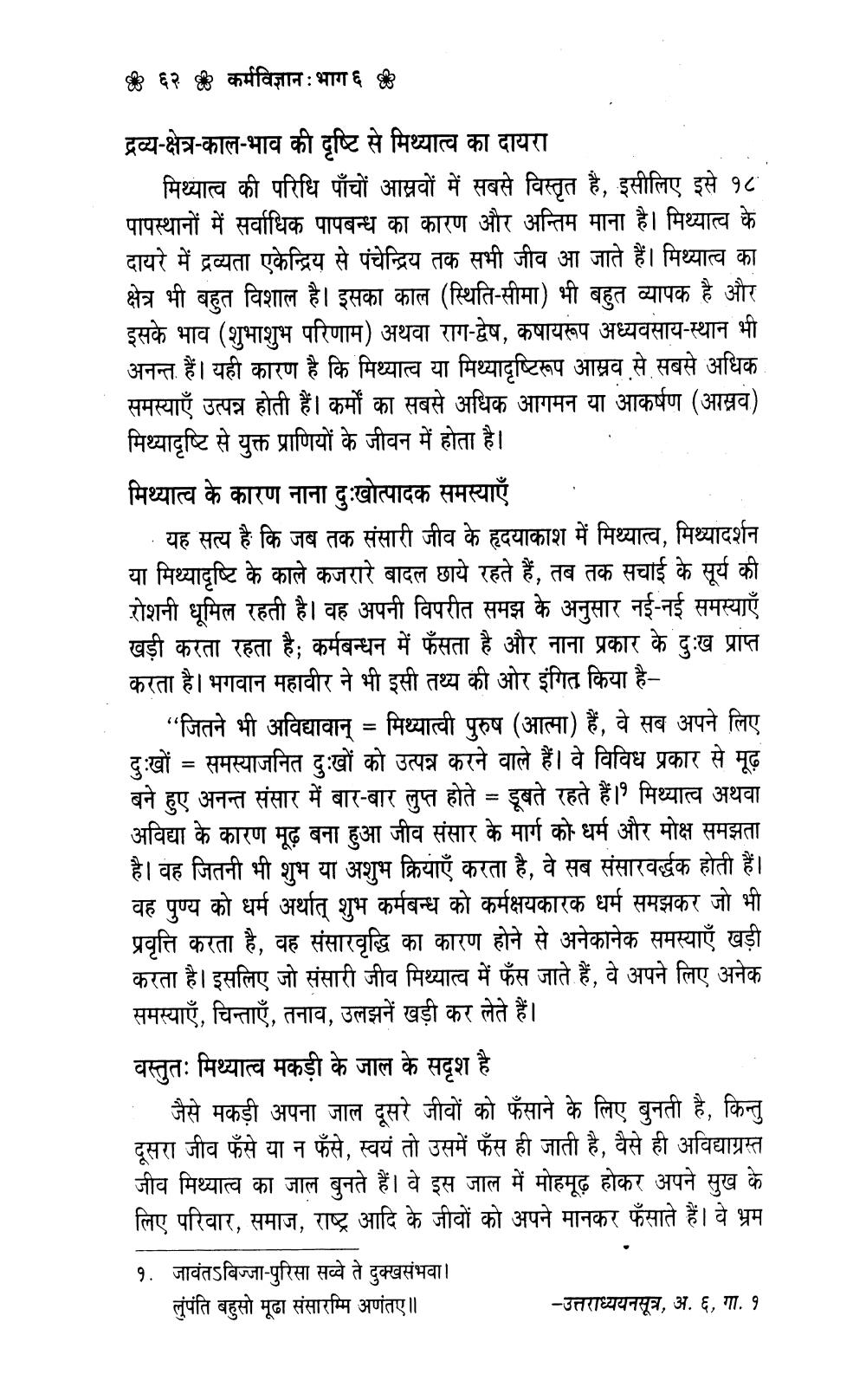________________
ॐ ६२ ® कर्मविज्ञान : भाग ६ *
द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की दृष्टि से मिथ्यात्व का दायरा
मिथ्यात्व की परिधि पाँचों आम्रवों में सबसे विस्तृत है, इसीलिए इसे १८ पापस्थानों में सर्वाधिक पापबन्ध का कारण और अन्तिम माना है। मिथ्यात्व के दायरे में द्रव्यता एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक सभी जीव आ जाते हैं। मिथ्यात्व का क्षेत्र भी बहुत विशाल है। इसका काल (स्थिति-सीमा) भी बहुत व्यापक है और इसके भाव (शुभाशुभ परिणाम) अथवा राग-द्वेष, कषायरूप अध्यवसाय-स्थान भी अनन्त हैं। यही कारण है कि मिथ्यात्व या मिथ्यादृष्टिरूप आस्रव से सबसे अधिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। कर्मों का सबसे अधिक आगमन या आकर्षण (आम्रव) मिथ्यादृष्टि से युक्त प्राणियों के जीवन में होता है। मिथ्यात्व के कारण नाना दुःखोत्पादक समस्याएँ
.. यह सत्य है कि जब तक संसारी जीव के हृदयाकाश में मिथ्यात्व, मिथ्यादर्शन या मिथ्यादृष्टि के काले कजरारे बादल छाये रहते हैं, तब तक सचाई के सूर्य की रोशनी धूमिल रहती है। वह अपनी विपरीत समझ के अनुसार नई-नई समस्याएँ खड़ी करता रहता है; कर्मबन्धन में फँसता है और नाना प्रकार के दुःख प्राप्त करता है। भगवान महावीर ने भी इसी तथ्य की ओर इंगित किया है___ "जितने भी अविद्यावान् = मिथ्यात्वी पुरुष (आत्मा) हैं, वे सब अपने लिए दुःखों = समस्याजनित दुःखों को उत्पन्न करने वाले हैं। वे विविध प्रकार से मूढ़ बने हुए अनन्त संसार में बार-बार लुप्त होते = डूबते रहते हैं।' मिथ्यात्व अथवा अविद्या के कारण मूढ़ बना हुआ जीव संसार के मार्ग को धर्म और मोक्ष समझता है। वह जितनी भी शुभ या अशुभ क्रियाएँ करता है, वे सब संसारवर्द्धक होती हैं। वह पुण्य को धर्म अर्थात् शुभ कर्मबन्ध को कर्मक्षयकारक धर्म समझकर जो भी प्रवृत्ति करता है, वह संसारवृद्धि का कारण होने से अनेकानेक समस्याएँ खड़ी करता है। इसलिए जो संसारी जीव मिथ्यात्व में फँस जाते हैं, वे अपने लिए अनेक समस्याएँ, चिन्ताएँ, तनाव, उलझनें खड़ी कर लेते हैं। वस्तुतः मिथ्यात्व मकड़ी के जाल के सदृश है - जैसे मकड़ी अपना जाल दूसरे जीवों को फँसाने के लिए बुनती है, किन्तु दुसरा जीव फँसे या न फँसे, स्वयं तो उसमें फँस ही जाती है, वैसे ही अविद्याग्रस्त जीव मिथ्यात्व का जाल बुनते हैं। वे इस जाल में मोहमूढ़ होकर अपने सुख के लिए परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के जीवों को अपने मानकर फँसाते हैं। वे भ्रम
१. जावंतऽविज्जा-पुरिसा सव्वे ते दुक्खसंभवा।
लुपंति बहुसो मूढा संसारम्मि अणंतए॥
-उत्तराध्ययनसूत्र, अ. ६, गा.१