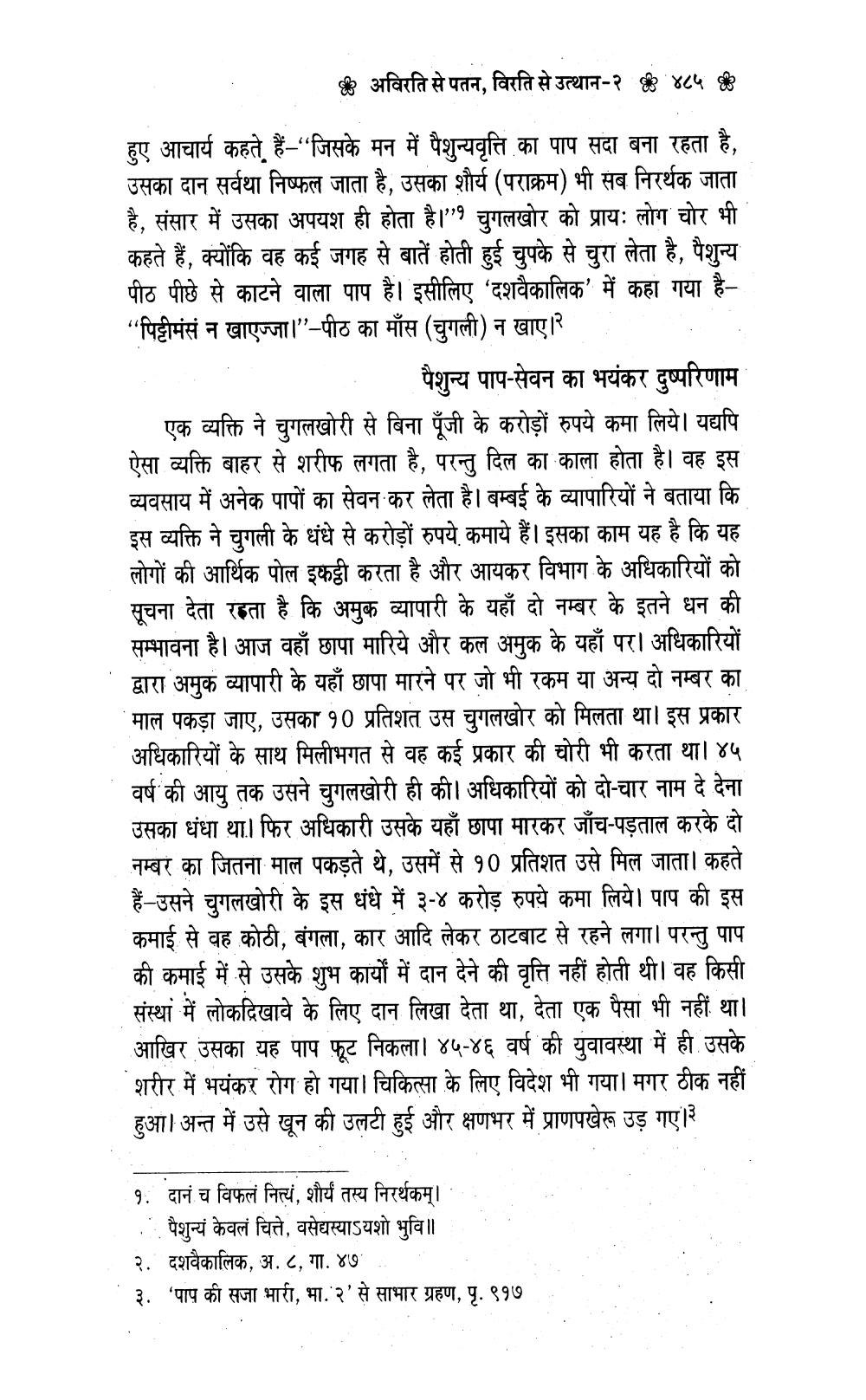________________
* अविरति से पतन, विरति से उत्थान-२ ॐ ४८५ *
हुए आचार्य कहते हैं-“जिसके मन में पैशुन्यवृत्ति का पाप सदा बना रहता है, उसका दान सर्वथा निष्फल जाता है, उसका शौर्य (पराक्रम) भी सब निरर्थक जाता है, संसार में उसका अपयश ही होता है।"१ चुगलखोर को प्रायः लोग चोर भी कहते हैं, क्योंकि वह कई जगह से बातें होती हुई चुपके से चुरा लेता है, पैशुन्य पीठ पीछे से काटने वाला पाप है। इसीलिए 'दशवैकालिक' में कहा गया है“पिट्टीमंसं न खाएज्जा।''-पीठ का माँस (चुगली) न खाए।२
. पैशुन्य पाप-सेवन का भयंकर दुष्परिणाम एक व्यक्ति ने चुगलखोरी से बिना पूँजी के करोड़ों रुपये कमा लिये। यद्यपि ऐसा व्यक्ति बाहर से शरीफ लगता है, परन्तु दिल का काला होता है। वह इस व्यवसाय में अनेक पापों का सेवन कर लेता है। बम्बई के व्यापारियों ने बताया कि इस व्यक्ति ने चुगली के धंधे से करोड़ों रुपये कमाये हैं। इसका काम यह है कि यह लोगों की आर्थिक पोल इकट्ठी करता है और आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचना देता रहता है कि अमुक व्यापारी के यहाँ दो नम्बर के इतने धन की सम्भावना है। आज वहाँ छापा मारिये और कल अमुक के यहाँ पर। अधिकारियों द्वारा अमुक व्यापारी के यहाँ छापा मारने पर जो भी रकम या अन्य दो नम्बर का माल पकड़ा जाए, उसका १० प्रतिशत उस चुगलखोर को मिलता था। इस प्रकार अधिकारियों के साथ मिलीभगत से वह कई प्रकार की चोरी भी करता था। ४५ वर्ष की आयु तक उसने चुगलखोरी ही की। अधिकारियों को दो-चार नाम दे देना उसका धंधा था। फिर अधिकारी उसके यहाँ छापा मारकर जाँच-पड़ताल करके दो नम्बर का जितना माल पकड़ते थे, उसमें से १० प्रतिशत उसे मिल जाता। कहते हैं-उसने चुगलखोरी के इस धंधे में ३-४ करोड़ रुपये कमा लिये। पाप की इस कमाई से वह कोठी, बंगला, कार आदि लेकर ठाटबाट से रहने लगा। परन्तु पाप की कमाई में से उसके शुभ कार्यों में दान देने की वृत्ति नहीं होती थी। वह किसी संस्था में लोकदिखावे के लिए दान लिखा देता था, देता एक पैसा भी नहीं था। आखिर उसका यह पाप फूट निकला। ४५-४६ वर्ष की युवावस्था में ही उसके शरीर में भयंकर रोग हो गया। चिकित्सा के लिए विदेश भी गया। मगर ठीक नहीं हुआ। अन्त में उसे खून की उलटी हुई और क्षणभर में प्राणपखेरू उड़ गए।३
१. दानं च विफलं नित्यं, शौर्यं तस्य निरर्थकम्। . पैशुन्यं केवलं चित्ते, वसेद्यस्याऽयशो भुवि॥ २. दशवैकालिक, अ. ८, गा. ४७ ३. 'पाप की सजा भारी, भा. २' से साभार ग्रहण, पृ. ९१७