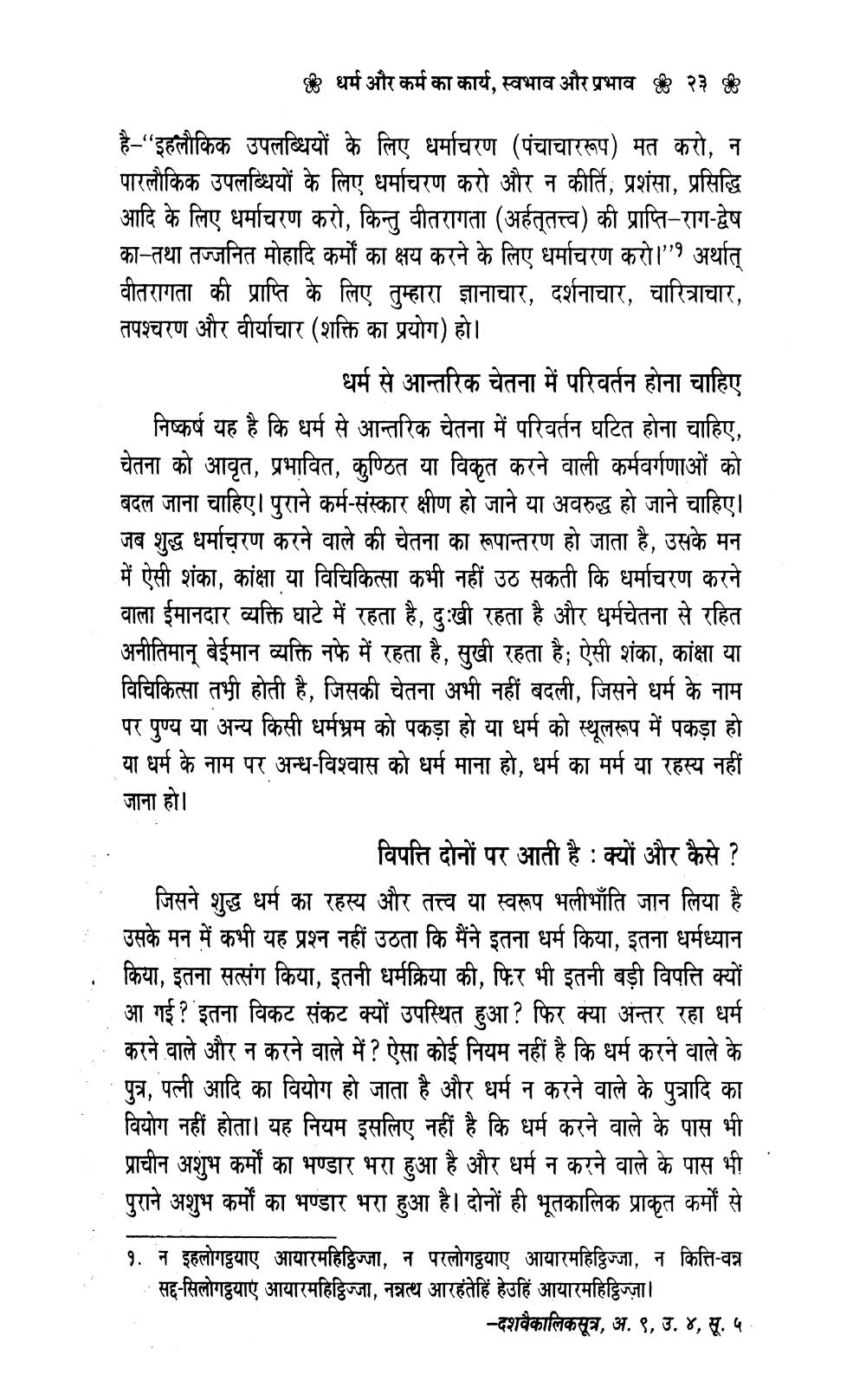________________
ॐ धर्म और कर्म का कार्य, स्वभाव और प्रभाव * २३ 8
है-“इहलौकिक उपलब्धियों के लिए धर्माचरण (पंचाचाररूप) मत करो, न पारलौकिक उपलब्धियों के लिए धर्माचरण करो और न कीर्ति, प्रशंसा, प्रसिद्धि आदि के लिए धर्माचरण करो, किन्तु वीतरागता (अर्हत्तत्त्व) की प्राप्ति-राग-द्वेष का-तथा तज्जनित मोहादि कर्मों का क्षय करने के लिए धर्माचरण करो।"१ अर्थात् वीतरागता की प्राप्ति के लिए तुम्हारा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपश्चरण और वीर्याचार (शक्ति का प्रयोग) हो।
धर्म से आन्तरिक चेतना में परिवर्तन होना चाहिए निष्कर्ष यह है कि धर्म से आन्तरिक चेतना में परिवर्तन घटित होना चाहिए, चेतना को आवृत, प्रभावित, कुण्ठित या विकृत करने वाली कर्मवर्गणाओं को बदल जाना चाहिए। पुराने कर्म-संस्कार क्षीण हो जाने या अवरुद्ध हो जाने चाहिए। जब शुद्ध धर्माचरण करने वाले की चेतना का रूपान्तरण हो जाता है, उसके मन में ऐसी शंका, कांक्षा या विचिकित्सा कभी नहीं उठ सकती कि धर्माचरण करने वाला ईमानदार व्यक्ति घाटे में रहता है, दुःखी रहता है और धर्मचेतना से रहित अनीतिमान् बेईमान व्यक्ति नफे में रहता है, सुखी रहता है; ऐसी शंका, कांक्षा या विचिकित्सा तभी होती है, जिसकी चेतना अभी नहीं बदली, जिसने धर्म के नाम पर पुण्य या अन्य किसी धर्मभ्रम को पकड़ा हो या धर्म को स्थूलरूप में पकड़ा हो या धर्म के नाम पर अन्ध-विश्वास को धर्म माना हो, धर्म का मर्म या रहस्य नहीं जाना हो।
विपत्ति दोनों पर आती है : क्यों और कैसे ? जिसने शुद्ध धर्म का रहस्य और तत्त्व या स्वरूप भलीभाँति जान लिया है उसके मन में कभी यह प्रश्न नहीं उठता कि मैंने इतना धर्म किया, इतना धर्मध्यान . किया, इतना सत्संग किया, इतनी धर्मक्रिया की, फिर भी इतनी बड़ी विपत्ति क्यों
आ गई? इतना विकट संकट क्यों उपस्थित हुआ? फिर क्या अन्तर रहा धर्म करने वाले और न करने वाले में? ऐसा कोई नियम नहीं है कि धर्म करने वाले के पुत्र, पत्नी आदि का वियोग हो जाता है और धर्म न करने वाले के पुत्रादि का वियोग नहीं होता। यह नियम इसलिए नहीं है कि धर्म करने वाले के पास भी प्राचीन अशुभ कर्मों का भण्डार भरा हुआ है और धर्म न करने वाले के पास भी पुराने अशुभ कर्मों का भण्डार भरा हुआ है। दोनों ही भूतकालिक प्राकृत कर्मों से
१. न इहलोगट्ठयाए आयारमहिट्ठिज्जा, न परलोगट्ठयाए आयारमहिट्ठिज्जा, न कित्ति-वन्न सद्द-सिलोगट्ठयाए आयारमहिट्ठिज्जा, नन्नत्थ आरहंतेहिं हेउहिं आयारमहिट्ठिज्जा।
-दशवकालिकसूत्र, अ. ९, उ. ४, सू. ५