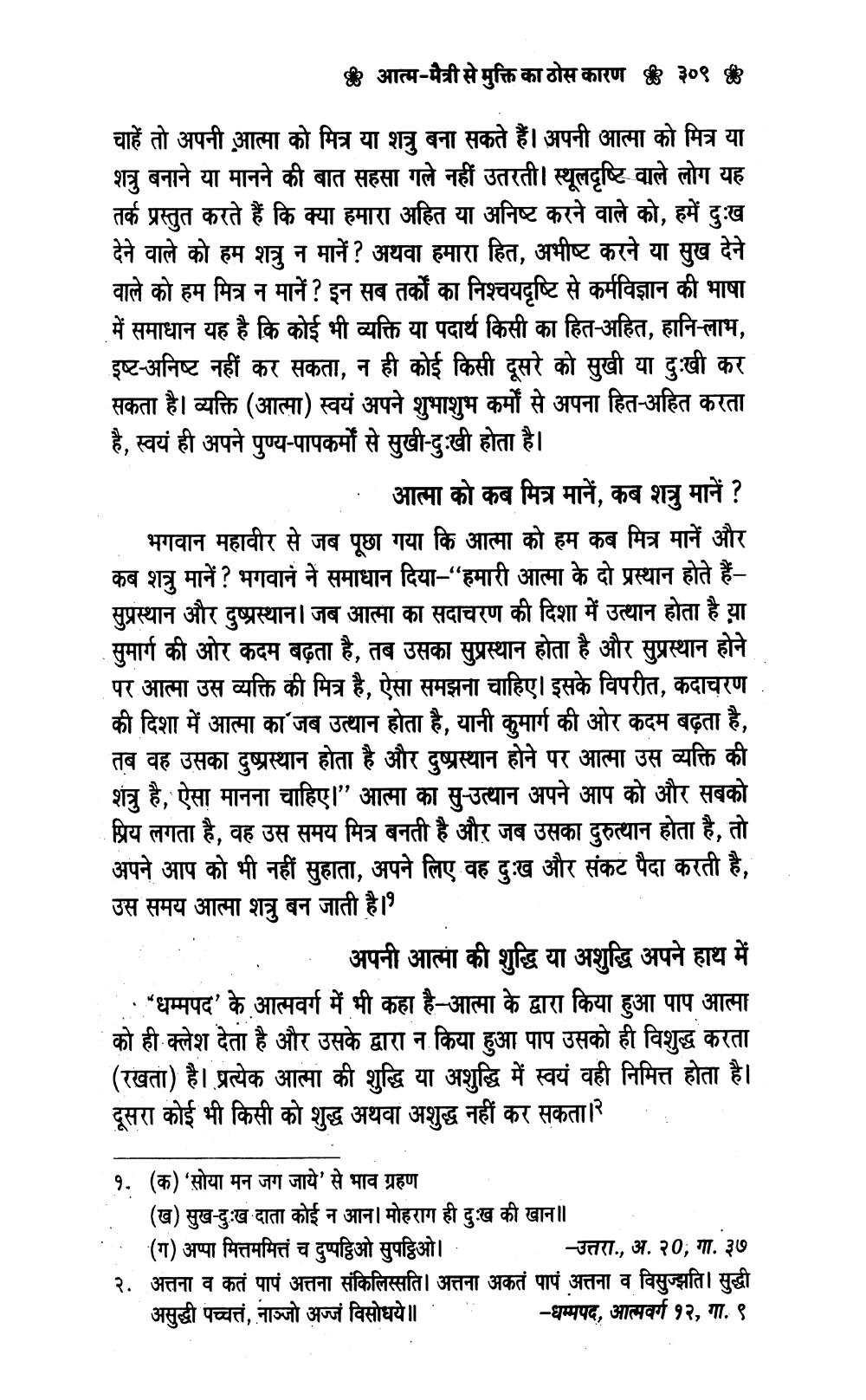________________
ॐ आत्म-मैत्री से मुक्ति का ठोस कारण 8 ३०९ 8
चाहें तो अपनी आत्मा को मित्र या शत्रु बना सकते हैं। अपनी आत्मा को मित्र या शत्रु बनाने या मानने की बात सहसा गले नहीं उतरती। स्थूलदृष्टि वाले लोग यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि क्या हमारा अहित या अनिष्ट करने वाले को, हमें दुःख देने वाले को हम शत्रु न मानें ? अथवा हमारा हित, अभीष्ट करने या सुख देने वाले को हम मित्र न मानें? इन सब तर्कों का निश्चयदृष्टि से कर्मविज्ञान की भाषा में समाधान यह है कि कोई भी व्यक्ति या पदार्थ किसी का हित-अहित, हानि-लाभ, इष्ट-अनिष्ट नहीं कर सकता, न ही कोई किसी दूसरे को सुखी या दुःखी कर सकता है। व्यक्ति (आत्मा) स्वयं अपने शुभाशुभ कर्मों से अपना हित-अहित करता है, स्वयं ही अपने पुण्य-पापकर्मों से सुखी-दुःखी होता है।
. आत्मा को कब मित्र मानें, कब शत्रु मानें ? भगवान महावीर से जब पूछा गया कि आत्मा को हम कब मित्र माने और कब शत्रु माने? भगवान ने समाधान दिया-"हमारी आत्मा के दो प्रस्थान होते हैंसुप्रस्थान और दुष्प्रस्थान। जब आत्मा का सदाचरण की दिशा में उत्थान होता है या सुमार्ग की ओर कदम बढ़ता है, तब उसका सुप्रस्थान होता है और सुप्रस्थान होने पर आत्मा उस व्यक्ति की मित्र है, ऐसा समझना चाहिए। इसके विपरीत, कदाचरण की दिशा में आत्मा का जब उत्थान होता है, यानी कुमार्ग की ओर कदम बढ़ता है, तब वह उसका दुष्प्रस्थान होता है और दुष्प्रस्थान होने पर आत्मा उस व्यक्ति की शत्रु है, ऐसा मानना चाहिए।" आत्मा का सु-उत्थान अपने आप को और सबको प्रिय लगता है, वह उस समय मित्र बनती है और जब उसका दुरुत्थान होता है, तो अपने आप को भी नहीं सुहाता, अपने लिए वह दुःख और संकट पैदा करती है, उस समय आत्मा शत्रु बन जाती है।'
. . अपनी आत्मा की शुद्धि या अशुद्धि अपने हाथ में • “धम्मपद' के आत्मवर्ग में भी कहा है-आत्मा के द्वारा किया हुआ पाप आत्मा को ही क्लेश देता है और उसके द्वारा न किया हुआ पाप उसको ही विशुद्ध करता (रखता) है। प्रत्येक आत्मा की शुद्धि या अशुद्धि में स्वयं वही निमित्त होता है। दूसरा कोई भी किसी को शुद्ध अथवा अशुद्ध नहीं कर सकता।
१. (क) 'सोया मन जग जाये' से भाव ग्रहण
(ख) सुख-दुःख दाता कोई न आन। मोहराग ही दुःख की खान॥ .. (ग) अप्पा मित्तममित्तं च दुष्पट्ठिओ सुपट्ठिओ। . -उत्तरा., अ. २०, गा. ३७ २. अत्तना व कतं पापं अत्तना संकिलिस्सति। अत्तना अकतं पापं अत्तना व विसुज्झति। सुद्धी असुद्धी पच्चत्तं, नाजो अज्जं विसोधये॥
-धम्मपद, आत्मवर्ग १२, गा. ९