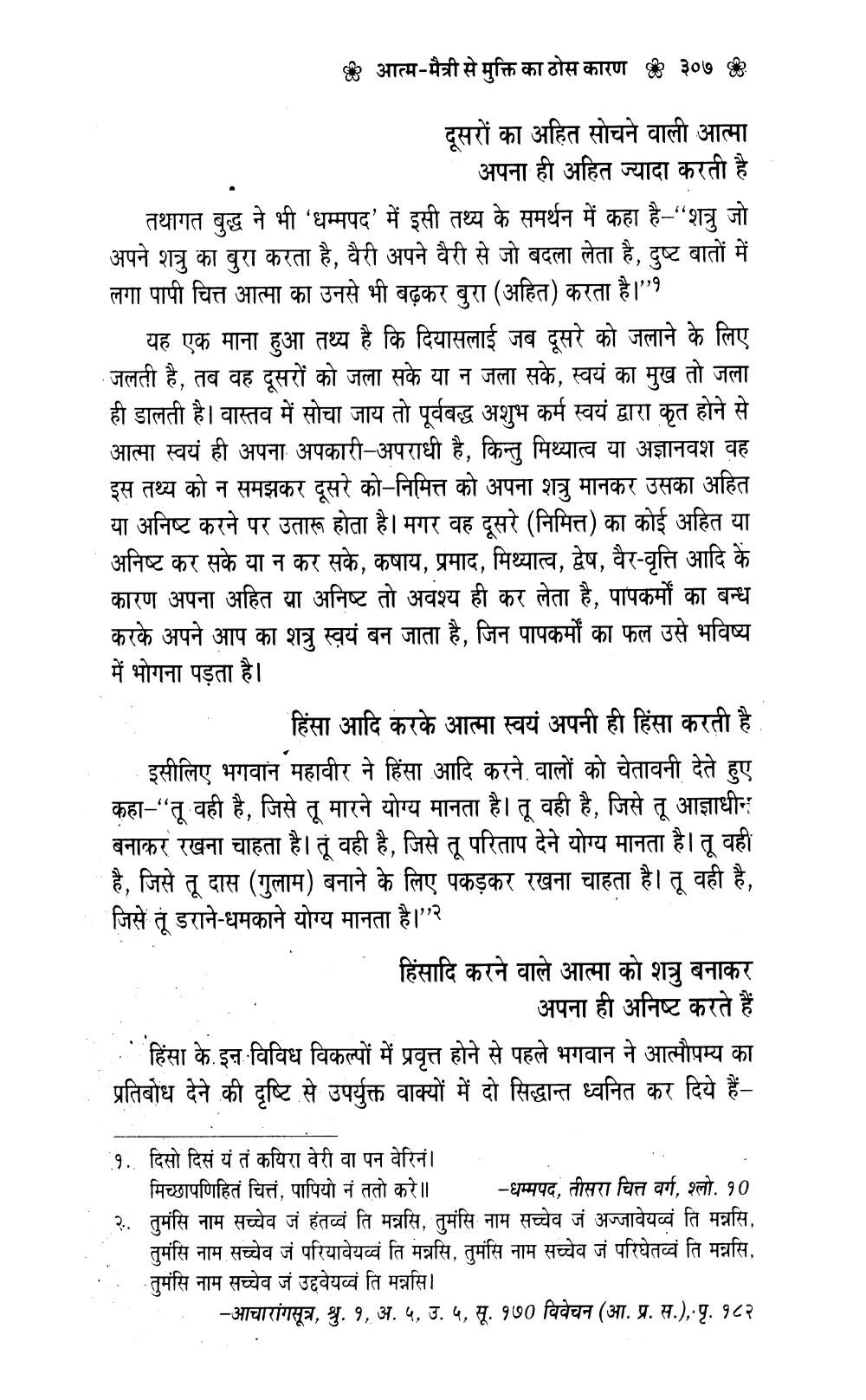________________
* आत्म-मैत्री से मुक्ति का ठोस कारण 8 ३०७ 8
दूसरों का अहित सोचने वाली आत्मा
अपना ही अहित ज्यादा करती है तथागत बुद्ध ने भी 'धम्मपद' में इसी तथ्य के समर्थन में कहा है-"शत्रु जो अपने शत्रु का बुरा करता है, वैरी अपने वैरी से जो बदला लेता है, दुष्ट बातों में लगा पापी चित्त आत्मा का उनसे भी बढ़कर बुरा (अहित) करता है।"
यह एक माना हुआ तथ्य है कि दियासलाई जब दूसरे को जलाने के लिए जलती है, तब वह दूसरों को जला सके या न जला सके, स्वयं का मुख तो जला ही डालती है। वास्तव में सोचा जाय तो पूर्वबद्ध अशुभ कर्म स्वयं द्वारा कृत होने से आत्मा स्वयं ही अपना अपकारी-अपराधी है, किन्तु मिथ्यात्व या अज्ञानवश वह इस तथ्य को न समझकर दूसरे को-निमित्त को अपना शत्रु मानकर उसका अहित या अनिष्ट करने पर उतारू होता है। मगर वह दूसरे (निमित्त) का कोई अहित या अनिष्ट कर सके या न कर सके, कषाय, प्रमाद, मिथ्यात्व, द्वेष, वैर-वृत्ति आदि के कारण अपना अहित या अनिष्ट तो अवश्य ही कर लेता है, पापकर्मों का बन्ध करके अपने आप का शत्रु स्वयं बन जाता है, जिन पापकर्मों का फल उसे भविष्य में भोगना पड़ता है।
हिंसा आदि करके आत्मा स्वयं अपनी ही हिंसा करती है . इसीलिए भगवान महावीर ने हिंसा आदि करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा-“तू वही है, जिसे तू मारने योग्य मानता है। तू वही है, जिसे तू आज्ञाधीन बनाकर रखना चाहता है। तूं वही है, जिसे तू परिताप देने योग्य मानता है। तू वही है, जिसे तू दास (गुलाम) बनाने के लिए पकड़कर रखना चाहता है। तू वही है, जिसे तू डराने-धमकाने योग्य मानता है।"२
हिंसादि करने वाले आत्मा को शत्रु बनाकर
अपना ही अनिष्ट करते हैं ..... हिंसा के. इन विविध विकल्पों में प्रवृत्त होने से पहले भगवान ने आत्मौपम्य का प्रतिबोध देने की दृष्टि से उपर्युक्त वाक्यों में दो सिद्धान्त ध्वनित कर दिये हैं
१. दिसो दिसं यं तं कयिरा वेरी वा पन वेरिनं।
मिच्छापणिहितं चित्तं, पापियो नं ततो करे॥ -धम्मपद, तीसरा चित्त वर्ग, श्लो. १० २.. तुमंसि नाम सच्चेव जं हंतव्वं ति मन्नसि, तुमंसि नाम सच्चेव जं अज्जावेयव्वं ति मन्नसि,
तुमंसि नाम सच्चेव जं परियावेयव्वं ति मन्नसि, तुमंसि नाम सच्चेव जं परिघेतव्वं ति मनसि, तुमंसि नाम सच्चेव जं उद्दवेयव्वं ति मन्नसि।
. -आचारांगसूत्र, श्रु. १, अ. ५, उ. ५, सू. १७0 विवेचन (आ. प्र. स.), पृ. १८२