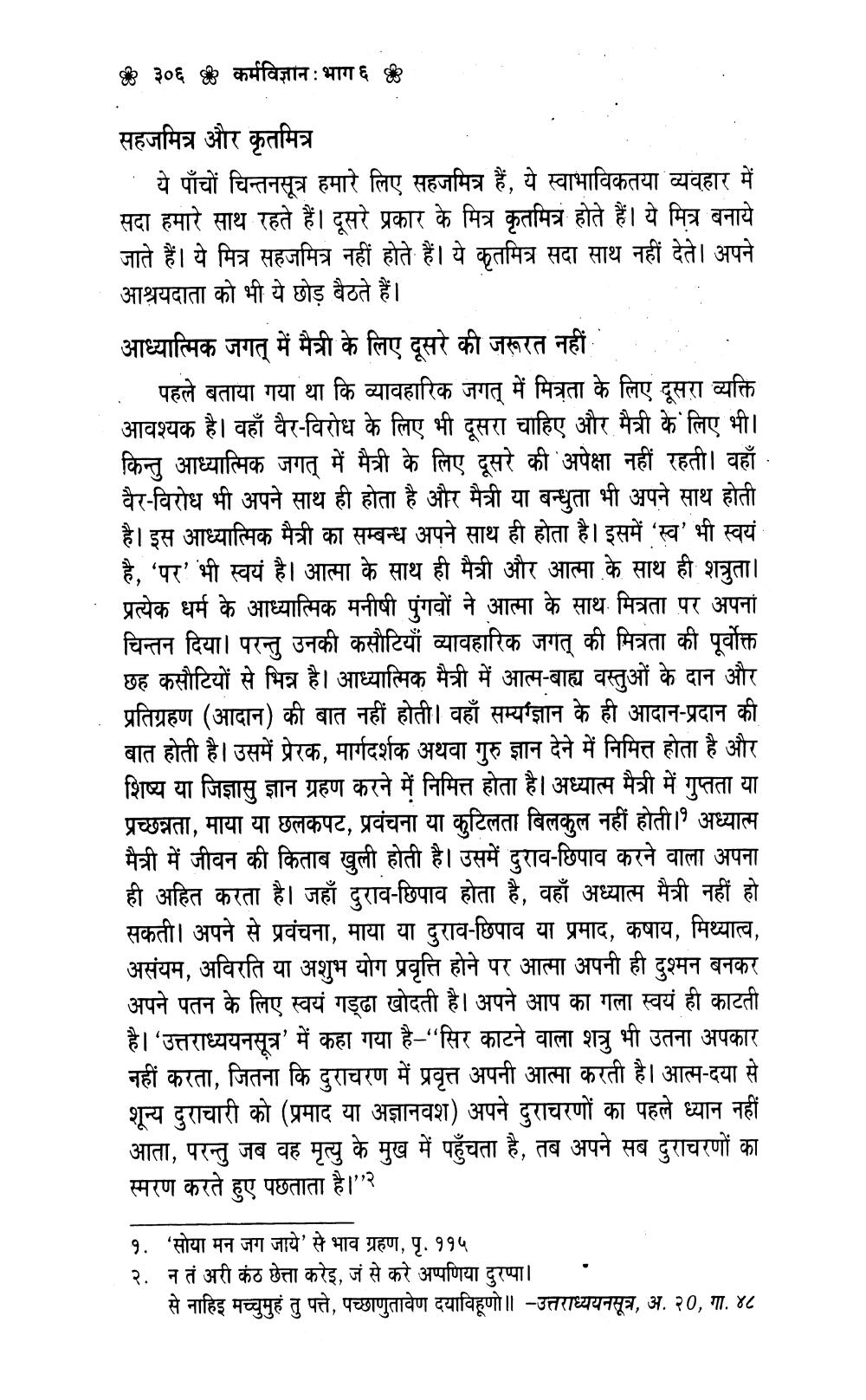________________
ॐ ३०६ * कर्मविज्ञान : भाग ६ 8
सहजमित्र और कृतमित्र - ये पाँचों चिन्तनसूत्र हमारे लिए सहजमित्र हैं, ये स्वाभाविकतया व्यवहार में सदा हमारे साथ रहते हैं। दूसरे प्रकार के मित्र कृतमित्र होते हैं। ये मित्र बनाये जाते हैं। ये मित्र सहजमित्र नहीं होते हैं। ये कृतमित्र सदा साथ नहीं देते। अपने आश्रयदाता को भी ये छोड़ बैठते हैं। आध्यात्मिक जगत् में मैत्री के लिए दूसरे की जरूरत नहीं . पहले बताया गया था कि व्यावहारिक जगत् में मित्रता के लिए दूसरा व्यक्ति
आवश्यक है। वहाँ वैर-विरोध के लिए भी दूसरा चाहिए और मैत्री के लिए भी। किन्तु आध्यात्मिक जगत् में मैत्री के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती। वहाँ :
वैर-विरोध भी अपने साथ ही होता है और मैत्री या बन्धुता भी अपने साथ होती है। इस आध्यात्मिक मैत्री का सम्बन्ध अपने साथ ही होता है। इसमें 'स्व' भी स्वयं है, 'पर' भी स्वयं है। आत्मा के साथ ही मैत्री और आत्मा के साथ ही शत्रुता। प्रत्येक धर्म के आध्यात्मिक मनीषी पुंगवों ने आत्मा के साथ मित्रता पर अपना चिन्तन दिया। परन्तु उनकी कसौटियाँ व्यावहारिक जगत् की मित्रता की पूर्वोक्त छह कसौटियों से भिन्न है। आध्यात्मिक मैत्री में आत्म-बाह्य वस्तुओं के दान और प्रतिग्रहण (आदान) की बात नहीं होती। वहाँ सम्यग्ज्ञान के ही आदान-प्रदान की बात होती है। उसमें प्रेरक, मार्गदर्शक अथवा गुरु ज्ञान देने में निमित्त होता है और शिष्य या जिज्ञासु ज्ञान ग्रहण करने में निमित्त होता है। अध्यात्म मैत्री में गुप्तता या प्रच्छन्नता, माया या छलकपट, प्रवंचना या कुटिलता बिलकुल नहीं होती।' अध्यात्म मैत्री में जीवन की किताब खुली होती है। उसमें दुराव-छिपाव करने वाला अपना ही अहित करता है। जहाँ दुराव-छिपाव होता है, वहाँ अध्यात्म मैत्री नहीं हो सकती। अपने से प्रवंचना, माया या दुराव-छिपाव या प्रमाद, कषाय, मिथ्यात्व, असंयम, अविरति या अशुभ योग प्रवृत्ति होने पर आत्मा अपनी ही दुश्मन बनकर अपने पतन के लिए स्वयं गड्ढा खोदती है। अपने आप का गला स्वयं ही काटती है। 'उत्तराध्ययनसूत्र' में कहा गया है-"सिर काटने वाला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता, जितना कि दुराचरण में प्रवृत्त अपनी आत्मा करती है। आत्म-दया से शून्य दुराचारी को (प्रमाद या अज्ञानवश) अपने दुराचरणों का पहले ध्यान नहीं आता, परन्तु जब वह मृत्यु के मुख में पहुँचता है, तब अपने सब दुराचरणों का स्मरण करते हुए पछताता है।"२
१. 'सोया मन जग जाये' से भाव ग्रहण, पृ. ११५ २. न तं अरी कंठ छेत्ता करेइ, जं से करे अप्पणिया दुरप्पा। .
से नाहिइ मच्चुमुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दयाविहूणो॥ -उत्तराध्ययनसूत्र, अ. २0, गा. ४८