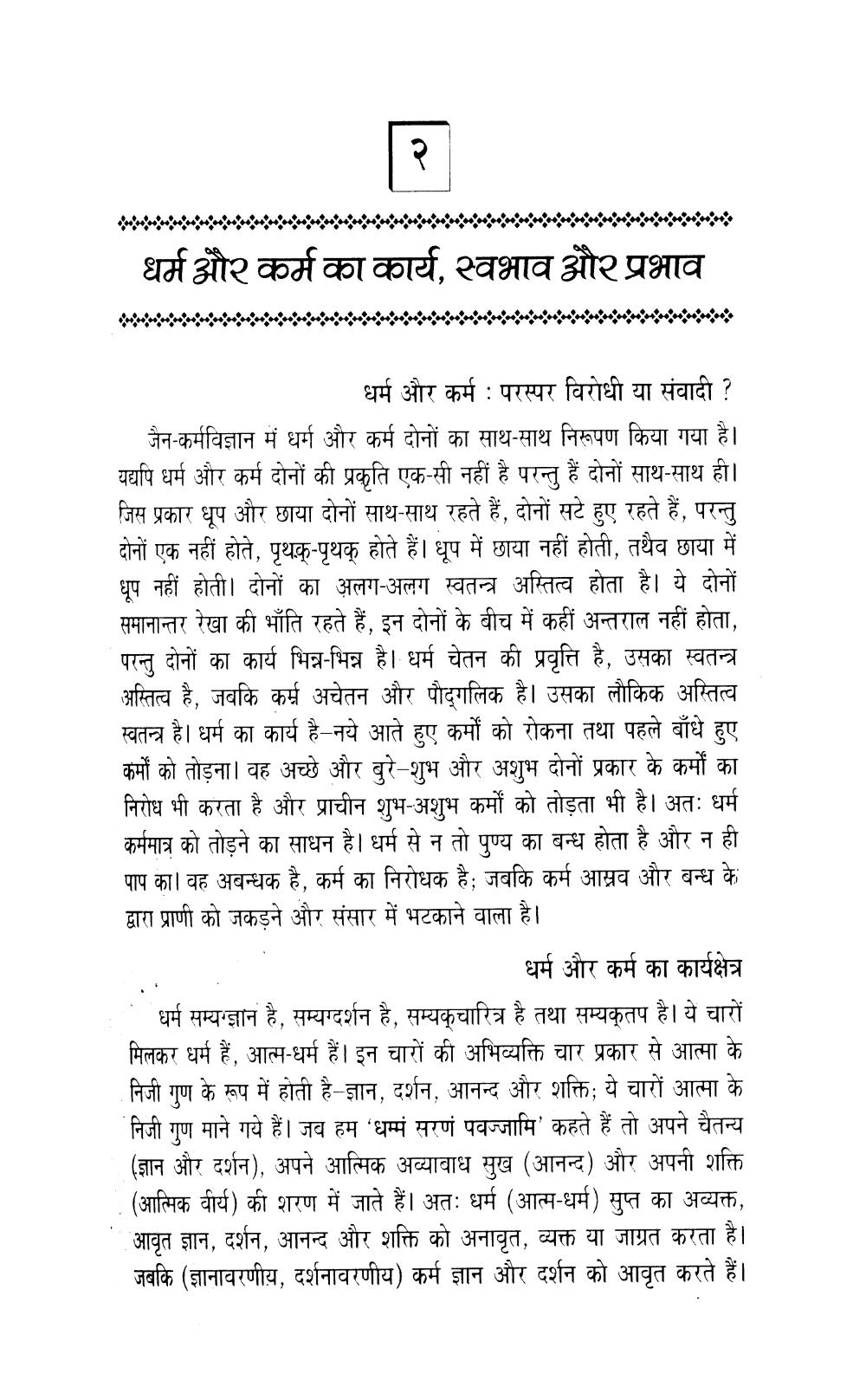________________
धर्म और कर्म का कार्य, स्वभाव और प्रभाव
܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀
धर्म और कर्म : परस्पर विरोधी या संवादी ? जैन-कर्मविज्ञान में धर्म और कर्म दोनों का साथ-साथ निरूपण किया गया है। यद्यपि धर्म और कर्म दोनों की प्रकृति एक-सी नहीं है परन्तु हैं दोनों साथ-साथ ही। जिस प्रकार धूप और छाया दोनों साथ-साथ रहते हैं, दोनों सटे हुए रहते हैं, परन्तु दोनों एक नहीं होते, पृथक्-पृथक् होते हैं। धूप में छाया नहीं होती, तथैव छाया में धूप नहीं होती। दोनों का अलग-अलग स्वतन्त्र अस्तित्व होता है। ये दोनों समानान्तर रेखा की भाँति रहते हैं, इन दोनों के बीच में कहीं अन्तराल नहीं होता, परन्तु दोनों का कार्य भिन्न-भिन्न है। धर्म चेतन की प्रवृत्ति है, उसका स्वतन्त्र अस्तित्व है, जबकि कर्म अचेतन और पौद्गलिक है। उसका लौकिक अस्तित्व स्वतन्त्र है। धर्म का कार्य है-नये आते हुए कर्मों को रोकना तथा पहले बाँधे हुए कर्मों को तोड़ना। वह अच्छे और बुरे-शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का निरोध भी करता है और प्राचीन शुभ-अशुभ कर्मों को तोड़ता भी है। अतः धर्म कर्ममात्र को तोड़ने का साधन है। धर्म से न तो पुण्य का बन्ध होता है और न ही पाप का। वह अबन्धक है, कर्म का निरोधक है; जबकि कर्म आस्रव और बन्ध के द्वारा प्राणी को जकड़ने और संसार में भटकाने वाला है।
धर्म और कर्म का कार्यक्षेत्र धर्म सम्यग्ज्ञान है, सम्यग्दर्शन है, सम्यकचारित्र है तथा सम्यकतप है। ये चारों मिलकर धर्म हैं, आत्म-धर्म हैं। इन चारों की अभिव्यक्ति चार प्रकार से आत्मा के निजी गुण के रूप में होती है-ज्ञान, दर्शन, आनन्द और शक्ति; ये चारों आत्मा के निजी गण माने गये हैं। जब हम ‘धम्म सरणं पवज्जामि' कहते हैं तो अपने चैतन्य (ज्ञान और दर्शन), अपने आत्मिक अव्यावाध सुख (आनन्द) और अपनी शक्ति (आत्मिक वीर्य) की शरण में जाते हैं। अतः धर्म (आत्म-धर्म) सुप्त का अव्यक्त, आवृत ज्ञान, दर्शन, आनन्द और शक्ति को अनावृत, व्यक्त या जाग्रत करता है। जबकि (ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय) कर्म ज्ञान और दर्शन को आवृत करते हैं।