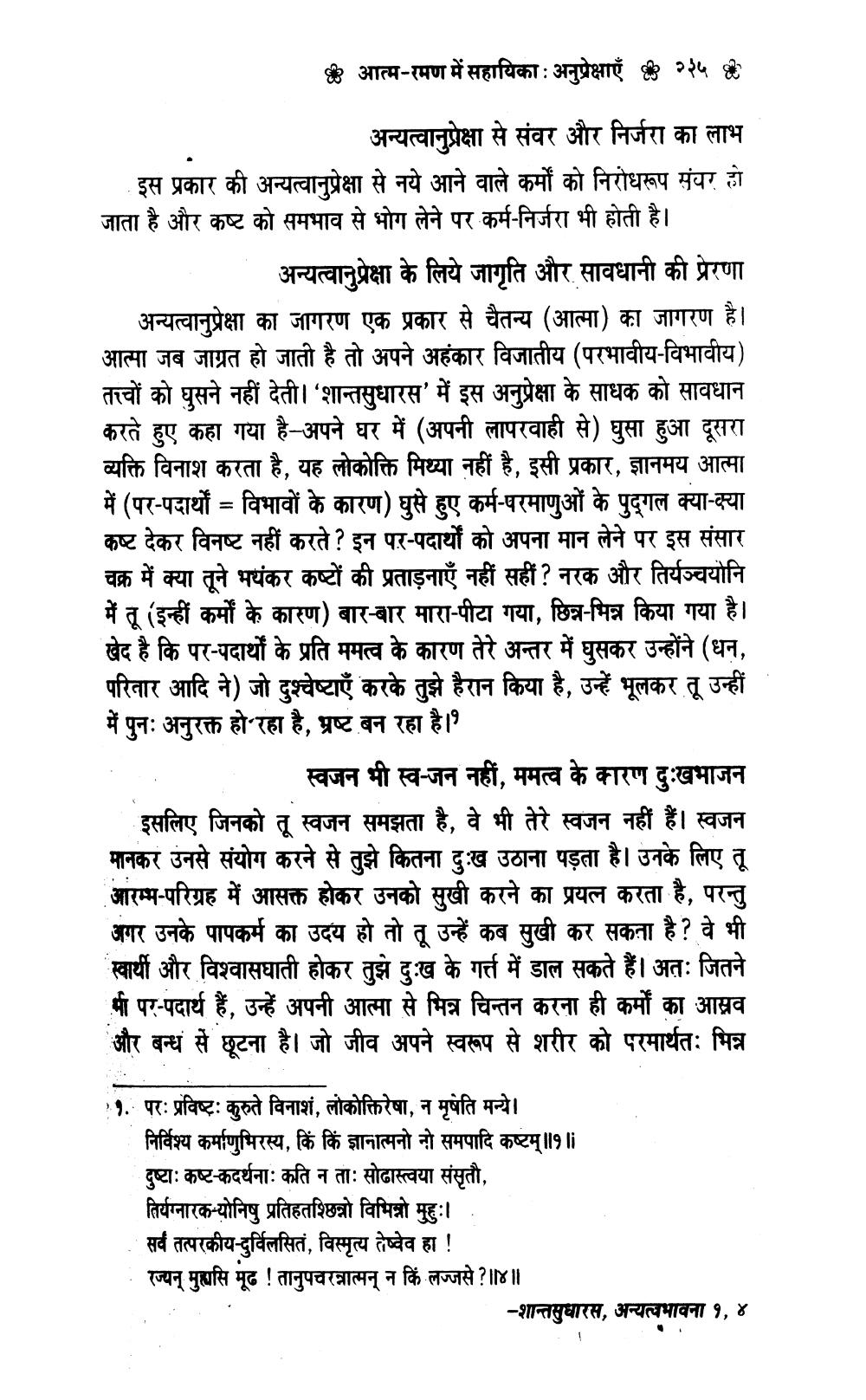________________
® आत्म-रमण में सहायिका : अनुप्रेक्षाएँ * २२५ .
___अन्यत्वानुप्रेक्षा से संवर और निर्जरा का लाभ इस प्रकार की अन्यत्वानुप्रेक्षा से नये आने वाले कर्मों को निरोधरूप संवर हो जाता है और कष्ट को समभाव से भोग लेने पर कर्म-निर्जरा भी होती है।
__ अन्यत्वानुप्रेक्षा के लिये जागृति और सावधानी की प्रेरणा अन्यत्वानुप्रेक्षा का जागरण एक प्रकार से चैतन्य (आत्मा) का जागरण है। आत्मा जब जाग्रत हो जाती है तो अपने अहंकार विजातीय (परभावीय-विभावीय) तत्वों को घुसने नहीं देती। 'शान्तसुधारस' में इस अनुप्रेक्षा के साधक को सावधान करते हुए कहा गया है-अपने घर में (अपनी लापरवाही से) घुसा हुआ दूसरा व्यक्ति विनाश करता है, यह लोकोक्ति मिथ्या नहीं है, इसी प्रकार, ज्ञानमय आत्मा में (पर-पदार्थों = विभावों के कारण) घुसे हुए कर्म-परमाणुओं के पुद्गल क्या-क्या कष्ट देकर विनष्ट नहीं करते? इन पर-पदार्थों को अपना मान लेने पर इस संसार चक्र में क्या तूने भयंकर कष्टों की प्रताड़नाएँ नहीं सहीं? नरक और तिर्यञ्चयोनि में तू (इन्हीं कर्मों के कारण) बार-बार मारा-पीटा गया, छिन्न-भिन्न किया गया है। खेद है कि पर-पदार्थों के प्रति ममत्व के कारण तेरे अन्तर में घुसकर उन्होंने (धन, परितार आदि ने) जो दुश्चेष्टाएँ करके तुझे हैरान किया है, उन्हें भूलकर तू उन्हीं में पुनः अनुरक्त हो रहा है, भ्रष्ट बन रहा है।
स्वजन भी स्व-जन नहीं, ममत्व के कारण दुःखभाजन इसलिए जिनको तू स्वजन समझता है, वे भी तेरे स्वजन नहीं हैं। स्वजन मानकर उनसे संयोग करने से तुझे कितना दुःख उठाना पड़ता है। उनके लिए तू आरम्भ-परिग्रह में आसक्त होकर उनको सुखी करने का प्रयत्न करता है, परन्तु अगर उनके पापकर्म का उदय हो तो तू उन्हें कब सुखी कर सकता है? वे भी स्वार्थी और विश्वासघाती होकर तुझे दुःख के गर्त में डाल सकते हैं। अतः जितने मी पर-पदार्थ हैं, उन्हें अपनी आत्मा से भिन्न चिन्तन करना ही कर्मों का आम्रव और बन्धं से छूटना है। जो जीव अपने स्वरूप से शरीर को परमार्थतः भिन्न
१. परः प्रविष्टः कुरुते विनाशं, लोकोक्तिरेषा, न मषेति मन्ये। निर्विश्य कर्माणुभिरस्य, किं किं ज्ञानात्मनो नो समपादि कष्टम्॥१॥ दुष्टाः कष्ट-कदर्थनाः कति न ताः सोढास्त्वया संसृतौ, तिर्यग्नारक-योनिषु प्रतिहतश्छिन्नो विभिन्नो मुहुः। . सर्वं तत्परकीय-दुर्विलसितं, विस्मृत्य तेष्वेव हा ! रज्यन् मुह्यसि मूढ ! तानुपचरन्नात्मन् न किं लज्जसे?॥४॥
-शान्तसुधारस, अन्यत्वभावना १,४