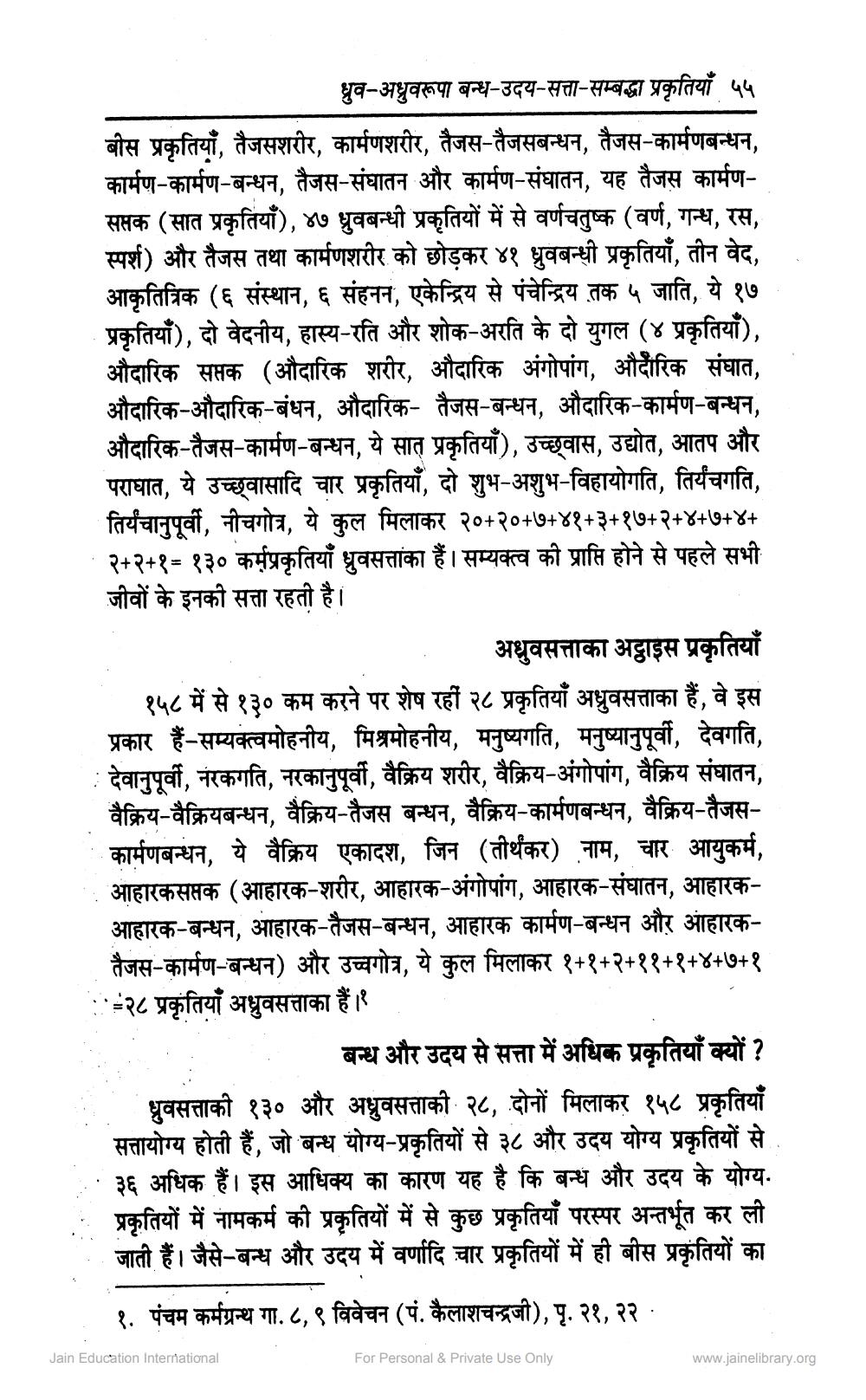________________
ध्रुव-अध्रुवरूपा बन्ध-उदय-सत्ता-सम्बद्धा प्रकृतियाँ ५५
बीस प्रकृतियाँ, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, तैजस-तैजसबन्धन, तैजस-कार्मणबन्धन कार्मण-कार्मण-बन्धन, तैजस-संघातन और कार्मण-संघातन, यह तैजस कार्मणसप्तक (सात प्रकृतियाँ), ४७ ध्रुवबन्धी प्रकृतियों में से वर्णचतुष्क (वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श) और तैजस तथा कार्मणशरीर को छोड़कर ४१ ध्रुवबन्धी प्रकृतियाँ, तीन वेद, आकृतित्रिक (६ संस्थान, ६ संहनन, एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक ५ जाति, ये १७ प्रकृतियाँ), दो वेदनीय, हास्य-रति और शोक-अरति के दो युगल (४ प्रकृतियाँ), औदारिक सप्तक (औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, औदीरिक संघात, औदारिक-औदारिक-बंधन, औदारिक- तैजस-बन्धन, औदारिक-कार्मण-बन्धन,
औदारिक-तैजस-कार्मण-बन्धन, ये सात प्रकृतियाँ), उच्छ्वास, उद्योत, आतप और पराघात, ये उच्छ्वासादि चार प्रकृतियाँ, दो शुभ-अशुभ-विहायोगति, तिर्यंचगति, तिर्यंचानपूर्वी, नीचगोत्र, ये कुल मिलाकर २०+२०+७+४१+३+१७+२+४+७+४+ २+२+१= १३० कर्मप्रकृतियाँ ध्रुवसत्ताका हैं। सम्यक्त्व की प्राप्ति होने से पहले सभी जीवों के इनकी सत्ता रहती है।
. अध्रुवसत्ताका अट्ठाइस प्रकृतियाँ १५८ में से १३० कम करने पर शेष रहीं २८ प्रकृतियाँ अध्रुवसत्ताका हैं, वे इस प्रकार हैं-सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, देवगति, देवानुपूर्वी, नरकगति, नरकानुपूर्वी, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय-अंगोपांग, वैक्रिय संघातन, वैक्रिय-वैक्रियबन्धन, वैक्रिय-तैजस बन्धन, वैक्रिय-कार्मणबन्धन, वैक्रिय-तैजसकार्मणबन्धन, ये वैक्रिय एकादश, जिन (तीर्थंकर) नाम, चार आयुकर्म, आहारकसप्तक (आहारक-शरीर, आहारक-अंगोपांग, आहारक-संघातन, आहारकआहारक-बन्धन, आहारक-तैजस-बन्धन, आहारक कार्मण-बन्धन और आहारकतैजस-कार्मण-बन्धन) और उच्चगोत्र, ये कुल मिलाकर १+१+२+११+१+४+७+१ · · २८ प्रकृतियाँ अध्रुवसत्ताका हैं।
बन्ध और उदय से सत्ता में अधिक प्रकृतियाँ क्यों ? ध्रुवसत्ताकी १३० और अध्रुवसत्ताकी २८, दोनों मिलाकर १५८ प्रकृतियाँ सत्तायोग्य होती हैं, जो बन्ध योग्य-प्रकृतियों से ३८ और उदय योग्य प्रकृतियों से • ३६ अधिक हैं। इस आधिक्य का कारण यह है कि बन्ध और उदय के योग्य.
प्रकृतियों में नामकर्म की प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियाँ परस्पर अन्तर्भूत कर ली ____ जाती हैं। जैसे-बन्ध और उदय में वर्णादि चार प्रकृतियों में ही बीस प्रकृतियों का
१. पंचम कर्मग्रन्थ गा. ८, ९ विवेचन (पं. कैलाशचन्द्रजी), पृ. २१, २२ .
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org