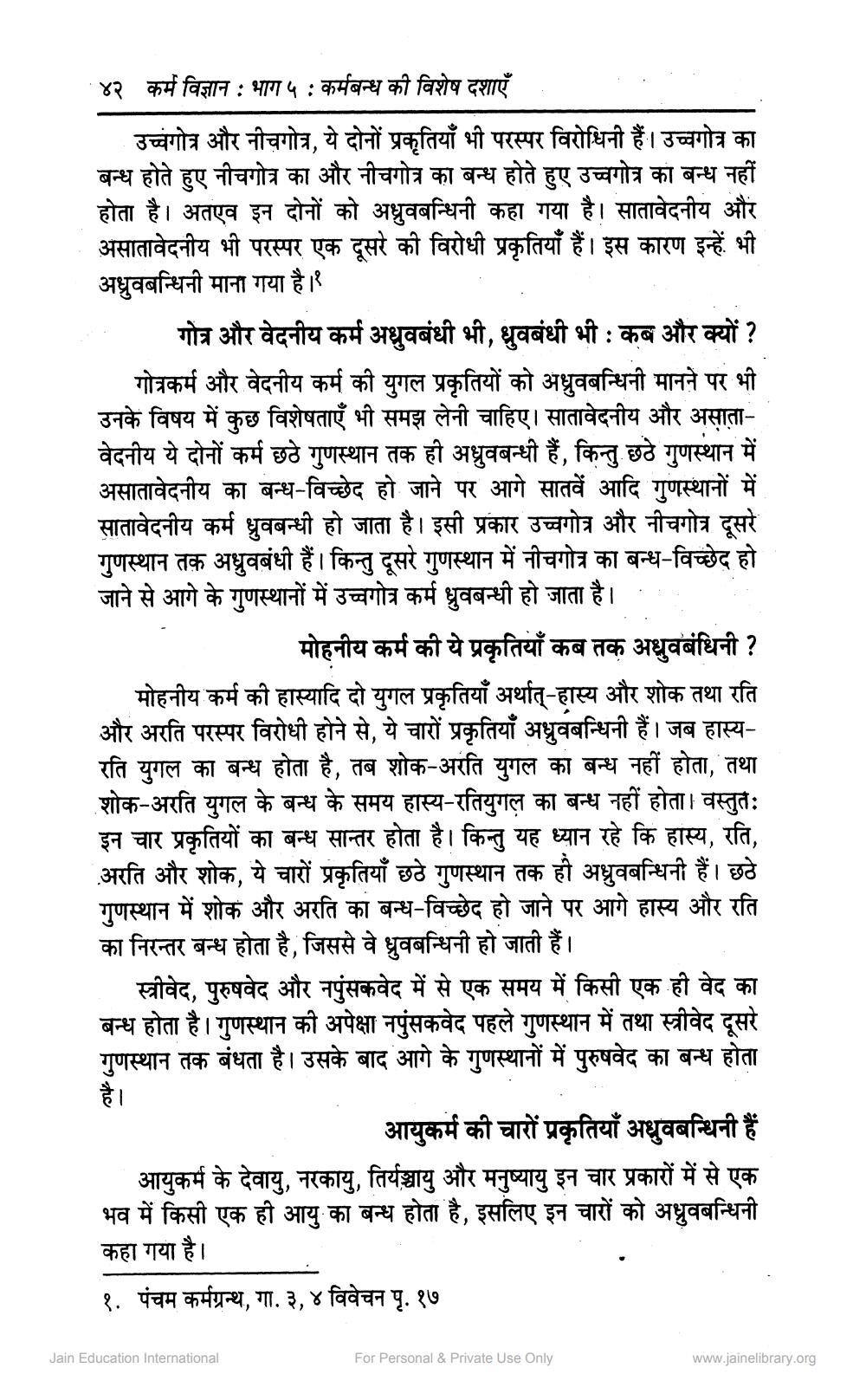________________
४२ कर्म विज्ञान : भाग ५ : कर्मबन्ध की विशेष दशाएँ
उच्चगोत्र और नीचगोत्र, ये दोनों प्रकृतियाँ भी परस्पर विरोधिनी हैं। उच्चगोत्र का बन्ध होते हुए नीचगोत्र का और नीचगोत्र का बन्ध होते हुए उच्चगोत्र का बन्ध नहीं होता है। अतएव इन दोनों को अध्रुवबन्धिनी कहा गया है। सातावेदनीय और असातावेदनीय भी परस्पर एक दूसरे की विरोधी प्रकृतियाँ हैं । इस कारण इन्हें भी अध्रुवबन्धिनी माना गया है । १
hi और वेदनीय कर्म अध्रुवबंधी भी, ध्रुवबंधी भी : कब और क्यों ?
गोत्रकर्म और वेदनीय कर्म की युगल प्रकृतियों को अध्रुवबन्धिनी मानने पर भी उनके विषय में कुछ विशेषताएँ भी समझ लेनी चाहिए । सातावेदनीय और असातावेदनीय ये दोनों कर्म छठे गुणस्थान तक ही अध्रुवबन्धी हैं, किन्तु छठे गुणस्थान में असातावेदनीय का बन्ध-विच्छेद हो जाने पर आगे सातवें आदि गुणस्थानों में सातावेदनीय कर्म ध्रुवबन्धी हो जाता है। इसी प्रकार उच्चगोत्र और नीचगोत्र दूसरे गुणस्थान तक अध्रुवबंधी हैं । किन्तु दूसरे गुणस्थान में नीचगोत्र का बन्ध-विच्छेद हो जाने से आगे के गुणस्थानों में उच्चगोत्र कर्म ध्रुवबन्धी हो जाता है।
मोहनीय कर्म की ये प्रकृतियाँ कब तक अध्रुवबंधिनी ?
-
मोहनीय कर्म की हास्यादि दो युगल प्रकृतियाँ अर्थात् - हास्य और शोक तथा रति और अरति परस्पर विरोधी होने से, ये चारों प्रकृतियाँ अध्रुवबन्धिनी हैं। जब हास्यरति युगल का बन्ध होता है, तब शोक - अरति युगल का बन्ध नहीं होता, तथा शोक-अरति युगल के बन्ध के समय हास्य-रतियुगल का बन्ध नहीं होता । वस्तुतः इन चार प्रकृतियों का बन्ध सान्तर होता है । किन्तु यह ध्यान रहे कि हास्य, रति, अरति और शोक, ये चारों प्रकृतियाँ छठे गुणस्थान तक ही अध्रुवबन्धिनी हैं। छठे गुणस्थान में शोक और अरति का बन्ध-विच्छेद हो जाने पर आगे हास्य और रति का निरन्तर बन्ध होता है, जिससे वे ध्रुवबन्धिनी हो जाती हैं।
स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद में से एक समय में किसी एक ही वेद का बन्ध होता है। गुणस्थान की अपेक्षा नपुंसकवेद पहले गुणस्थान में तथा स्त्रीवेद दूसरे गुणस्थान तक बंधता है। उसके बाद आगे के गुणस्थानों में पुरुषवेद का बन्ध होता
है।
आयुकर्म की चारों प्रकृतियाँ अध्रुवबन्धिनी हैं
आयुकर्म के देवायु, नरकायु, तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु इन चार प्रकारों में से एक भव में किसी एक ही आयु का बन्ध होता है, इसलिए इन चारों को अध्रुवबन्धिनी कहा गया है।
१. पंचम कर्मग्रन्थ, गा. ३, ४ विवेचन पृ. १७
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org