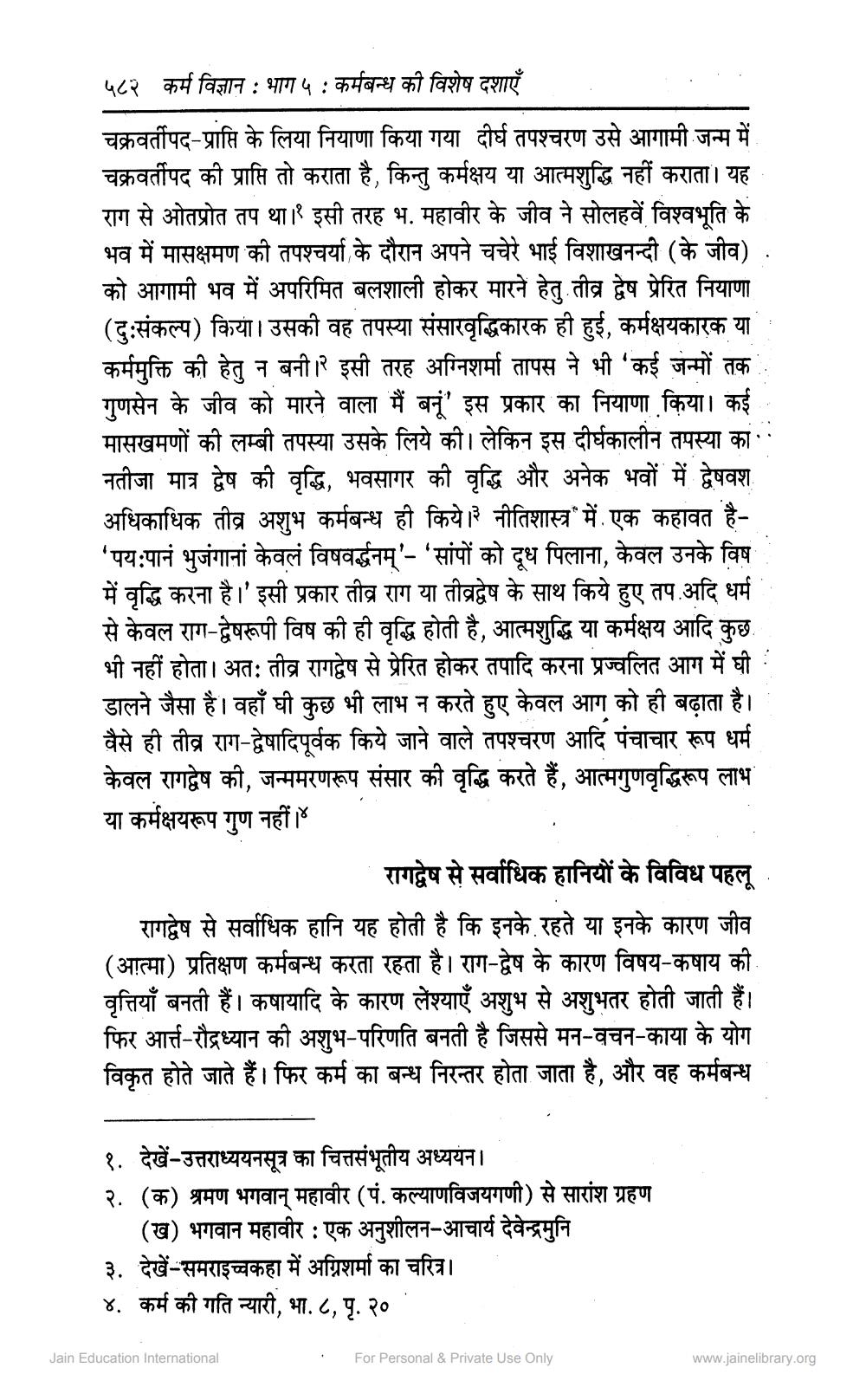________________
५८२ कर्म विज्ञान : भाग ५ : कर्मबन्ध की विशेष दशाएँ चक्रवर्तीपद-प्राप्ति के लिया नियाणा किया गया दीर्घ तपश्चरण उसे आगामी जन्म में चक्रवर्तीपद की प्राप्ति तो कराता है, किन्तु कर्मक्षय या आत्मशुद्धि नहीं कराता। यह राग से ओतप्रोत तप था। इसी तरह भ. महावीर के जीव ने सोलहवें विश्वभूति के भव में मासक्षमण की तपश्चर्या के दौरान अपने चचेरे भाई विशाखनन्दी (के जीव) . को आगामी भव में अपरिमित बलशाली होकर मारने हेतु तीव्र द्वेष प्रेरित नियाणा (दुःसंकल्प) किया। उसकी वह तपस्या संसारवृद्धिकारक ही हुई, कर्मक्षयकारक या कर्ममुक्ति की हेतु न बनी। इसी तरह अग्निशर्मा तापस ने भी 'कई जन्मों तक गुणसेन के जीव को मारने वाला मैं बनूं' इस प्रकार का नियाणा किया। कई मासखमणों की लम्बी तपस्या उसके लिये की। लेकिन इस दीर्घकालीन तपस्या का नतीजा मात्र द्वेष की वृद्धि, भवसागर की वृद्धि और अनेक भवों में द्वेषवश
अधिकाधिक तीव्र अशुभ कर्मबन्ध ही किये। नीतिशास्त्र में एक कहावत है'पयःपानं भुजंगानां केवलं विषवर्द्धनम्'- 'सांपों को दूध पिलाना, केवल उनके विष में वृद्धि करना है।' इसी प्रकार तीव्र राग या तीव्रद्वेष के साथ किये हुए तप अदि धर्म से केवल राग-द्वेषरूपी विष की ही वृद्धि होती है, आत्मशुद्धि या कर्मक्षय आदि कुछ भी नहीं होता। अतः तीव्र रागद्वेष से प्रेरित होकर तपादि करना प्रज्वलित आग में घी . डालने जैसा है। वहाँ घी कुछ भी लाभ न करते हुए केवल आग को ही बढ़ाता है। वैसे ही तीव्र राग-द्वेषादिपूर्वक किये जाने वाले तपश्चरण आदि पंचाचार रूप धर्म केवल रागद्वेष की, जन्ममरणरूप संसार की वृद्धि करते हैं, आत्मगुणवृद्धिरूप लाभ या कर्मक्षयरूप गुण नहीं।
रागद्वेष से सर्वाधिक हानियों के विविध पहलू रागद्वेष से सर्वाधिक हानि यह होती है कि इनके रहते या इनके कारण जीव (आत्मा) प्रतिक्षण कर्मबन्ध करता रहता है। राग-द्वेष के कारण विषय-कषाय की वृत्तियाँ बनती हैं। कषायादि के कारण लेश्याएँ अशुभ से अशुभतर होती जाती हैं। फिर आर्त्त-रौद्रध्यान की अशुभ-परिणति बनती है जिससे मन-वचन-काया के योग विकृत होते जाते हैं। फिर कर्म का बन्ध निरन्तर होता जाता है, और वह कर्मबन्ध
१. देखें-उत्तराध्ययनसूत्र का चित्तसंभूतीय अध्ययन। २. (क) श्रमण भगवान् महावीर (पं. कल्याणविजयगणी) से सारांश ग्रहण
(ख) भगवान महावीर : एक अनुशीलन-आचार्य देवेन्द्रमुनि ३. देखें-समराइच्चकहा में अग्निशर्मा का चरित्र। ४. कर्म की गति न्यारी, भा.८, पृ. २०
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org