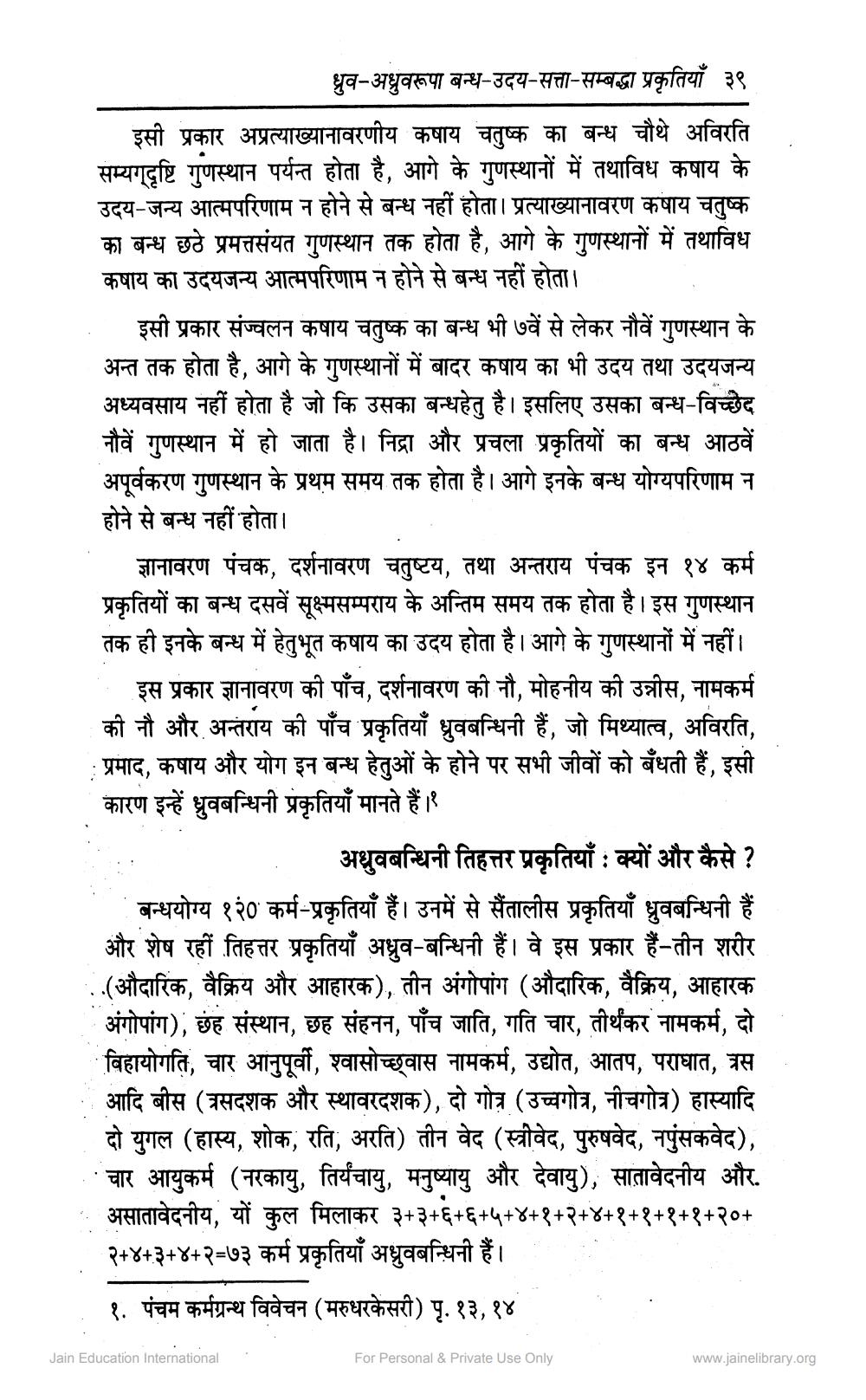________________
ध्रुव-अध्रुवरूपा बन्ध-उदय-सत्ता-सम्बद्धा प्रकृतियाँ ३९ इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय चतुष्क का बन्ध चौथे अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थान पर्यन्त होता है, आगे के गुणस्थानों में तथाविध कषाय के उदय-जन्य आत्मपरिणाम न होने से बन्ध नहीं होता। प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क का बन्ध छठे प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक होता है, आगे के गुणस्थानों में तथाविध कषाय का उदयजन्य आत्मपरिणाम न होने से बन्ध नहीं होता।
इसी प्रकार संज्वलन कषाय चतुष्क का बन्ध भी ७वें से लेकर नौवें गुणस्थान के अन्त तक होता है, आगे के गुणस्थानों में बादर कषाय का भी उदय तथा उदयजन्य अध्यवसाय नहीं होता है जो कि उसका बन्धहेतु है। इसलिए उसका बन्ध-विच्छेद नौवें गुणस्थान में हो जाता है। निद्रा और प्रचला प्रकृतियों का बन्ध आठवें अपूर्वकरण गुणस्थान के प्रथम समय तक होता है। आगे इनके बन्ध योग्यपरिणाम न होने से बन्ध नहीं होता। ___ ज्ञानावरण पंचक, दर्शनावरण चतुष्टय, तथा अन्तराय पंचक इन १४ कर्म प्रकृतियों का बन्ध दसवें सूक्ष्मसम्पराय के अन्तिम समय तक होता है। इस गुणस्थान तक ही इनके बन्ध में हेतुभूत कषाय का उदय होता है। आगे के गुणस्थानों में नहीं।
इस प्रकार ज्ञानावरण की पाँच, दर्शनावरण की नौ, मोहनीय की उन्नीस, नामकर्म की नौ और अन्तराय की पाँच प्रकृतियाँ ध्रुवबन्धिनी हैं, जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इन बन्ध हेतुओं के होने पर सभी जीवों को बंधती हैं, इसी कारण इन्हें ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ मानते हैं।
. अध्रुवबन्धिनी तिहत्तर प्रकृतियाँ : क्यों और कैसे ? बन्धयोग्य १२० कर्म-प्रकृतियाँ हैं। उनमें से सैंतालीस प्रकृतियाँ ध्रुवबन्धिनी हैं और शेष रहीं तिहत्तर प्रकृतियाँ अध्रुव-बन्धिनी हैं। वे इस प्रकार हैं-तीन शरीर (औदारिक, वैक्रिय और आहारक), तीन अंगोपांग (औदारिक, वैक्रिय, आहारक अंगोपांग), छंह संस्थान, छह संहनन, पाँच जाति, गति चार, तीर्थंकर नामकर्म, दो विहायोगति, चार आनुपूर्वी, श्वासोच्छ्वास नामकर्म, उद्योत, आतप, पराघात, त्रस आदि बीस (त्रसदशक और स्थावरदशक), दो गोत्र (उच्चगोत्र, नीचगोत्र) हास्यादि दो युगल (हास्य, शोक, रति, अरति) तीन वेद (स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद), 'चार आयुकर्म (नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु), सातावेदनीय और. .. असातावेदनीय, यों कुल मिलाकर ३+३+६+६+५+४+१+२+४+१+१+१+१+२०+
२+४+३+४+२=७३ कर्म प्रकृतियाँ अध्रुवबन्धिनी हैं। १. पंचम कर्मग्रन्थ विवेचन (मरुधरकेसरी) पृ. १३, १४
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org