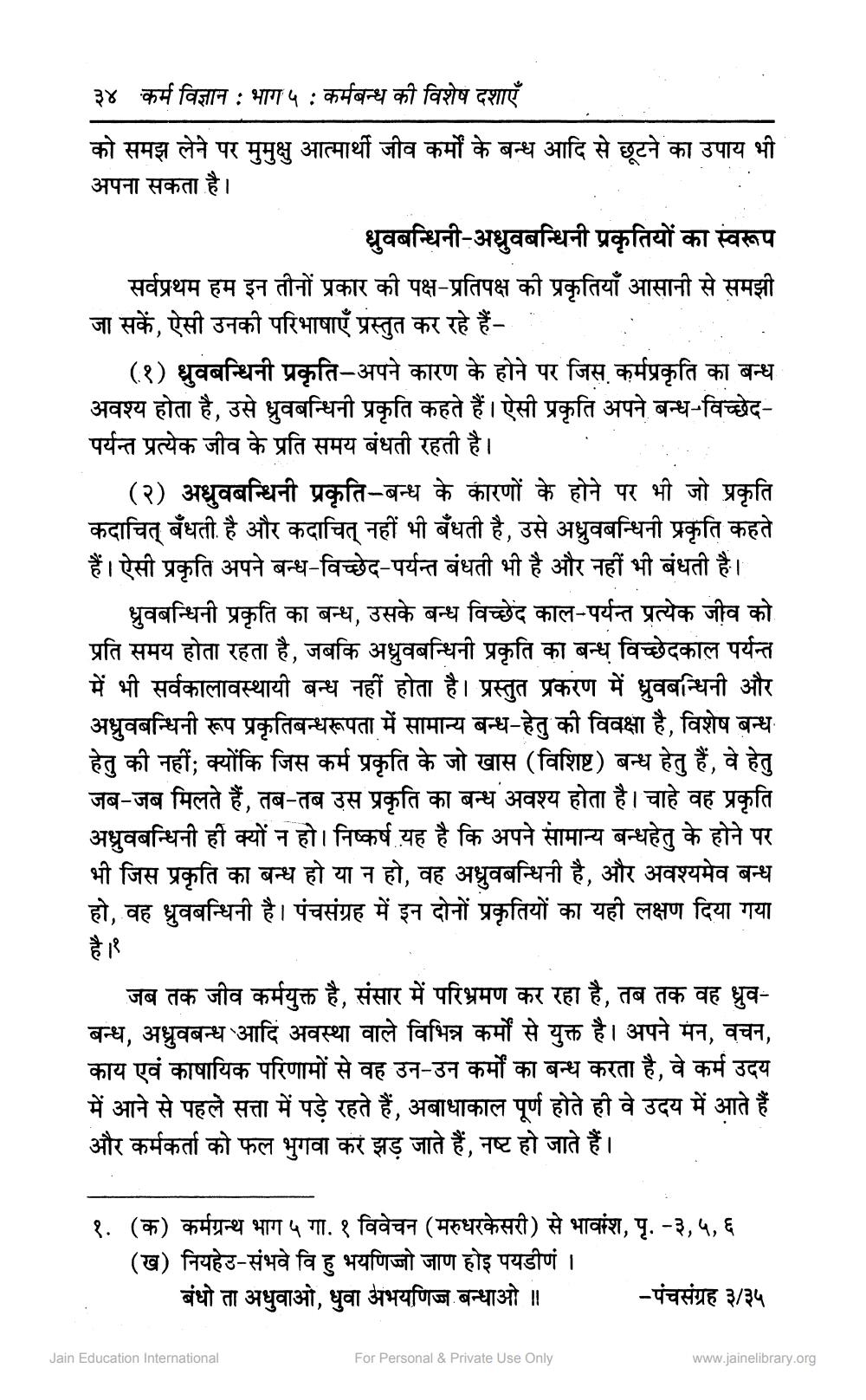________________
३४ कर्म विज्ञान : भाग ५ : कर्मबन्ध की विशेष दशाएँ को समझ लेने पर मुमुक्षु आत्मार्थी जीव कर्मों के बन्ध आदि से छूटने का उपाय भी अपना सकता है।
ध्रुवबन्धिनी-अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों का स्वरूप सर्वप्रथम हम इन तीनों प्रकार की पक्ष-प्रतिपक्ष की प्रकृतियाँ आसानी से समझी जा सकें, ऐसी उनकी परिभाषाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं
(१) ध्रुवबन्धिनी प्रकृति-अपने कारण के होने पर जिस कर्मप्रकृति का बन्ध अवश्य होता है, उसे ध्रुवबन्धिनी प्रकृति कहते हैं। ऐसी प्रकृति अपने बन्ध-विच्छेदपर्यन्त प्रत्येक जीव के प्रति समय बंधती रहती है।
(२) अध्रुवबन्धिनी प्रकृति-बन्ध के कारणों के होने पर भी जो प्रकृति कदाचित् बँधती है और कदाचित् नहीं भी बंधती है, उसे अध्रुवबन्धिनी प्रकृति कहते हैं। ऐसी प्रकृति अपने बन्ध-विच्छेद-पर्यन्त बंधती भी है और नहीं भी बंधती है।
ध्रुवबन्धिनी प्रकृति का बन्ध, उसके बन्ध विच्छेद काल-पर्यन्त प्रत्येक जीव को प्रति समय होता रहता है, जबकि अध्रुवबन्धिनी प्रकृति का बन्ध विच्छेदकाल पर्यन्त में भी सर्वकालावस्थायी बन्ध नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ध्रुवबन्धिनी और अध्रुवबन्धिनी रूप प्रकृतिबन्धरूपता में सामान्य बन्ध-हेतु की विवक्षा है, विशेष बन्ध हेतु की नहीं; क्योंकि जिस कर्म प्रकृति के जो खास (विशिष्ट) बन्ध हेतु हैं, वे हेतु जब-जब मिलते हैं, तब-तब उस प्रकृति का बन्ध अवश्य होता है। चाहे वह प्रकृति अध्रुवबन्धिनी ही क्यों न हो। निष्कर्ष यह है कि अपने सामान्य बन्धहेतु के होने पर भी जिस प्रकृति का बन्ध हो या न हो, वह अध्रुवबन्धिनी है, और अवश्यमेव बन्ध हो, वह ध्रुवबन्धिनी है। पंचसंग्रह में इन दोनों प्रकृतियों का यही लक्षण दिया गया है।
जब तक जीव कर्मयुक्त है, संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तब तक वह ध्रुवबन्ध, अध्रुवबन्ध आदि अवस्था वाले विभिन्न कर्मों से युक्त है। अपने मन, वचन, काय एवं काषायिक परिणामों से वह उन-उन कर्मों का बन्ध करता है, वे कर्म उदय में आने से पहले सत्ता में पड़े रहते हैं, अबाधाकाल पूर्ण होते ही वे उदय में आते हैं और कर्मकर्ता को फल भुगवा कर झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
१. (क) कर्मग्रन्थ भाग ५ गा. १ विवेचन (मरुधरकेसरी) से भावंश, पृ. -३,५,६ (ख) नियहेउ-संभवे वि हु भयणिज्जो जाण होइ पयडीणं ।
बंधो ता अधुवाओ, धुवा अभयणिज बन्धाओ ॥ -पंचसंग्रह ३/३५
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org