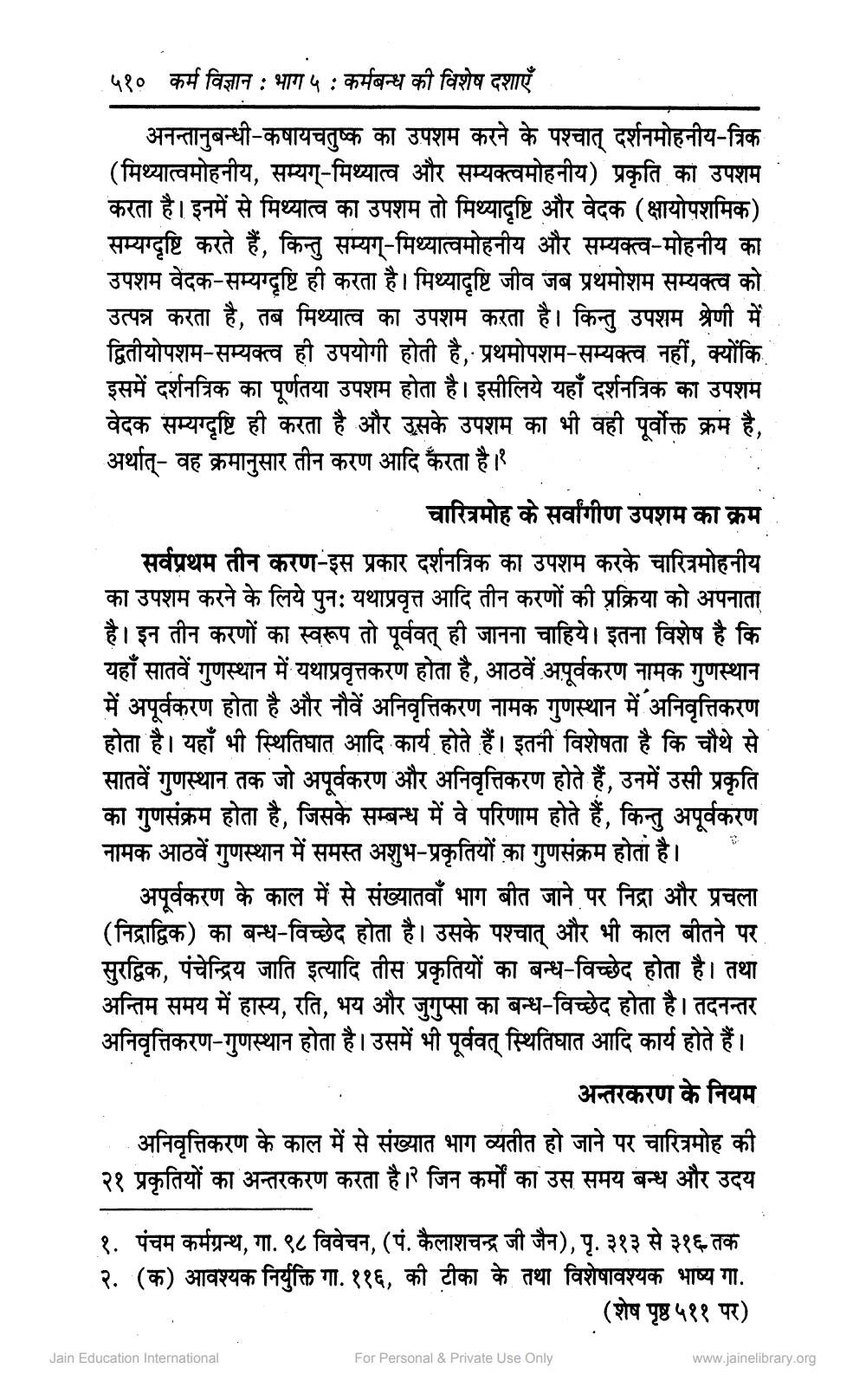________________
५१० कर्म विज्ञान : भाग ५ : कर्मबन्ध की विशेष दशाएँ
अनन्तानुबन्धी- कषायचतुष्क का उपशम करने के पश्चात् दर्शनमोहनीय- त्रिक (मिथ्यात्वमोहनीय, सम्यग् - मिथ्यात्व और सम्यक्त्वमोहनीय) प्रकृति का उपशम करता है। इनमें से मिथ्यात्व का उपशम तो मिथ्यादृष्टि और वेदक ( क्षायोपशमिक) सम्यग्दृष्टि करते हैं, किन्तु सम्यग् - मिध्यात्वमोहनीय और सम्यक्त्व - मोहनीय का उपशम वेदक-सम्यग्दृष्टि ही करता है । मिथ्यादृष्टि जीव जब प्रथमोशम सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है, तब मिथ्यात्व का उपशम करता है। किन्तु उपशम श्रेणी में द्वितीयोपशम-सम्यक्त्व ही उपयोगी होती है, प्रथमोपशम- सम्यक्त्व नहीं, क्योंकि.. इसमें दर्शनत्रिक का पूर्णतया उपशम होता है । इसीलिये यहाँ दर्शनत्रिक का उपशम वेदक सम्यग्दृष्टि ही करता है और उसके उपशम का भी वही पूर्वोक्त क्रम है, अर्थात् - वह क्रमानुसार तीन करण आदि करता है ।
चारित्रमोह के सर्वांगीण उपशम का क्रम
सर्वप्रथम तीन करण- इस प्रकार दर्शनत्रिक का उपशम करके चारित्रमोहनीय का उपशम करने के लिये पुनः यथाप्रवृत्त आदि तीन करणों की प्रक्रिया को अपनाता है। इन तीन करणों का स्वरूप तो पूर्ववत् ही जानना चाहिये । इतना विशेष है कि यहाँ सातवें गुणस्थान में यथाप्रवृत्तकरण होता है, आठवें अपूर्वकरण नामक गुणस्थान में अपूर्वकरण होता है और नौवें अनिवृत्तिकरण नामक गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण होता है । यहाँ भी स्थितिघात आदि कार्य होते हैं। इतनी विशेषता है कि चौथे से सातवें गुणस्थान तक जो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण होते हैं, उनमें उसी प्रकृति का गुणसंक्रम होता है, जिसके सम्बन्ध में वे परिणाम होते हैं, किन्तु अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थान में समस्त अशुभ- प्रकृतियों का गुणसंक्रम होता है।
अपूर्वकरण के काल में से संख्यातवाँ भाग बीत जाने पर निद्रा और प्रचला (निद्राद्विक) का बन्ध-विच्छेद होता है। उसके पश्चात् और भी काल बीतने पर सुरद्विक, पंचेन्द्रिय जाति इत्यादि तीस प्रकृतियों का बन्ध-विच्छेद होता है। तथा अन्तिम समय में हास्य, रति, भय और जुगुप्सा का बन्ध-विच्छेद होता है । तदनन्तर अनिवृत्तिकरण-गुणस्थान होता है। उसमें भी पूर्ववत् स्थितिघात आदि कार्य होते हैं।
अन्तरकरण के नियम
अनिवृत्तिकरण के काल में से संख्यात भाग व्यतीत हो जाने पर चारित्रमोह की २१ प्रकृतियों का अन्तरकरण करता है। जिन कर्मों का उस समय बन्ध और उदय
१. पंचम कर्मग्रन्थ, गा. ९८ विवेचन, (पं. कैलाशचन्द्र जी जैन), पृ. ३१३ से ३१६ तक २. (क) आवश्यक निर्युक्ति गा. ११६, की टीका के तथा विशेषावश्यक भाष्य गा.
(शेष पृष्ठ ५११ पर)
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org