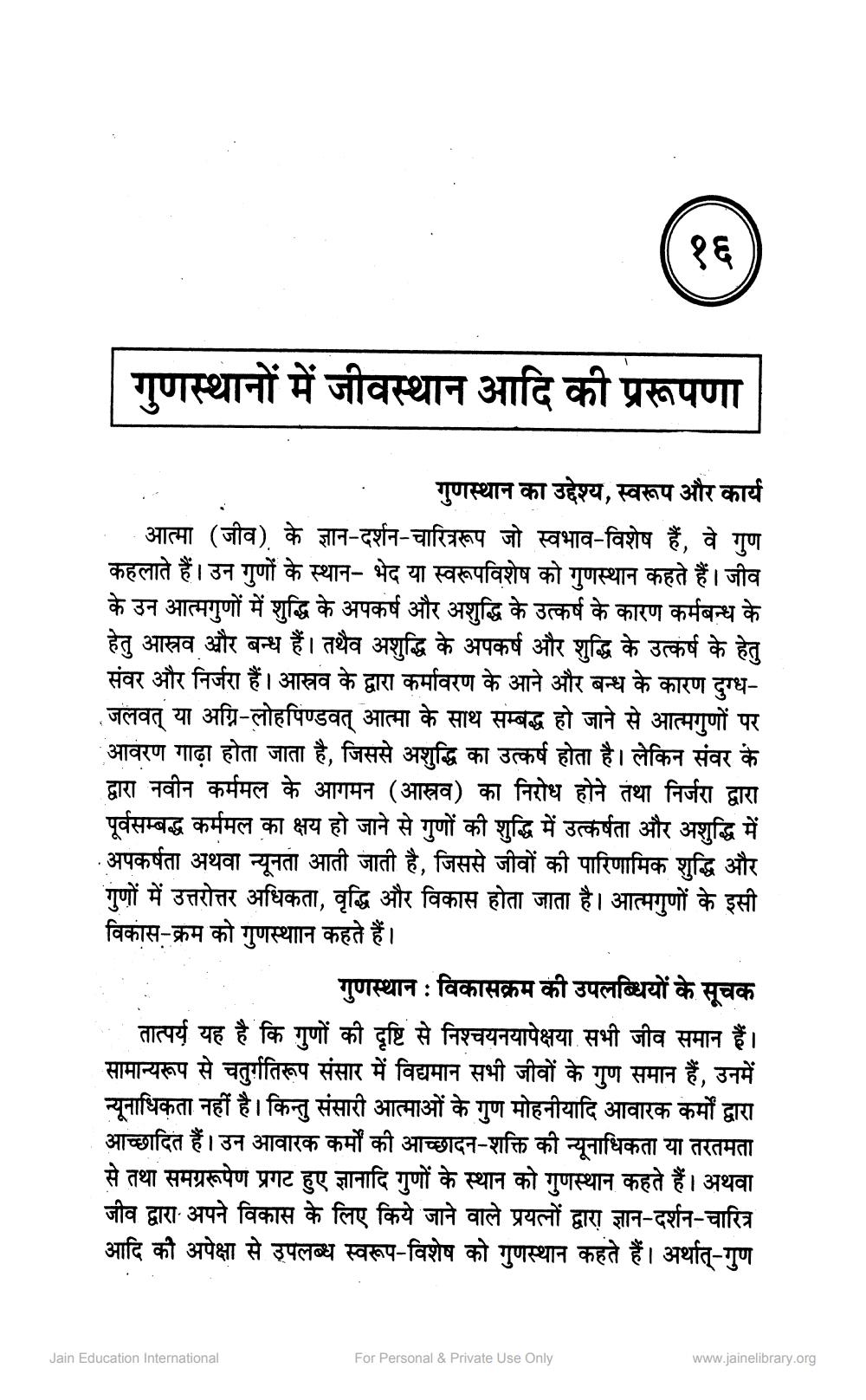________________
गुणस्थानों में जीवस्थान आदि की प्ररूपणा
. गुणस्थान का उद्देश्य, स्वरूप और कार्य आत्मा (जीव) के ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप जो स्वभाव-विशेष हैं, वे गुण कहलाते हैं। उन गुणों के स्थान- भेद या स्वरूपविशेष को गुणस्थान कहते हैं। जीव के उन आत्मगुणों में शुद्धि के अपकर्ष और अशुद्धि के उत्कर्ष के कारण कर्मबन्ध के हेतु आस्रव और बन्ध हैं। तथैव अशुद्धि के अपकर्ष और शुद्धि के उत्कर्ष के हेतु संवर और निर्जरा हैं। आस्रव के द्वारा कर्मावरण के आने और बन्ध के कारण दुग्धजलवत् या अग्नि-लोहपिण्डवत् आत्मा के साथ सम्बद्ध हो जाने से आत्मगुणों पर आवरण गाढ़ा होता जाता है, जिससे अशुद्धि का उत्कर्ष होता है। लेकिन संवर के द्वारा नवीन कर्ममल के आगमन (आस्रव) का निरोध होने तथा निर्जरा द्वारा पूर्वसम्बद्ध कर्ममल का क्षय हो जाने से गुणों की शुद्धि में उत्कर्षता और अशुद्धि में अपकर्षता अथवा न्यूनता आती जाती है, जिससे जीवों की पारिणामिक शद्धि और गुणों में उत्तरोत्तर अधिकता, वृद्धि और विकास होता जाता है। आत्मगुणों के इसी विकास-क्रम को गुणस्थान कहते हैं।
गुणस्थान : विकासक्रम की उपलब्धियों के सूचक तात्पर्य यह है कि गुणों की दृष्टि से निश्चयनयापेक्षया सभी जीव समान हैं। सामान्यरूप से चतुर्गतिरूप संसार में विद्यमान सभी जीवों के गुण समान हैं, उनमें न्यूनाधिकता नहीं है। किन्तु संसारी आत्माओं के गुण मोहनीयादि आवारक कर्मों द्वारा आच्छादित हैं। उन आवारक कर्मों की आच्छादन-शक्ति की न्यूनाधिकता या तरतमता से तथा समग्ररूपेण प्रगट हुए ज्ञानादि गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं। अथवा जीव द्वारा अपने विकास के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों द्वारा ज्ञान-दर्शन-चारित्र आदि की अपेक्षा से उपलब्ध स्वरूप-विशेष को गुणस्थान कहते हैं। अर्थात्-गुण
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org