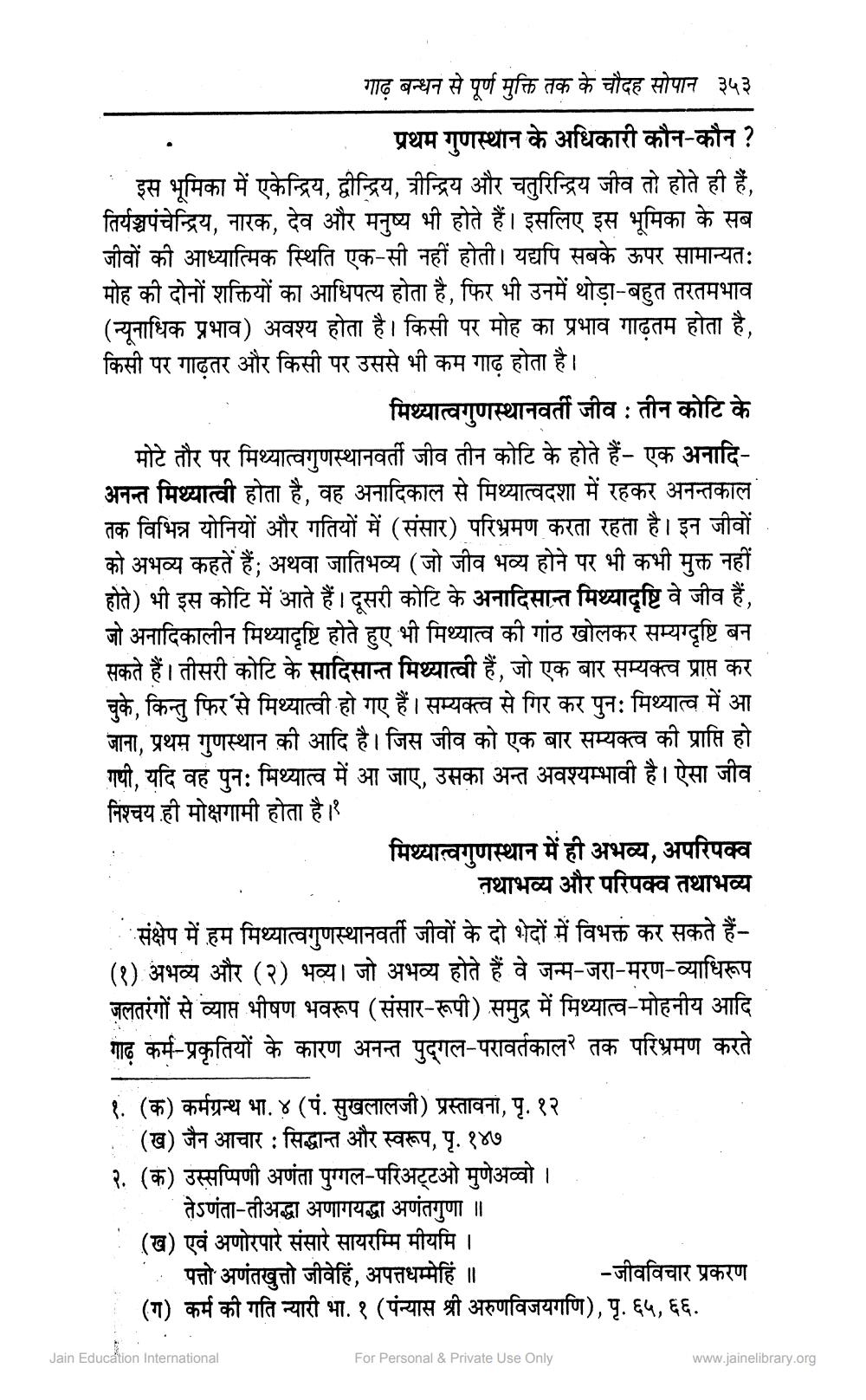________________
गाढ़ बन्धन से पूर्ण मुक्ति तक के चौदह सोपान ३५३
प्रथम गुणस्थान के अधिकारी कौन-कौन ?
इस भूमिका में एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीव तो होते ही हैं, तिर्यञ्चपंचेन्द्रिय, नारक, देव और मनुष्य भी होते हैं । इसलिए इस भूमिका के सब जीवों की आध्यात्मिक स्थिति एक सी नहीं होती । यद्यपि सबके ऊपर सामान्यतः मोह की दोनों शक्तियों का आधिपत्य होता है, फिर भी उनमें थोड़ा-बहुत तरतमभाव (न्यूनाधिक प्रभाव ) अवश्य होता है। किसी पर मोह का प्रभाव गाढ़तम होता है, किसी पर गाढ़तर और किसी पर उससे भी कम गाढ़ होता है ।
मिथ्यात्वगुणस्थानवर्ती जीव तीन कोटि के
:
मोटे तौर पर मिथ्यात्वगुणस्थानवर्ती जीव तीन कोटि के होते हैं - एक अनादिअनन्त मिथ्यात्वी होता है, वह अनादिकाल से मिथ्यात्वदशा में रहकर अनन्तकाल तक विभिन्न योनियों और गतियों में (संसार) परिभ्रमण करता रहता है। इन जीवों को अभव्य कहतें हैं; अथवा जातिभव्य (जो जीव भव्य होने पर भी कभी मुक्त नहीं होते) भी इस कोटि में आते हैं। दूसरी कोटि के अनादिसान्त मिथ्यादृष्टि वे जीव हैं, जो अनादिकालीन मिथ्यादृष्टि होते हुए भी मिथ्यात्व की गांठ खोलकर सम्यग्दृष्टि बन सकते हैं। तीसरी कोटि के सादिसान्त मिथ्यात्वी हैं, जो एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर चुके, किन्तु फिर से मिथ्यात्वी हो गए हैं। सम्यक्त्व से गिर कर पुनः मिथ्यात्व में आ जाना, प्रथम गुणस्थान की आदि है। जिस जीव को एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गधी, यदि वह पुन: मिथ्यात्व में आ जाए, उसका अन्त अवश्यम्भावी है। ऐसा जीव निश्चय ही मोक्षगामी होता है । १
मिथ्यात्वगुणस्थान में ही अभव्य, अपरिपक्व तथाभव्य और परिपक्व तथाभव्य
संक्षेप में हम मिथ्यात्वगुणस्थानवर्ती जीवों के दो भेदों में विभक्त कर सकते हैं(१) अभव्य और (२) भव्य । जो अभव्य होते हैं वे जन्म- जरा - मरण-व्याधिरूप जलतरंगों से व्याप्त भीषण भवरूप (संसार रूपी) समुद्र में मिथ्यात्व - मोहनीय आदि गाढ़ कर्म- प्रकृतियों के कारण अनन्त पुद्गल - परावर्तकाल तक परिभ्रमण करते
१. (क) कर्मग्रन्थ भा. ४ (पं. सुखलालजी) प्रस्तावना, पृ. १२
(ख) जैन आचार : सिद्धान्त और स्वरूप, पृ. १४७ (क) उस्सप्पिणी अणंता पुग्गल - परिअट्टओ मुणेअव्वो । तेऽणंता-तीअद्धा अणागयद्धा अणंतगुणा ॥
(ख) एवं अणोरपारे संसारे सायरम्मि मीयमि ।
Jain Education International
पत्तो अनंतखुत्तो जीवेहिं, अपत्तधम्मेहिं ॥
- जीवविचार प्रकरण
(ग) कर्म की गति न्यारी भा. १ ( पंन्यास श्री अरुणविजयगणि), पृ. ६५, ६६.
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org