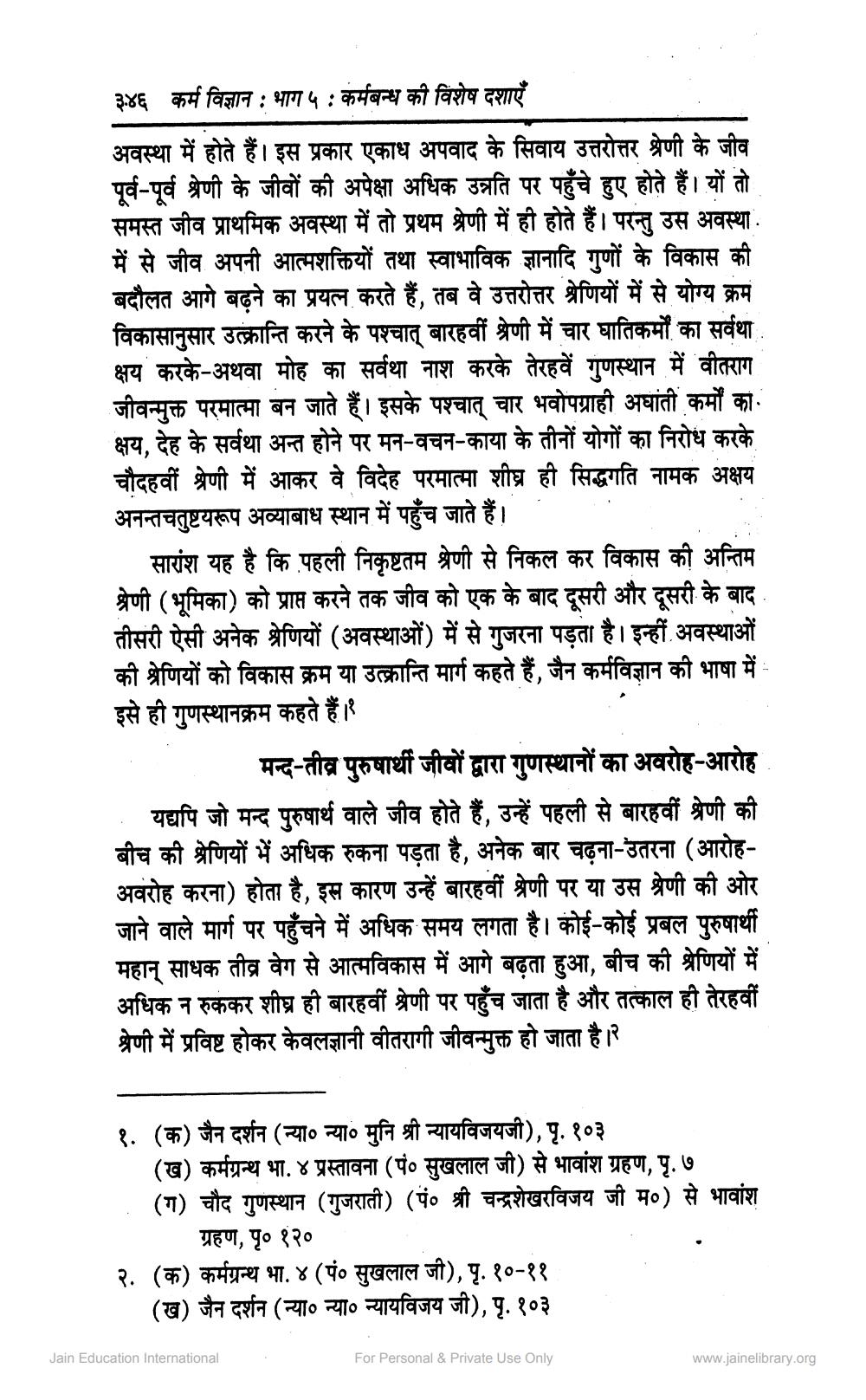________________
३-४६ कर्म विज्ञान : भाग ५ : कर्मबन्ध की विशेष दशाएँ
अवस्था में होते हैं। इस प्रकार एकाध अपवाद के सिवाय उत्तरोत्तर श्रेणी के जीव पूर्व - पूर्व श्रेणी के जीवों की अपेक्षा अधिक उन्नति पर पहुँचे हुए होते हैं। यों तो समस्त जीव प्राथमिक अवस्था में तो प्रथम श्रेणी में ही होते हैं। परन्तु उस अवस्था. में से जीव अपनी आत्मशक्तियों तथा स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों के विकास की बदौलत आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, तब वे उत्तरोत्तर श्रेणियों में से योग्य क्रम विकासानुसार उत्क्रान्ति करने के पश्चात् बारहवीं श्रेणी में चार घातिकर्मों का सर्वथा क्षय करके अथवा मोह का सर्वथा नाश करके तेरहवें गुणस्थान में वीतराग जीवन्मुक्त परमात्मा बन जाते हैं। इसके पश्चात् चार भवोपग्राही अघाती कर्मों का. क्षय, देह के सर्वथा अन्त होने पर मन-वचन-काया के तीनों योगों का निरोध करके चौदहवीं श्रेणी में आकर वे विदेह परमात्मा शीघ्र ही सिद्धगति नामक अक्षय अनन्तचतुष्टयरूप अव्याबाध स्थान में पहुँच जाते हैं।
सारांश यह है कि पहली निकृष्टतम श्रेणी से निकल कर विकास की अन्तिम श्रेणी (भूमिका) को प्राप्त करने तक जीव को एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी ऐसी अनेक श्रेणियों (अवस्थाओं) में से गुजरना पड़ता है। इन्हीं अवस्थाओं की श्रेणियों को विकासक्रम या उत्क्रान्ति मार्ग कहते हैं, जैन कर्मविज्ञान की भाषा में इसे ही गुणस्थानक्रम कहते हैं । १
मन्द-तीव्र पुरुषार्थी जीवों द्वारा गुणस्थानों का अवरोह-आरोह
यद्यपि जो मन्द पुरुषार्थ वाले जीव होते हैं, उन्हें पहली से बारहवीं श्रेणी की बीच की श्रेणियों में अधिक रुकना पड़ता है, अनेक बार चढ़ना-उतरना (आरोहअवरोह करना) होता है, इस कारण उन्हें बारहवीं श्रेणी पर या उस श्रेणी की ओर जाने वाले मार्ग पर पहुँचने में अधिक समय लगता है । कोई-कोई प्रबल पुरुषार्थी महान् साधक तीव्र वेग से आत्मविकास में आगे बढ़ता हुआ, बीच की श्रेणियों में अधिक न रुककर शीघ्र ही बारहवीं श्रेणी पर पहुँच जाता है और तत्काल ही तेरहवीं श्रेणी में प्रविष्ट होकर केवलज्ञानी वीतरागी जीवन्मुक्त हो जाता है। २
१. (क) जैन दर्शन (न्या० न्या० मुनि श्री न्यायविजयजी), पृ. १०३
(ख) कर्मग्रन्थ भा. ४ प्रस्तावना (पं० सुखलाल जी) से भावांश ग्रहण, पृ. ७ (ग) चौद गुणस्थान (गुजराती) ( पं० श्री चन्द्रशेखरविजय जी म० ) से भावांश
ग्रहण, पृ० १२०
२. (क) कर्मग्रन्थ भा. ४ ( पं० सुखलाल जी), पृ. १०-११
(ख) जैन दर्शन (न्या० न्या० न्यायविजय जी ), पृ. १०३
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org