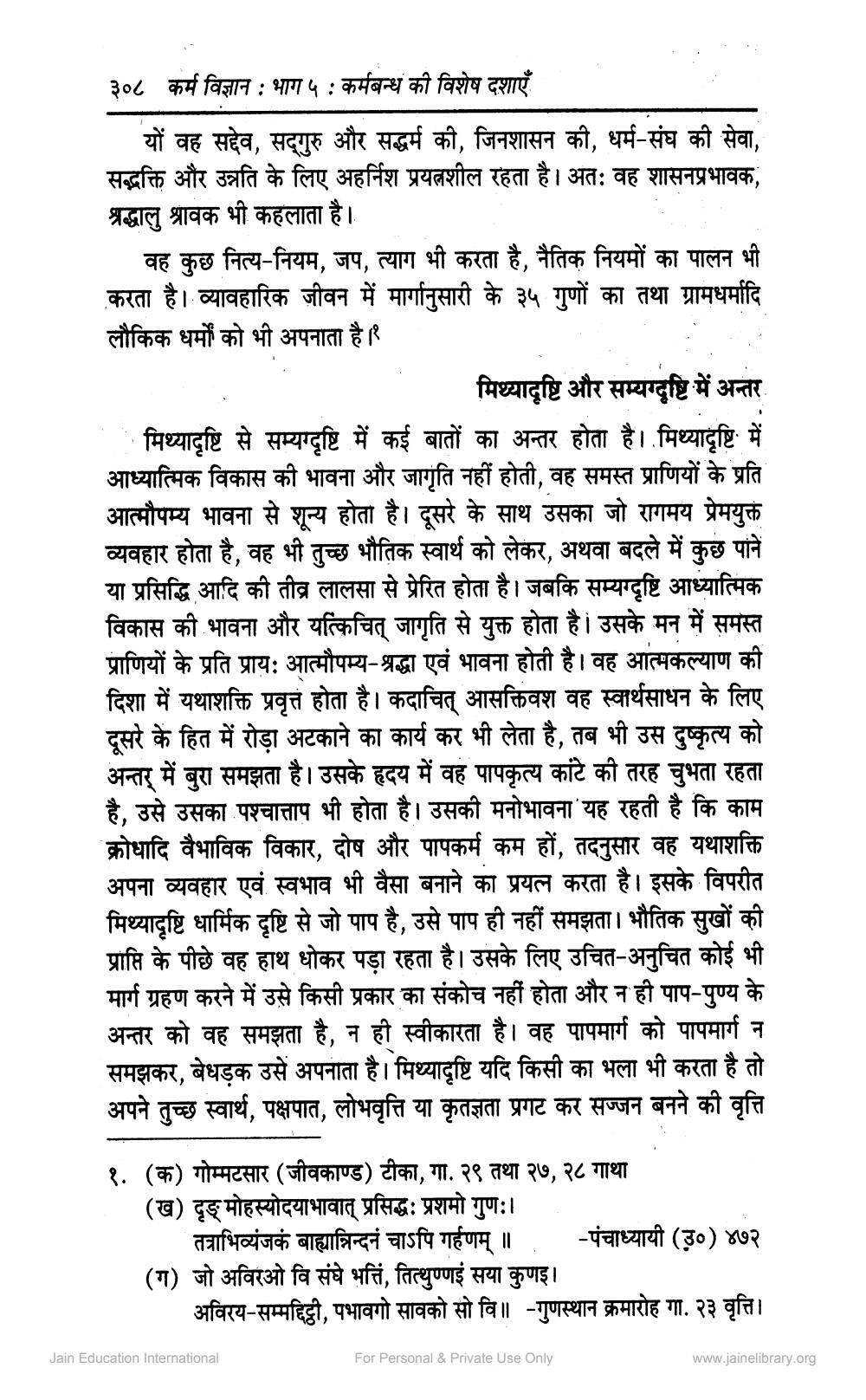________________
३०८ कर्म विज्ञान : भाग ५ : कर्मबन्ध की विशेष दशाएँ
___यों वह सद्देव, सद्गुरु और सद्धर्म की, जिनशासन की, धर्म-संघ की सेवा, सद्भक्ति और उन्नति के लिए अहर्निश प्रयत्नशील रहता है। अतः वह शासनप्रभावक, श्रद्धालु श्रावक भी कहलाता है।
वह कुछ नित्य-नियम, जप, त्याग भी करता है, नैतिक नियमों का पालन भी करता है। व्यावहारिक जीवन में मार्गानुसारी के ३५ गुणों का तथा ग्रामधर्मादि लौकिक धर्मों को भी अपनाता है।
- मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि में अन्तर मिथ्यादृष्टि से सम्यग्दृष्टि में कई बातों का अन्तर होता है। मिथ्यादृष्टि में आध्यात्मिक विकास की भावना और जागृति नहीं होती, वह समस्त प्राणियों के प्रति आत्मौपम्य भावना से शून्य होता है। दूसरे के साथ उसका जो रागमय प्रेमयुक्त व्यवहार होता है, वह भी तुच्छ भौतिक स्वार्थ को लेकर, अथवा बदले में कुछ पाने या प्रसिद्धि आदि की तीव्र लालसा से प्रेरित होता है। जबकि सम्यग्दृष्टि आध्यात्मिक विकास की भावना और यत्किचित् जागृति से युक्त होता है। उसके मन में समस्त प्राणियों के प्रति प्रायः आत्मौपम्य-श्रद्धा एवं भावना होती है। वह आत्मकल्याण की दिशा में यथाशक्ति प्रवृत्त होता है। कदाचित् आसक्तिवश वह स्वार्थसाधन के लिए दूसरे के हित में रोड़ा अटकाने का कार्य कर भी लेता है, तब भी उस दुष्कृत्य को अन्तर् में बुरा समझता है। उसके हृदय में वह पापकृत्य कांटे की तरह चुभता रहता है, उसे उसका पश्चात्ताप भी होता है। उसकी मनोभावना यह रहती है कि काम क्रोधादि वैभाविक विकार, दोष और पापकर्म कम हों, तदनुसार वह यथाशक्ति अपना व्यवहार एवं स्वभाव भी वैसा बनाने का प्रयत्न करता है। इसके विपरीत मिथ्यादृष्टि धार्मिक दृष्टि से जो पाप है, उसे पाप ही नहीं समझता। भौतिक सुखों की प्राप्ति के पीछे वह हाथ धोकर पड़ा रहता है। उसके लिए उचित-अनुचित कोई भी मार्ग ग्रहण करने में उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं होता और न ही पाप-पुण्य के अन्तर को वह समझता है, न ही स्वीकारता है। वह पापमार्ग को पापमार्ग न समझकर, बेधड़क उसे अपनाता है। मिथ्यादृष्टि यदि किसी का भला भी करता है तो अपने तुच्छ स्वार्थ, पक्षपात, लोभवृत्ति या कृतज्ञता प्रगट कर सज्जन बनने की वृत्ति
१. (क) गोम्मटसार (जीवकाण्ड) टीका, गा. २९ तथा २७, २८ गाथा (ख) दृङ्मोहस्योदयाभावात् प्रसिद्धः प्रशमो गुणः।।
तत्राभिव्यंजकं बाह्यान्निन्दनं चाऽपि गर्हणम् ॥ . -पंचाध्यायी (उ०) ४७२ (ग) जो अविरओ वि संघे भत्तिं, तित्थुण्णइं सया कुणइ।
अविरय-सम्मद्दिट्ठी, पभावगो सावको सो वि॥ -गुणस्थान क्रमारोह गा. २३ वृत्ति।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org