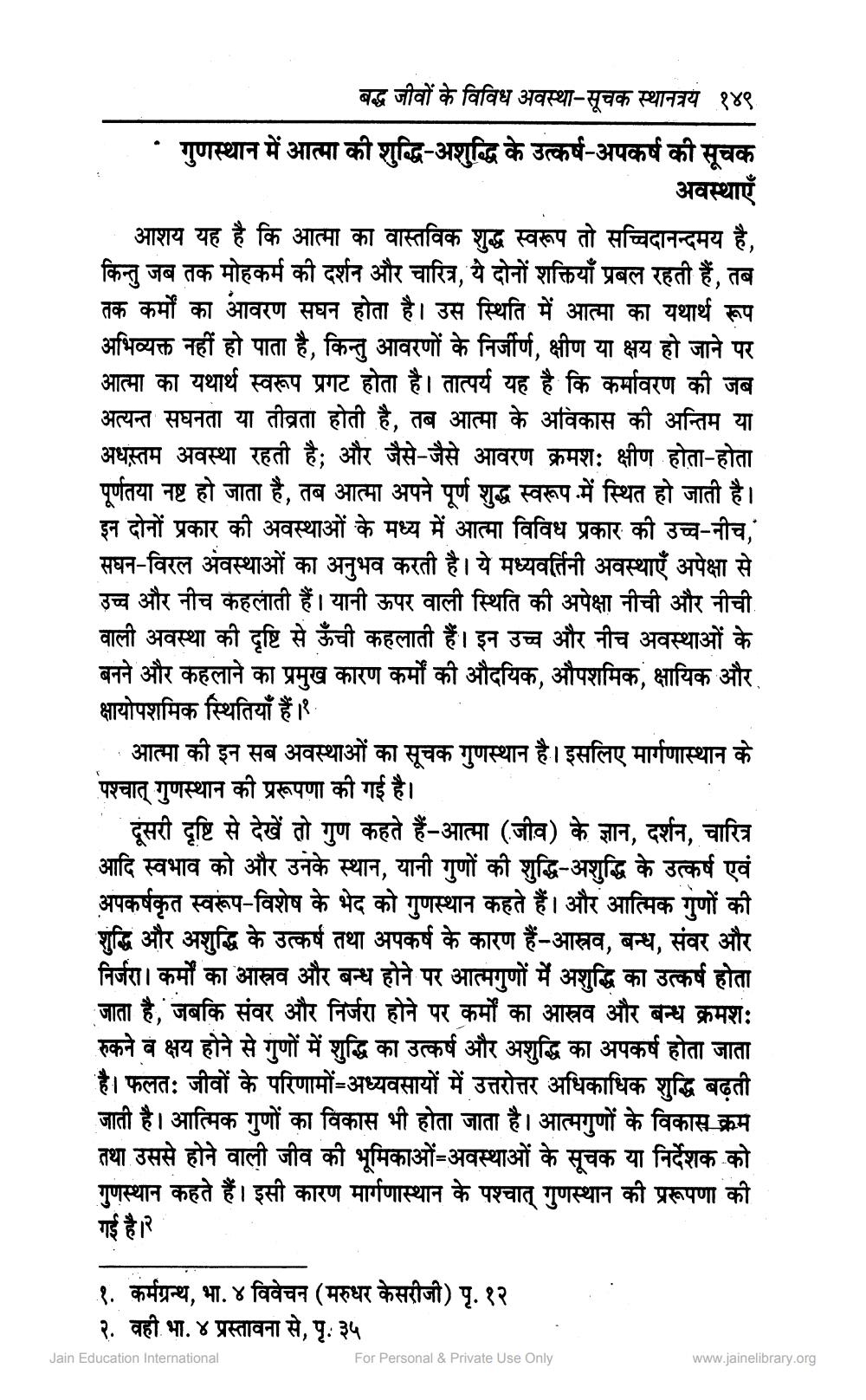________________
बद्ध जीवों के विविध अवस्था - सूचक स्थानत्रय १४९ गुणस्थान में आत्मा की शुद्धि - अशुद्धि के उत्कर्ष - अपकर्ष की सूचक अवस्थाएँ
आशय यह है कि आत्मा का वास्तविक शुद्ध स्वरूप तो सच्चिदानन्दमय है, किन्तु जब तक मोहकर्म की दर्शन और चारित्र, ये दोनों शक्तियाँ प्रबल रहती हैं, तब तक कर्मों का आवरण सघन होता है। उस स्थिति में आत्मा का यथार्थ रूप अभिव्यक्त नहीं हो पाता है, किन्तु आवरणों के निर्जीर्ण, क्षीण या क्षय हो जाने पर आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रगट होता है। तात्पर्य यह है कि कर्मावरण की जब अत्यन्त सघनता या तीव्रता होती है, तब आत्मा के अविकास की अन्तिम या अधस्तम अवस्था रहती है; और जैसे-जैसे आवरण क्रमशः क्षीण होता-होता पूर्णतया नष्ट हो जाता है, तब आत्मा अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है। इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं के मध्य में आत्मा विविध प्रकार की उच्च-नीच, सघन-विरल अवस्थाओं का अनुभव करती है। ये मध्यवर्तिनी अवस्थाएँ अपेक्षा से उच्च और नीच कहलाती हैं। यानी ऊपर वाली स्थिति की अपेक्षा नीची और नीची. वाली अवस्था की दृष्टि से ऊँची कहलाती हैं। इन उच्च और नीच अवस्थाओं के बनने और कहलाने का प्रमुख कारण कर्मों की औदयिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक स्थितियाँ हैं ।
आत्मा की इन सब अवस्थाओं का सूचक गुणस्थान है। इसलिए मार्गणास्थान के पश्चात् गुणस्थान की प्ररूपणा की गई है।
दूसरी दृष्टि से देखें तो गुण कहते हैं- आत्मा (जीव ) के ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि स्वभाव को और उनके स्थान, यानी गुणों की शुद्धि - अशुद्धि के उत्कर्ष एवं अपकर्षकृत स्वरूप - विशेष के भेद को गुणस्थान कहते हैं। और आत्मिक गुणों की शुद्धि और अशुद्धि के उत्कर्ष तथा अपकर्ष के कारण हैं- आस्रव, बन्ध, संवर और निर्जरा । कर्मों का आस्रव और बन्ध होने पर आत्मगुणों में अशुद्धि का उत्कर्ष होता जाता है, जबकि संवर और निर्जरा होने पर कर्मों का आस्रव और बन्ध क्रमशः रुकने व क्षय होने से गुणों में शुद्धि का उत्कर्ष और अशुद्धि का अपकर्ष होता जाता है। फलतः जीवों के परिणामों - अध्यवसायों में उत्तरोत्तर अधिकाधिक शुद्धि बढ़ती जाती है। आत्मिक गुणों का विकास भी होता जाता है। आत्मगुणों के विकास क्रम तथा उससे होने वाली जीव की भूमिकाओं = अवस्थाओं के सूचक या निर्देशक को गुणस्थान कहते हैं । इसी कारण मार्गणास्थान के पश्चात् गुणस्थान की प्ररूपणा की गई है। २
१. कर्मग्रन्थ, भा. ४ विवेचन ( मरुधर केसरीजी) पृ. १२
२. वही भा. ४ प्रस्तावना से, पृ: ३५
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org