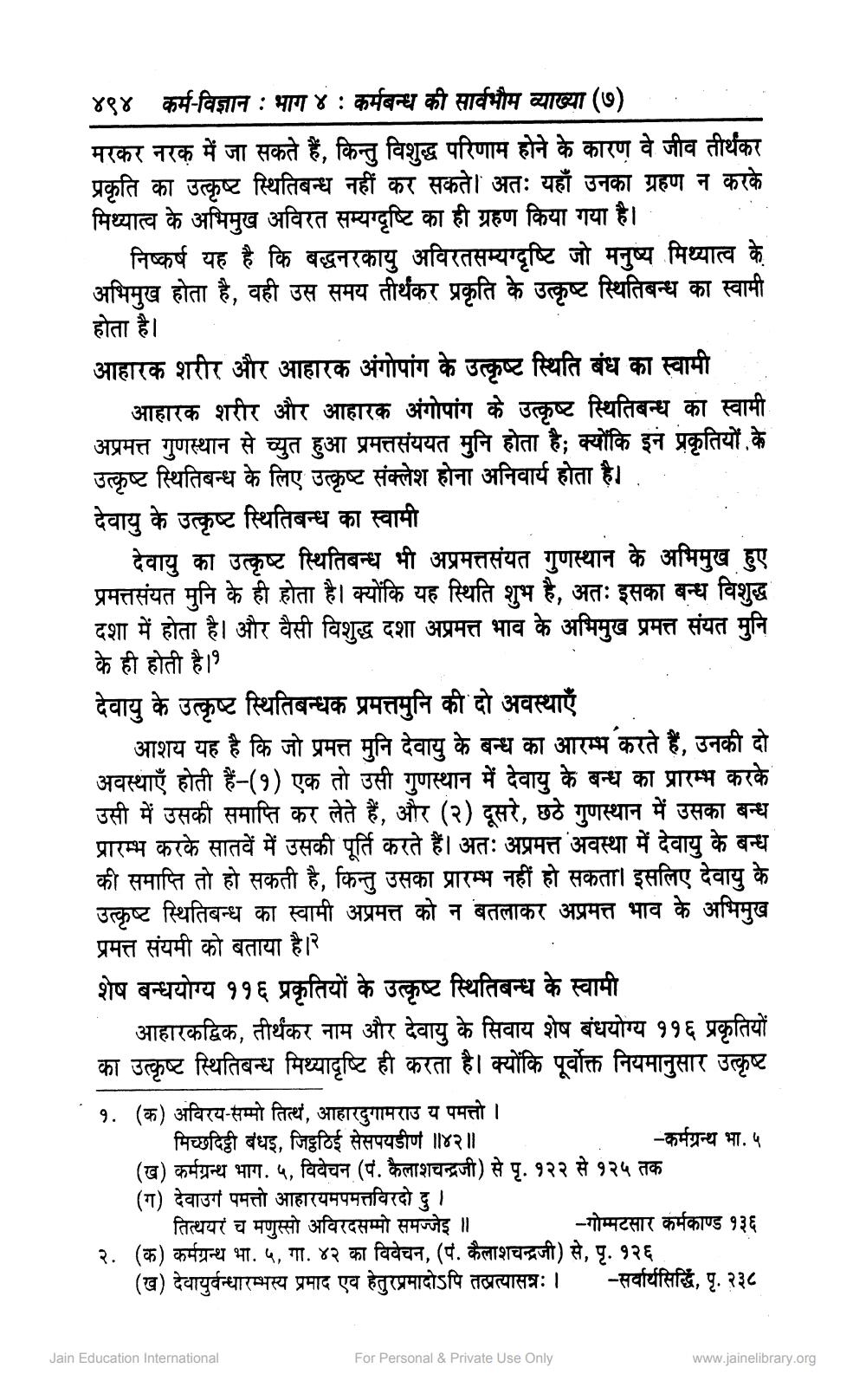________________
४९४ कर्म-विज्ञान : भाग ४ : कर्मबन्ध की सार्वभौम व्याख्या (७) मरकर नरक में जा सकते हैं, किन्तु विशुद्ध परिणाम होने के कारण वे जीव तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं कर सकते। अतः यहाँ उनका ग्रहण न करके मिथ्यात्व के अभिमुख अविरत सम्यग्दृष्टि का ही ग्रहण किया गया है।
निष्कर्ष यह है कि बद्धनरकायु अविरतसम्यग्दृष्टि जो मनुष्य मिथ्यात्व के अभिमुख होता है, वही उस समय तीर्थंकर प्रकृति के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का स्वामी होता है। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग के उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी __ आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का स्वामी अप्रमत्त गुणस्थान से च्युत हुआ प्रमत्तसंययत मुनि होता है; क्योंकि इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध के लिए उत्कृष्ट संक्लेश होना अनिवार्य होता है। . देवायु के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का स्वामी
देवायु का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध भी अप्रमत्तसंयत गुणस्थान के अभिमुख हुए प्रमत्तसंयत मुनि के ही होता है। क्योंकि यह स्थिति शुभ है, अतः इसका बन्ध विशुद्ध दशा में होता है। और वैसी विशुद्ध दशा अप्रमत्त भाव के अभिमुख प्रमत्त संयत मुनि के ही होती है। देवायु के उत्कृष्ट स्थितिबन्धक प्रमत्तमुनि की दो अवस्थाएँ .
आशय यह है कि जो प्रमत्त मुनि देवायु के बन्ध का आरम्भ करते हैं, उनकी दो अवस्थाएँ होती हैं-(१) एक तो उसी गुणस्थान में देवायु के बन्ध का प्रारम्भ करके उसी में उसकी समाप्ति कर लेते हैं, और (२) दूसरे, छठे गुणस्थान में उसका बन्ध प्रारम्भ करके सातवें में उसकी पूर्ति करते हैं। अतः अप्रमत्त अवस्था में देवायु के बन्ध की समाप्ति तो हो सकती है, किन्तु उसका प्रारम्भ नहीं हो सकता। इसलिए देवायु के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का स्वामी अप्रमत्त को न बतलाकर अप्रमत्त भाव के अभिमुख प्रमत्त संयमी को बताया है।२ शेष बन्धयोग्य ११६ प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध के स्वामी __ आहारकद्विक, तीर्थंकर नाम और देवायु के सिवाय शेष बंधयोग्य ११६ प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यादृष्टि ही करता है। क्योंकि पूर्वोक्त नियमानुसार उत्कृष्ट १. (क) अविरय-सम्मो तित्थं, आहारदुगामराउ य पमत्तो । मिच्छदिट्ठी बंधइ, जिट्ठठिई सेसपयडीणं ॥४२॥
-कर्मग्रन्थ भा.५ (ख) कर्मग्रन्थ भाग. ५, विवेचन (प. कैलाशचन्द्रजी) से पृ. १२२ से १२५ तक (ग) देवाउगं पमत्तो आहारयमपमत्तविरदो दु।।
तित्थयरं च मणुस्सो अविरदसम्मो समज्जेइ ॥ -गोम्मटसार कर्मकाण्ड १३६ २. (क) कर्मग्रन्थ भा. ५, गा. ४२ का विवेचन, (पं. कैलाशचन्द्रजी) से, पृ. १२६ ।
(ख) देवायुर्वन्धारम्भस्य प्रमाद एव हेतुरप्रमादोऽपि तत्प्रत्यासन्नः। -सर्वार्थसिद्धिं, पृ. २३८
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org