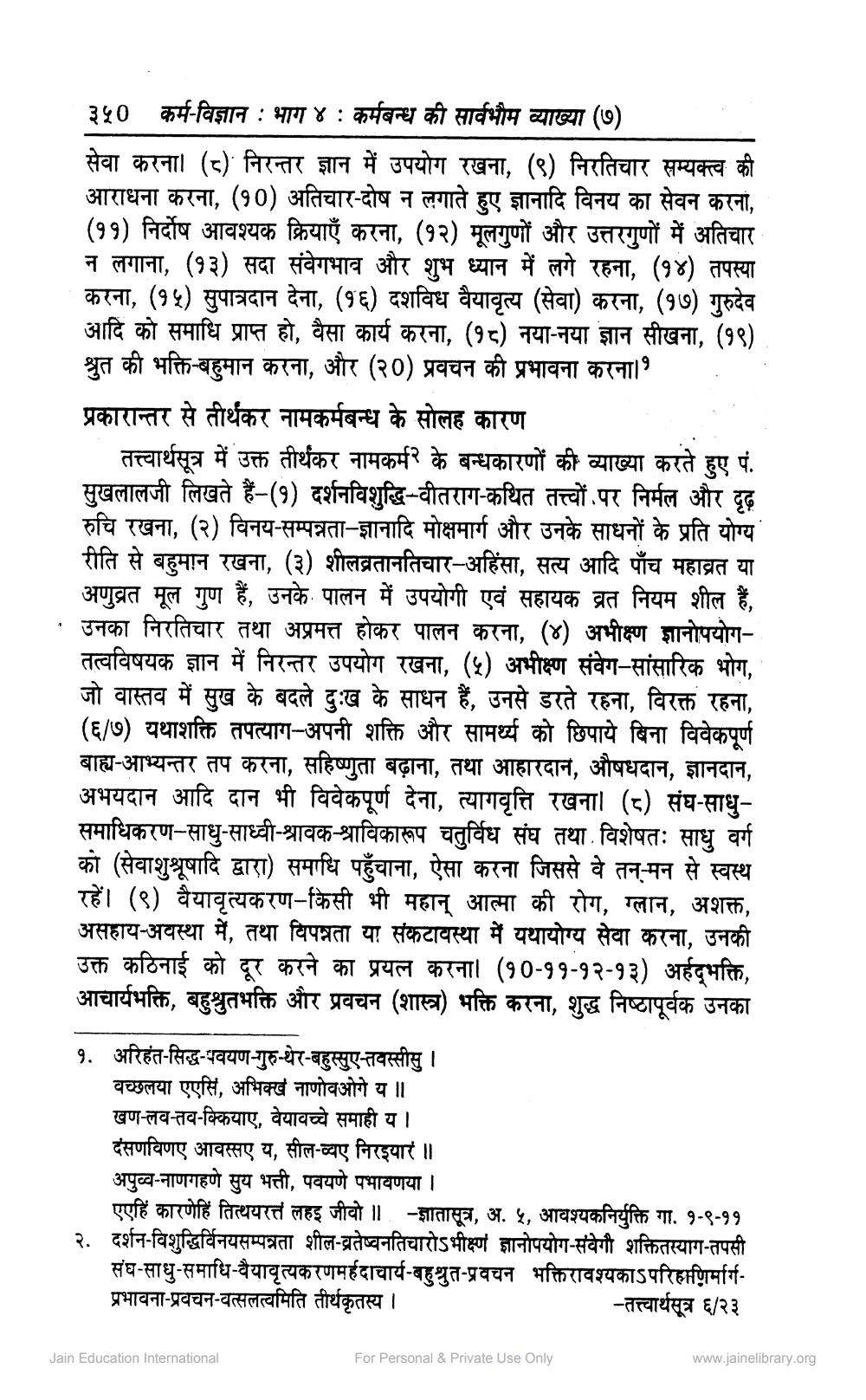________________
३५0 कर्म-विज्ञान : भाग ४ : कर्मबन्ध की सार्वभौम व्याख्या (७) सेवा करना। (८) निरन्तर ज्ञान में उपयोग रखना, (९) निरतिचार सम्यक्त्व की आराधना करना, (१०) अतिचार-दोष न लगाते हुए ज्ञानादि विनय का सेवन करना, (११) निर्दोष आवश्यक क्रियाएँ करना, (१२) मूलगुणों और उत्तरगुणों में अतिचार न लगाना, (१३) सदा संवेगभाव और शुभ ध्यान में लगे रहना, (१४) तपस्या करना, (१५) सुपात्रदान देना, (१६) दशविध वैयावृत्य (सेवा) करना, (१७) गुरुदेव आदि को समाधि प्राप्त हो, वैसा कार्य करना, (१८) नया-नया ज्ञान सीखना, (१९) श्रुत की भक्ति-बहुमान करना, और (२०) प्रवचन की प्रभावना करना। प्रकारान्तर से तीर्थंकर नामकर्मबन्ध के सोलह कारण
तत्त्वार्थसूत्र में उक्त तीर्थंकर नामकर्मर के बन्धकारणों की व्याख्या करते हुए पं. सुखलालजी लिखते हैं-(१) दर्शनविशुद्धि-वीतराग-कथित तत्त्वों पर निर्मल और दृढ़ रुचि रखना, (२) विनय-सम्पन्नता-ज्ञानादि मोक्षमार्ग और उनके साधनों के प्रति योग्य रीति से बहुमान रखना, (३) शीलव्रतानतिचार-अहिंसा, सत्य आदि पाँच महाव्रत या अणुव्रत मूल गुण हैं, उनके पालन में उपयोगी एवं सहायक व्रत नियम शील हैं, उनका निरतिचार तथा अप्रमत्त होकर पालन करना, (४) अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगतत्वविषयक ज्ञान में निरन्तर उपयोग रखना, (५) अभीक्ष्ण संवेग-सांसारिक भोग. जो वास्तव में सुख के बदले दुःख के साधन हैं, उनसे डरते रहना, विरक्त रहना, (६/७) यथाशक्ति तपत्याग-अपनी शक्ति और सामर्थ्य को छिपाये बिना विवेकपूर्ण बाह्य-आभ्यन्तर तप करना, सहिष्णुता बढ़ाना, तथा आहारदान, औषधदान, ज्ञानदान, अभयदान आदि दान भी विवेकपूर्ण देना, त्यागवृत्ति रखना। (८) संघ-साधुसमाधिकरण-साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध संघ तथा विशेषतः साधु वर्ग को (सेवाशुश्रूषादि द्वारा) समाधि पहुँचाना, ऐसा करना जिससे वे तन-मन से स्वस्थ रहें। (९) वैयावृत्यकरण-किसी भी महान् आत्मा की रोग, ग्लान, अशक्त, असहाय-अवस्था में, तथा विपन्नता या संकटावस्था में यथायोग्य सेवा करना, उनकी उक्त कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करना। (१०-११-१२-१३) अर्हद्भक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति और प्रवचन (शास्त्र) भक्ति करना, शुद्ध निष्ठापूर्वक उनका
१. अरिहंत-सिद्ध-पवयण-गुरु-थेर-बहुस्सुए-तवस्सीसु ।
वच्छलया एएसि, अभिक्ख नाणोवओगे य । खण-लव-तव-क्कियाए, वेयावच्चे समाही य । दसणविणए आवस्सए य, सील-व्यए निरइयार ॥ अपुव्व-नाणगहणे सुय भत्ती, पवयणे पभायणया ।
एएहिं कारणेहिं तित्थयरत्त लहइ जीवो ॥ -ज्ञातासूत्र, अ. ५, आवश्यकनियुक्ति गा. १-९-११ २. दर्शन-विशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शील-व्रतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णं ज्ञानोपयोग-संवेगी शक्तितस्याग-तपसी
संघ-साधु-समाधि-वैयावृत्यकरणमर्हदाचार्य-बहुश्रुत-प्रवचन भक्तिरावश्यकाऽपरिहाणिर्गिप्रभावना-प्रवचन-वत्सलत्वमिति तीर्थकृतस्य ।
-तत्त्वार्थसूत्र ६/२३
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org