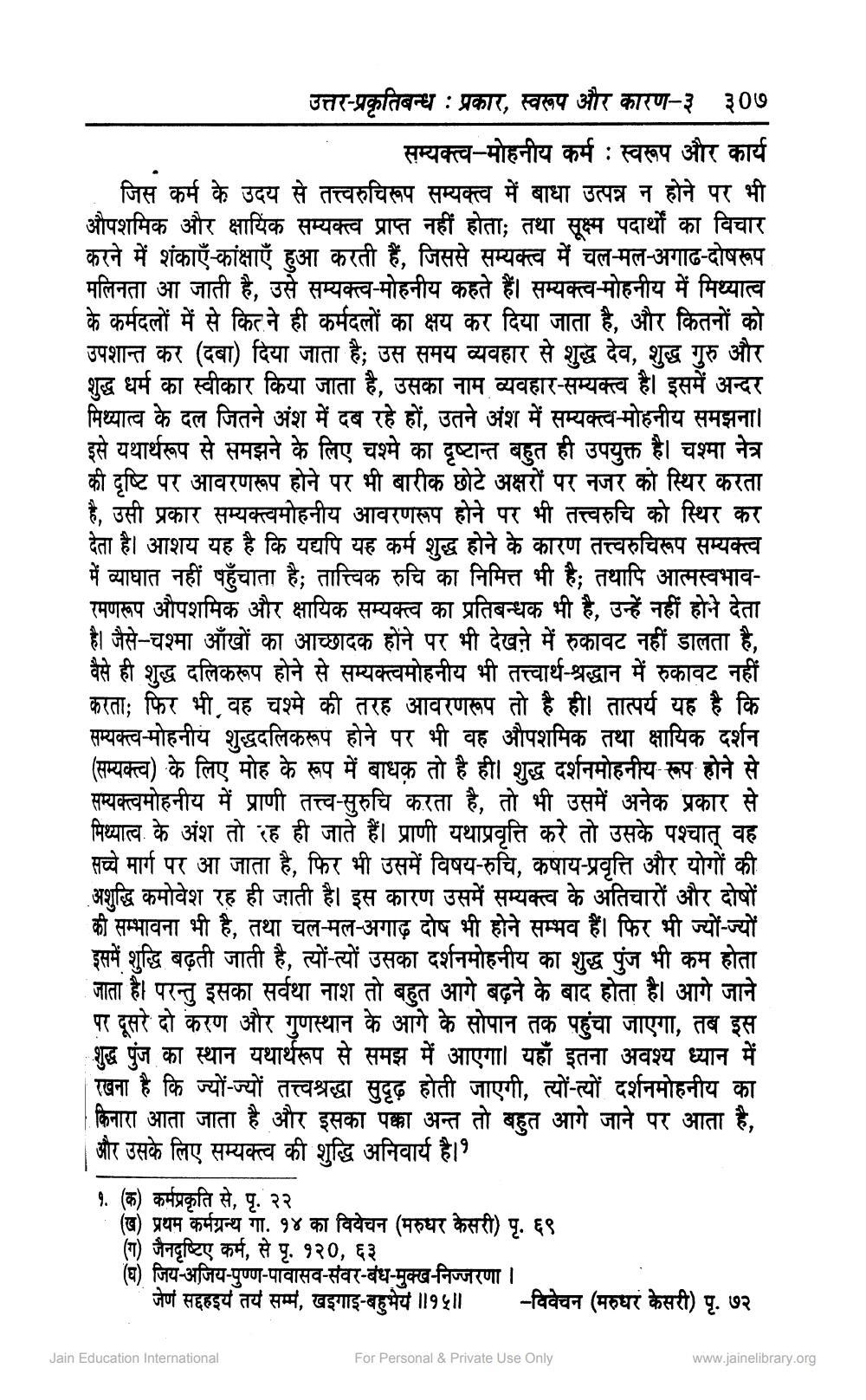________________
उत्तर-प्रकृतिबन्ध : प्रकार, स्वरूप और कारण-३ ३०७
सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म : स्वरूप और कार्य जिस कर्म के उदय से तत्त्वरुचिरूप सम्यक्त्व में बाधा उत्पन्न न होने पर भी औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता; तथा सूक्ष्म पदार्थों का विचार करने में शंकाएँ-कांक्षाएँ हुआ करती हैं, जिससे सम्यक्त्व में चल-मल-अगाढ-दोषरूप मलिनता आ जाती है, उसे सम्यक्त्व-मोहनीय कहते हैं। सम्यक्त्व-मोहनीय में मिथ्यात्व के कर्मदलों में से कितने ही कर्मदलों का क्षय कर दिया जाता है, और कितनों को उपशान्त कर (दबा) दिया जाता है; उस समय व्यवहार से शुद्ध देव, शुद्ध गुरु और शुद्ध धर्म का स्वीकार किया जाता है, उसका नाम व्यवहार-सम्यक्त्व है। इसमें अन्दर मिथ्यात्व के दल जितने अंश में दब रहे हों, उतने अंश में सम्यक्त्व मोहनीय समझना। इसे यथार्थरूप से समझने के लिए चश्मे का दृष्टान्त बहुत ही उपयुक्त है। चश्मा नेत्र की दृष्टि पर आवरणरूप होने पर भी बारीक छोटे अक्षरों पर नजर को स्थिर करता है, उसी प्रकार सम्यक्त्वमोहनीय आवरणरूप होने पर भी तत्त्वरुचि को स्थिर कर देता है। आशय यह है कि यद्यपि यह कर्म शुद्ध होने के कारण तत्त्वरुचिरूप सम्यक्त्व में व्याघात नहीं पहुँचाता है; तात्त्विक रुचि का निमित्त भी है; तथापि आत्मस्वभावरमणरूप औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व का प्रतिबन्धक भी है, उन्हें नहीं होने देता है। जैसे-चश्मा आँखों का आच्छादक होने पर भी देखने में रुकावट नहीं डालता है, वैसे ही शुद्ध दलिकरूप होने से सम्यक्त्वमोहनीय भी तत्त्वार्थ-श्रद्धान में रुकावट नहीं करता; फिर भी, वह चश्मे की तरह आवरणरूप तो है ही। तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्व-मोहनीय शुद्धदलिकरूप होने पर भी वह औपशमिक तथा क्षायिक दर्शन (सम्यक्त्व) के लिए मोह के रूप में बाधक तो है ही। शुद्ध दर्शनमोहनीय रूप होने से सम्यक्त्वमोहनीय में प्राणी तत्त्व-सुरुचि करता है, तो भी उसमें अनेक प्रकार से मिथ्यात्व के अंश तो रह ही जाते हैं। प्राणी यथाप्रवृत्ति करे तो उसके पश्चात् वह सच्चे मार्ग पर आ जाता है, फिर भी उसमें विषय-रुचि, कषाय-प्रवृत्ति और योगों की अशुद्धि कमोवेश रह ही जाती है। इस कारण उसमें सम्यक्त्व के अतिचारों और दोषों की सम्भावना भी है, तथा चल-मल-अगाढ़ दोष भी होने सम्भव हैं। फिर भी ज्यों-ज्यों इसमें शुद्धि बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों उसका दर्शनमोहनीय का शुद्ध पुंज भी कम होता जाता है। परन्तु इसका सर्वथा नाश तो बहुत आगे बढ़ने के बाद होता है। आगे जाने पर दूसरे दो करण और गुणस्थान के आगे के सोपान तक पहुंचा जाएगा, तब इस शुद्ध पुंज का स्थान यथार्थरूप से समझ में आएगा। यहाँ इतना अवश्य ध्यान में रखना है कि ज्यों-ज्यों तत्त्वश्रद्धा सुदृढ़ होती जाएगी, त्यों-त्यों दर्शनमोहनीय का किनारा आता जाता है और इसका पक्का अन्त तो बहुत आगे जाने पर आता है, | और उसके लिए सम्यक्त्व की शुद्धि अनिवार्य है। १. (क) कर्मप्रकृति से, पृ. २२ (ख) प्रथम कर्मग्रन्थ गा. १४ का विवेचन (मरुधर केसरी) पृ. ६९ (ग) जैनदृष्टिए कर्म, से पृ. १२०, ६३ (घ) जिय-अजिय-पुण्ण-पावासव-संवर-बंध-मुक्ख-निज्जरणा ।
जेणं सद्दहइयं तय सम्म, खइगाइ-बहुभेयं ॥१५॥ -विवेचन (मरुधर केसरी) पृ. ७२
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org