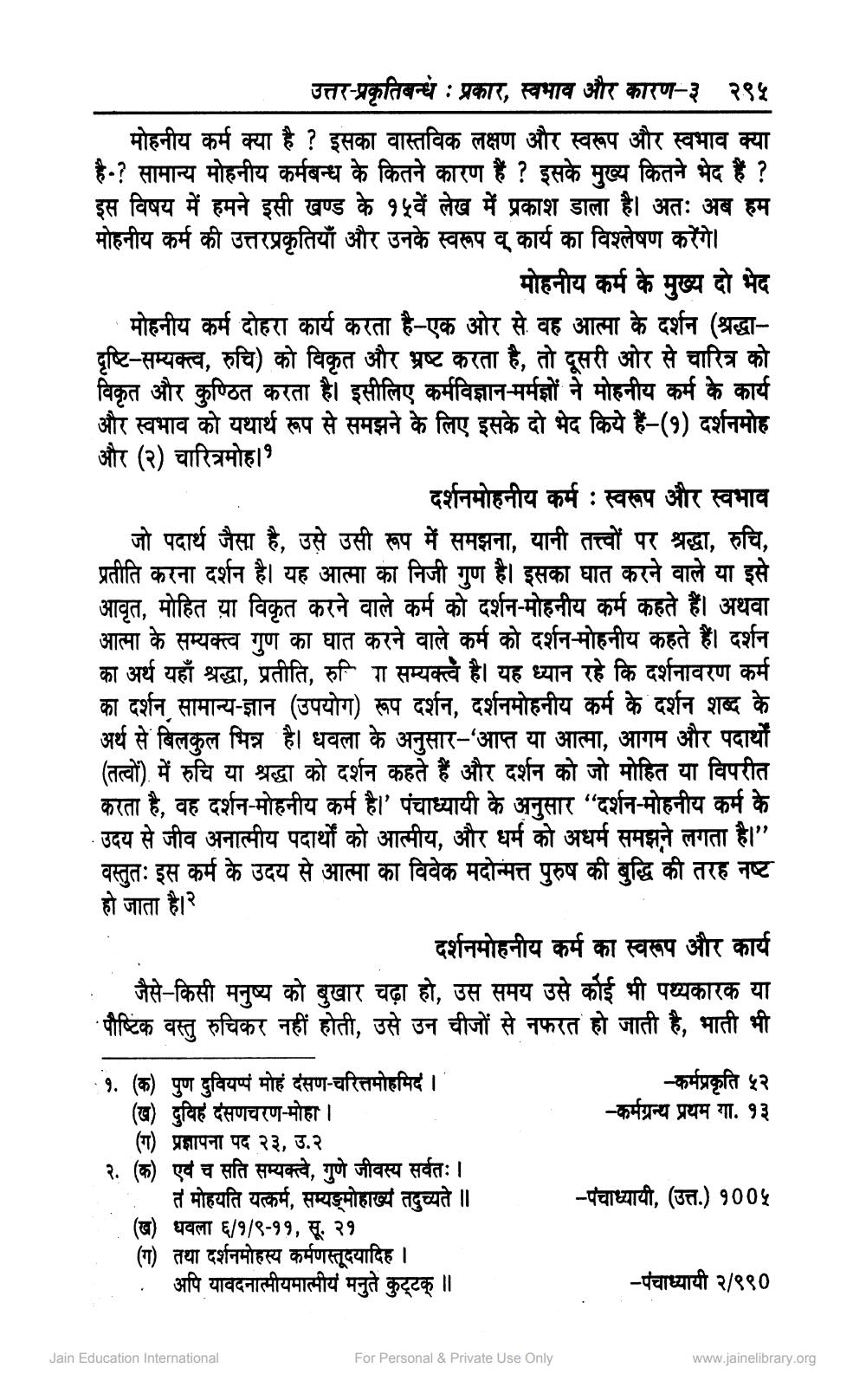________________
उत्तर-प्रकृतिबन्ध : प्रकार, स्वभाव और कारण-३ २९५ मोहनीय कर्म क्या है ? इसका वास्तविक लक्षण और स्वरूप और स्वभाव क्या है.? सामान्य मोहनीय कर्मबन्ध के कितने कारण हैं ? इसके मुख्य कितने भेद हैं ? इस विषय में हमने इसी खण्ड के १५वें लेख में प्रकाश डाला है। अतः अब हम मोहनीय कर्म की उत्तरप्रकृतियाँ और उनके स्वरूप व कार्य का विश्लेषण करेंगे।
मोहनीय कर्म के मुख्य दो भेद - मोहनीय कर्म दोहरा कार्य करता है-एक ओर से. वह आत्मा के दर्शन (श्रद्धादृष्टि-सम्यक्त्व, रुचि) को विकृत और भ्रष्ट करता है, तो दूसरी ओर से चारित्र को विकृत और कुण्ठित करता है। इसीलिए कर्मविज्ञान-मर्मज्ञों ने मोहनीय कर्म के कार्य और स्वभाव को यथार्थ रूप से समझने के लिए इसके दो भेद किये हैं-(१) दर्शनमोह और (२) चारित्रमोह।'
दर्शनमोहनीय कर्म : स्वरूप और स्वभाव जो पदार्थ जैसा है, उसे उसी रूप में समझना, यानी तत्त्वों पर श्रद्धा, रुचि, प्रतीति करना दर्शन है। यह आत्मा का निजी गण है। इसका घात करने वाले या इसे आवृत, मोहित या विकृत करने वाले कर्म को दर्शन-मोहनीय कर्म कहते हैं। अथवा आत्मा के सम्यक्त्व गुण का घात करने वाले कर्म को दर्शन-मोहनीय कहते हैं। दर्शन का अर्थ यहाँ श्रद्धा, प्रतीति, रुाि सम्यक्त्व है। यह ध्यान रहे कि दर्शनावरण कर्म का दर्शन सामान्य-ज्ञान (उपयोग) रूप दर्शन, दर्शनमोहनीय कर्म के दर्शन शब्द के अर्थ से बिलकुल भिन्न है। धवला के अनुसार-'आप्त या आत्मा, आगम और पदार्थों (तत्वों) में रुचि या श्रद्धा को दर्शन कहते हैं और दर्शन को जो मोहित या विपरीत करता है, वह दर्शन-मोहनीय कर्म है।' पंचाध्यायी के अनुसार “दर्शन-मोहनीय कर्म के उदय से जीव अनात्मीय पदार्थों को आत्मीय, और धर्म को अधर्म समझने लगता है।" वस्तुतः इस कर्म के उदय से आत्मा का विवेक मदोन्मत्त पुरुष की बुद्धि की तरह नष्ट हो जाता है।
दर्शनमोहनीय कर्म का स्वरूप और कार्य जैसे-किसी मनुष्य को बुखार चढ़ा हो, उस समय उसे कोई भी पथ्यकारक या पौष्टिक वस्तु रुचिकर नहीं होती, उसे उन चीजों से नफरत हो जाती है, भाती भी
-कर्मप्रकृति ५२ -कर्मग्रन्य प्रथम गा. १३
१. (क) पुण दुवियप्पं मोहं दसण-चरित्तमोहमिदं ।
(ख) दुविहं दसणचरण-मोहा।
(ग) प्रज्ञापना पद २३, उ.२ २. (क) एवं च सति सम्यक्त्वे, गुणे जीवस्य सर्वतः ।
त मोहयति यत्कर्म, सम्यङ्मोहाख्यं तदुच्यते ॥ (ख) धवला ६/१/९-११, सू. २१ (ग) तथा दर्शनमोहस्य कर्मणस्तूदयादिह । __ अपि यावदनात्मीयमात्मीयं मनुते कुट्टक् ॥
-पंचाध्यायी, (उत्त.) १००५
-पंचाध्यायी २/९९०
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org