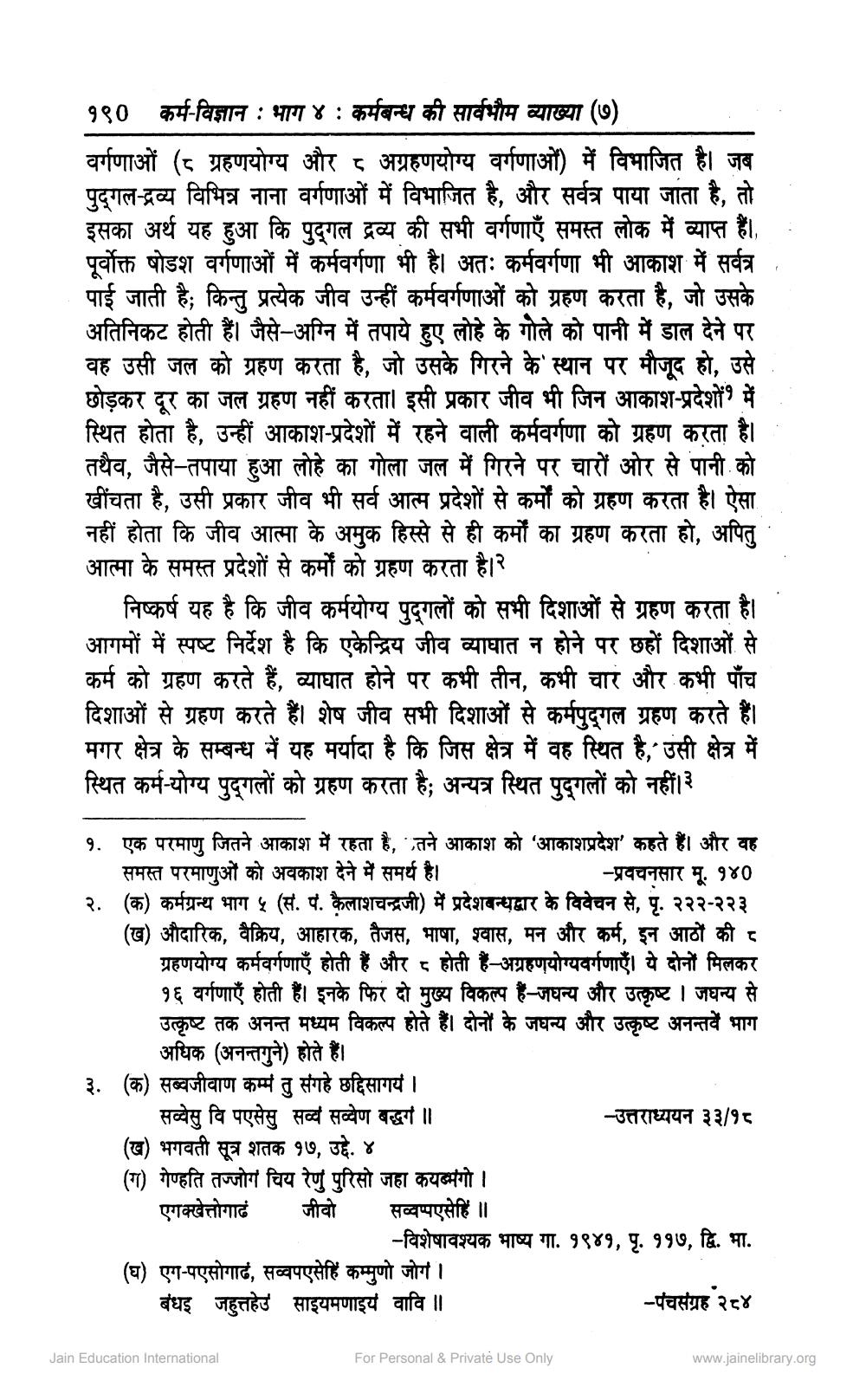________________
१९० कर्म-विज्ञान : भाग ४ : कर्मबन्ध की सार्वभौम व्याख्या (७) वर्गणाओं (८ ग्रहणयोग्य और ८ अग्रहणयोग्य वर्गणाओं) में विभाजित है। जब पुद्गल-द्रव्य विभिन्न नाना वर्गणाओं में विभाजित है, और सर्वत्र पाया जाता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पुद्गल द्रव्य की सभी वर्गणाएँ समस्त लोक में व्याप्त हैं। पूर्वोक्त षोडश वर्गणाओं में कर्मवर्गणा भी है। अतः कर्मवर्गणा भी आकाश में सर्वत्र पाई जाती है; किन्तु प्रत्येक जीव उन्हीं कर्मवर्गणाओं को ग्रहण करता है, जो उसके अतिनिकट होती हैं। जैसे-अग्नि में तपाये हुए लोहे के गोले को पानी में डाल देने पर वह उसी जल को ग्रहण करता है, जो उसके गिरने के स्थान पर मौजूद हो, उसे छोड़कर दूर का जल ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार जीव भी जिन आकाश-प्रदेशों में स्थित होता है, उन्हीं आकाश-प्रदेशों में रहने वाली कर्मवर्गणा को ग्रहण करता है। तथैव, जैसे-तपाया हुआ लोहे का गोला जल में गिरने पर चारों ओर से पानी को खींचता है, उसी प्रकार जीव भी सर्व आत्म प्रदेशों से कर्मों को ग्रहण करता है। ऐसा नहीं होता कि जीव आत्मा के अमुक हिस्से से ही कर्मों का ग्रहण करता हो, अपितु आत्मा के समस्त प्रदेशों से कर्मों को ग्रहण करता है।२
निष्कर्ष यह है कि जीव कर्मयोग्य पुद्गलों को सभी दिशाओं से ग्रहण करता है। आगमों में स्पष्ट निर्देश है कि एकेन्द्रिय जीव व्याघात न होने पर छहों दिशाओं से कर्म को ग्रहण करते हैं, व्याघात होने पर कभी तीन, कभी चार और कभी पाँच दिशाओं से ग्रहण करते हैं। शेष जीव सभी दिशाओं से कर्मपुद्गल ग्रहण करते हैं। मगर क्षेत्र के सम्बन्ध में यह मर्यादा है कि जिस क्षेत्र में वह स्थित है, उसी क्षेत्र में स्थित कर्म-योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है; अन्यत्र स्थित पुद्गलों को नहीं।३
१. एक परमाणु जितने आकाश में रहता है, तने आकाश को 'आकाशप्रदेश' कहते हैं। और वह समस्त परमाणुओं को अवकाश देने में समर्थ है।
-प्रवचनसार मू. १४० २. (क) कर्मग्रन्थ भाग ५ (सं. पं. कैलाशचन्द्रजी) में प्रदेशबन्धद्वार के विवेचन से, पृ. २२२-२२३ (ख) औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, भाषा, श्वास, मन और कर्म, इन आठों की ८
ग्रहणयोग्य कर्मवर्गणाएँ होती हैं और ८ होती हैं-अग्रहणयोग्यवर्गणाएँ। ये दोनों मिलकर १६ वर्गणाएँ होती हैं। इनके फिर दो मुख्य विकल्प हैं-जघन्य और उत्कृष्ट । जघन्य से उत्कृष्ट तक अनन्त मध्यम विकल्प होते हैं। दोनों के जघन्य और उत्कृष्ट अनन्तवें भाग
अधिक (अनन्तगुने) होते हैं। ३. (क) सब्वजीवाण कम्मं तु संगहे छद्दिसागय । सव्येसु वि पएसेसु सव्व सव्येण बद्धग ॥
-उत्तराध्ययन ३३/१८ (ख) भगवती सूत्र शतक १७, उद्दे. ४ (ग) गेहति तज्जोग चिय रेणु पुरिसो जहा कयन्मंगो । एगक्खेत्तोगाढं जीवो सव्वप्पएसेहिं ॥
-विशेषावश्यक भाष्य गा. १९४१, पृ. ११७, द्वि. भा. (घ) एग-पएसोगाढं, सव्वपएसेहिं कम्मुणो जोग । बंधइ जहुत्तहेउं साइयमणाइयं वावि ॥
-पंचसंग्रह २८४
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org