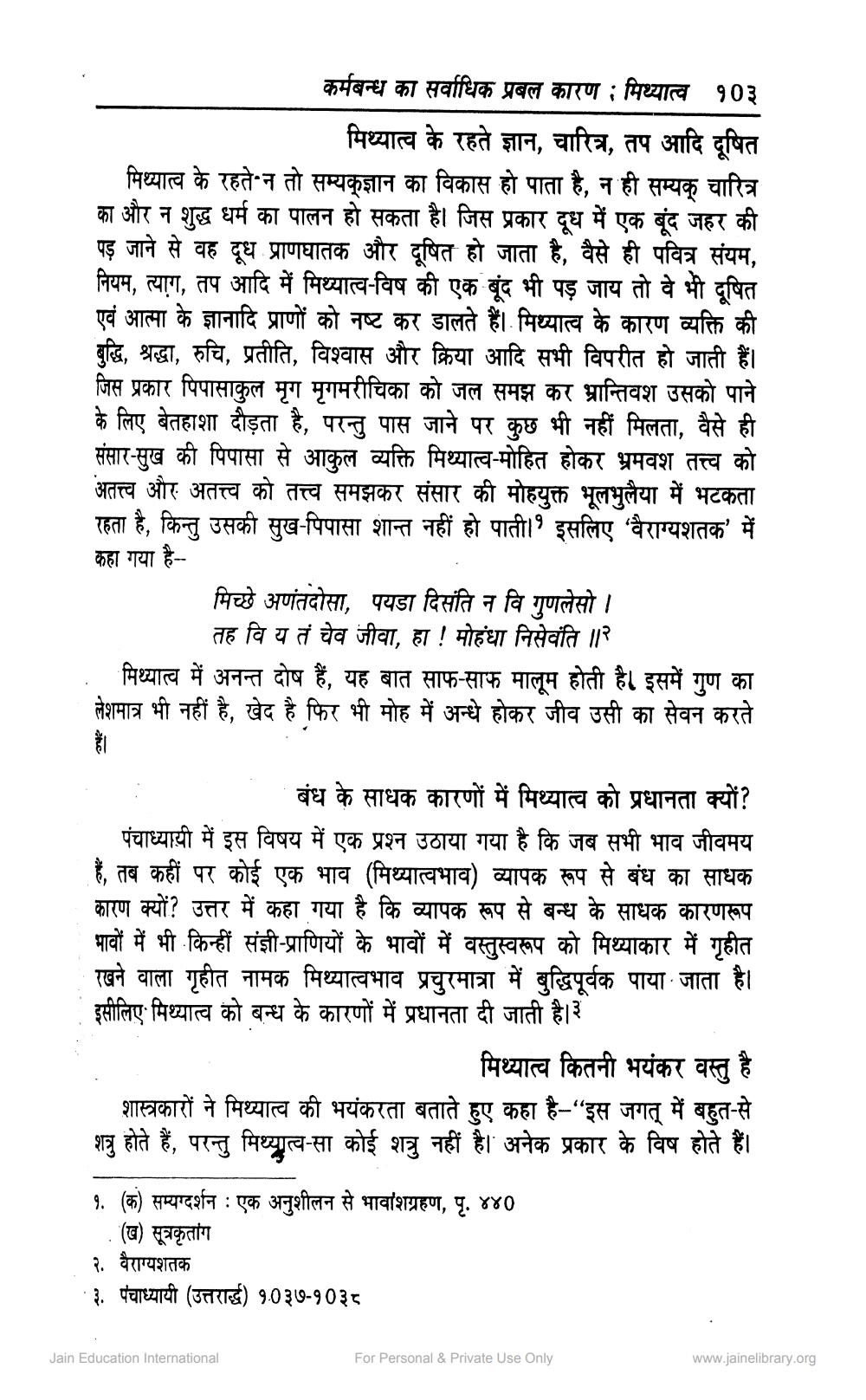________________
कर्मबन्ध का सर्वाधिक प्रबल कारण : मिथ्यात्व १०३
मिथ्यात्व के रहते ज्ञान, चारित्र, तप आदि दूषित मिथ्यात्व के रहते न तो सम्यक्ज्ञान का विकास हो पाता है, न ही सम्यक् चारित्र का और न शुद्ध धर्म का पालन हो सकता है। जिस प्रकार दूध में एक बूंद जहर की पड़ जाने से वह दूध प्राणघातक और दूषित हो जाता है, वैसे ही पवित्र संयम, नियम, त्याग, तप आदि में मिथ्यात्व-विष की एक बूंद भी पड़ जाय तो वे भी दूषित एवं आत्मा के ज्ञानादि प्राणों को नष्ट कर डालते हैं। मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति की बुद्धि, श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, विश्वास और क्रिया आदि सभी विपरीत हो जाती हैं। जिस प्रकार पिपासाकुल मृग मृगमरीचिका को जल समझ कर भ्रान्तिवश उसको पाने के लिए बेतहाशा दौड़ता है, परन्तु पास जाने पर कुछ भी नहीं मिलता, वैसे ही संसार-सुख की पिपासा से आकुल व्यक्ति मिथ्यात्व-मोहित होकर भ्रमवश तत्त्व को अतत्त्व और अतत्त्व को तत्त्व समझकर संसार की मोहयुक्त भूलभुलैया में भटकता रहता है, किन्तु उसकी सुख-पिपासा शान्त नहीं हो पाती। इसलिए 'वैराग्यशतक' में कहा गया है
मिच्छे अणंतदोसा, पयडा दिसंति न वि गुणलेसो ।
तह वि य तं चेव जीवा, हा ! मोहंधा निसेवंति ॥२ मिथ्यात्व में अनन्त दोष हैं, यह बात साफ-साफ मालूम होती है। इसमें गुण का लेशमात्र भी नहीं है, खेद है फिर भी मोह में अन्धे होकर जीव उसी का सेवन करते
बंध के साधक कारणों में मिथ्यात्व को प्रधानता क्यों? पंचाध्यायी में इस विषय में एक प्रश्न उठाया गया है कि जब सभी भाव जीवमय हैं, तब कहीं पर कोई एक भाव (मिथ्यात्वभाव) व्यापक रूप से बंध का साधक कारण क्यों? उत्तर में कहा गया है कि व्यापक रूप से बन्ध के साधक कारणरूप भावों में भी किन्हीं संज्ञी-प्राणियों के भावों में वस्तुस्वरूप को मिथ्याकार में गृहीत रखने वाला गृहीत नामक मिथ्यात्वभाव प्रचुरमात्रा में बुद्धिपूर्वक पाया जाता है। इसीलिए मिथ्यात्व को बन्ध के कारणों में प्रधानता दी जाती है।३
मिथ्यात्व कितनी भयंकर वस्तु है शास्त्रकारों ने मिथ्यात्व की भयंकरता बताते हुए कहा है-"इस जगत् में बहुत-से शत्रु होते हैं, परन्तु मिथ्यात्व-सा कोई शत्रु नहीं है। अनेक प्रकार के विष होते हैं।
१. (क) सम्यग्दर्शन : एक अनुशीलन से भावशिग्रहण, पृ. ४४०
(ख) सूत्रकृतांग २. वैराग्यशतक ३. पंचाध्यायी (उत्तरार्द्ध) १०३७-१०३८
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org