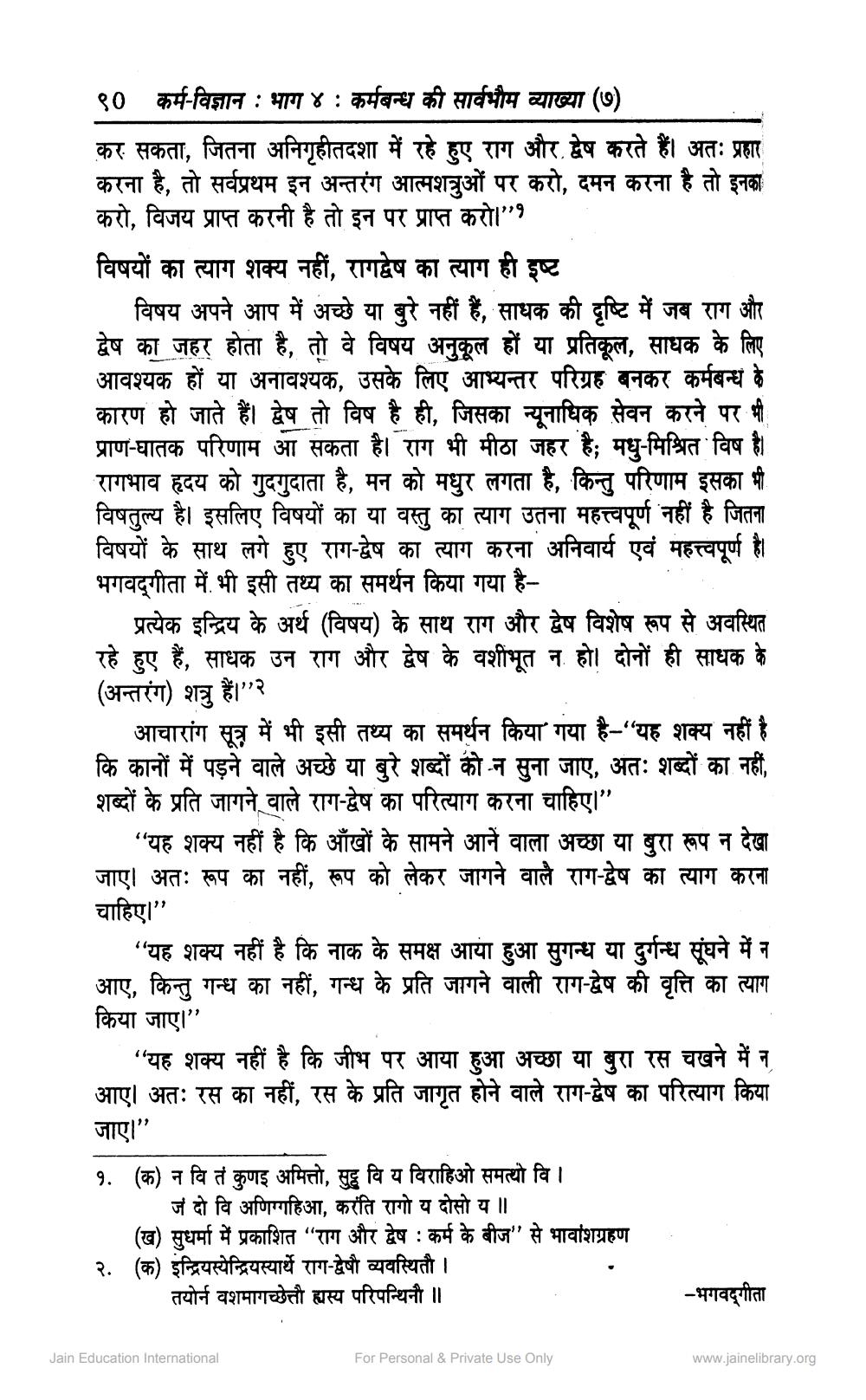________________
९० कर्म-विज्ञान : भाग ४ : कर्मबन्ध की सार्वभौम व्याख्या (७) कर सकता, जितना अनिगृहीतदशा में रहे हुए राग और द्वेष करते हैं। अतः प्रहार करना है, तो सर्वप्रथम इन अन्तरंग आत्मशत्रुओं पर करो, दमन करना है तो इनका करो, विजय प्राप्त करनी है तो इन पर प्राप्त करो।"१ विषयों का त्याग शक्य नहीं, रागद्वेष का त्याग ही इष्ट
विषय अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं हैं, साधक की दृष्टि में जब राग और द्वेष का जहर होता है, तो वे विषय अनुकूल हों या प्रतिकूल, साधक के लिए आवश्यक हों या अनावश्यक, उसके लिए आभ्यन्तर परिग्रह बनकर कर्मबन्ध के कारण हो जाते हैं। द्वेष तो विष है ही, जिसका न्यूनाधिक सेवन करने पर भी प्राण-घातक परिणाम आ सकता है। राग भी मीठा जहर है; मधु-मिश्रित विष है। रागभाव हृदय को गुदगुदाता है, मन को मधुर लगता है, किन्तु परिणाम इसका भी विषतुल्य है। इसलिए विषयों का या वस्तु का त्याग उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना विषयों के साथ लगे हुए राग-द्वेष का त्याग करना अनिवार्य एवं महत्त्वपूर्ण है। भगवद्गीता में भी इसी तथ्य का समर्थन किया गया है
प्रत्येक इन्द्रिय के अर्थ (विषय) के साथ राग और द्वेष विशेष रूप से अवस्थित रहे हुए हैं, साधक उन राग और द्वेष के वशीभूत न हो। दोनों ही साधक के (अन्तरंग) शत्रु हैं।"२
__ आचारांग सूत्र में भी इसी तथ्य का समर्थन किया गया है-“यह शक्य नहीं है कि कानों में पड़ने वाले अच्छे या बरे शब्दों को न सुना जाए, अतः शब्दों का नहीं, शब्दों के प्रति जागने वाले राग-द्वेष का परित्याग करना चाहिए।" __"यह शक्य नहीं है कि आँखों के सामने आने वाला अच्छा या बुरा रूप न देखा जाए। अतः रूप का नहीं, रूप को लेकर जागने वाले राग-द्वेष का त्याग करना चाहिए।"
"यह शक्य नहीं है कि नाक के समक्ष आया हुआ सुगन्ध या दुर्गन्ध सूंघने में न आए, किन्तु गन्ध का नहीं, गन्ध के प्रति जागने वाली राग-द्वेष की वृत्ति का त्याग किया जाए।"
“यह शक्य नहीं है कि जीभ पर आया हुआ अच्छा या बुरा रस चखने में न आए। अतः रस का नहीं, रस के प्रति जागृत होने वाले राग-द्वेष का परित्याग किया जाए।" १. (क) न वि तं कुणइ अमित्तो, सुट्ठ वि य विराहिओ समत्यो वि ।
जं दो वि अणिग्गहिआ, करंति रागो य दोसो य ॥ (ख) सुधर्मा में प्रकाशित "राग और द्वेष : कर्म के बीज" से भावांशग्रहण २. (क) इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग-द्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोर्न वशमागछेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनी ॥
-भगवद्गीता
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org