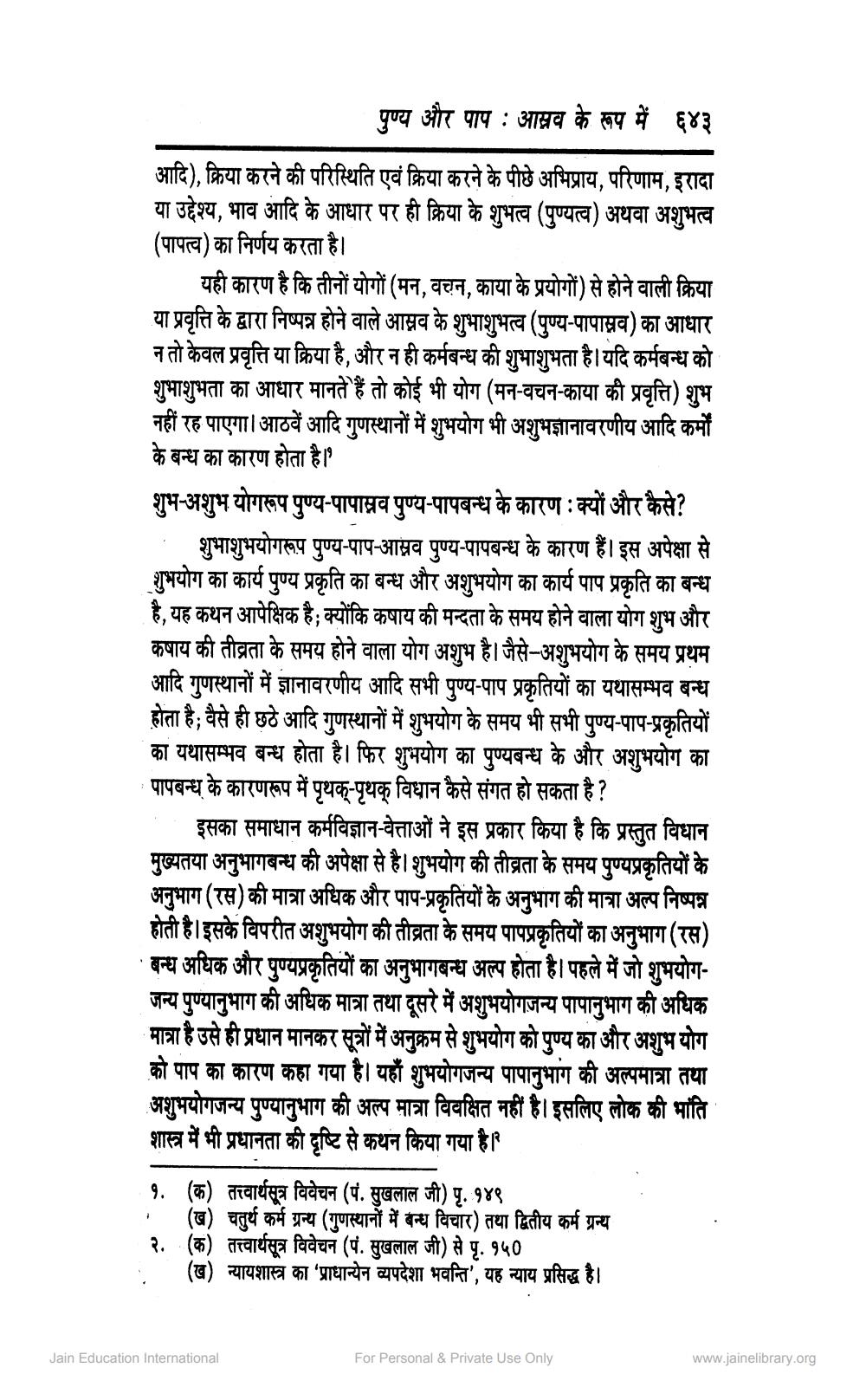________________
पुण्य और पाप : आनव के रूप में ६४३
आदि), क्रिया करने की परिस्थिति एवं क्रिया करने के पीछे अभिप्राय, परिणाम, इरादा या उद्देश्य, भाव आदि के आधार पर ही क्रिया के शुभत्व (पुण्यत्व) अथवा अशुभत्व (पापत्व) का निर्णय करता है।
यही कारण है कि तीनों योगों (मन, वचन, काया के प्रयोगों) से होने वाली क्रिया या प्रवृत्ति के द्वारा निष्पन्न होने वाले आनव के शुभाशुभत्व (पुण्य-पापानव) का आधार न तो केवल प्रवृत्ति या क्रिया है, और न ही कर्मबन्ध की शुभाशुभता है। यदि कर्मबन्ध को शुभाशुभता का आधार मानते हैं तो कोई भी योग ( मन-वचन काया की प्रवृत्ति) शुभ नहीं रह पाएगा। आठवें आदि गुणस्थानों में शुभयोग भी अशुभज्ञानावरणीय आदि कर्मों बन्धका कारण होता है।'
शुभ-अशुभ योगरूप पुण्य-पापास्नव पुण्य-पापबन्ध के कारण : क्यों और कैसे ?
शुभाशुभयोगरूप पुण्य-पाप- आस्रव पुण्य-पापबन्ध के कारण हैं। इस अपेक्षा से _शुभयोग का कार्य पुण्य प्रकृति का बन्ध और अशुभयोग का कार्य पाप प्रकृति का बन्ध है, यह कथन आपेक्षिक है; क्योंकि कषाय की मन्दता के समय होने वाला योग शुभ और कषाय की तीव्रता के समय होने वाला योग अशुभ है। जैसे- अशुभयोग के समय प्रथम आदि गुणस्थानों में ज्ञानावरणीय आदि सभी पुण्य-पाप प्रकृतियों का यथासम्भव बन्ध होता है, वैसे ही छठे आदि गुणस्थानों में शुभयोग के समय भी सभी पुण्य-पाप-प्रकृतियों का यथासम्भव बन्ध होता है। फिर शुभयोग का पुण्यबन्ध के और अशुभयोग का पापबन्ध के कारणरूप में पृथक्-पृथक् विधान कैसे संगत हो सकता है ?
इसका समाधान कर्मविज्ञान-वेत्ताओं ने इस प्रकार किया है कि प्रस्तुत विधान मुख्यतया अनुभागबन्ध की अपेक्षा से है। शुभयोग की तीव्रता के समय पुण्यप्रकृतियों के अनुभाग (रस) की मात्रा अधिक और पाप-प्रकृतियों के अनुभाग की मात्रा अल्प निष्पन्न होती है। इसके विपरीत अशुभयोग की तीव्रता के समय पापप्रकृतियों का अनुभाग (रस) 'बन्ध अधिक और पुण्यप्रकृतियों का अनुभागबन्ध अल्प होता है। पहले में जो शुभयोगजन्य पुण्यानुभाग की अधिक मात्रा तथा दूसरे में अशुभयोगजन्य पापानुभाग की अधिक मात्रा है उसे ही प्रधान मानकर सूत्रों में अनुक्रम से शुभयोग को पुण्य का और अशुभ योग को पाप का कारण कहा गया है। यहाँ शुभयोगजन्य पापानुभाग की अल्पमात्रा तथा अशुभयोगजन्य पुण्यानुभाग की अल्प मात्रा विवक्षित नहीं है। इसलिए लोक की भांति शास्त्र में भी प्रधानता की दृष्टि से कथन किया गया है।
1
१. (क) तत्त्वार्थसूत्र विवेचन (पं. सुखलाल जी) पृ. १४९
(ख) चतुर्थ कर्म ग्रन्थ ( गुणस्थानों में बन्ध विचार) तथा द्वितीय कर्म ग्रन्थ
२. (क) तत्त्वार्थसूत्र विवेचन (पं. सुखलाल जी) से पृ. १५०
(ख) न्यायशास्त्र का 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति', यह न्याय प्रसिद्ध है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org