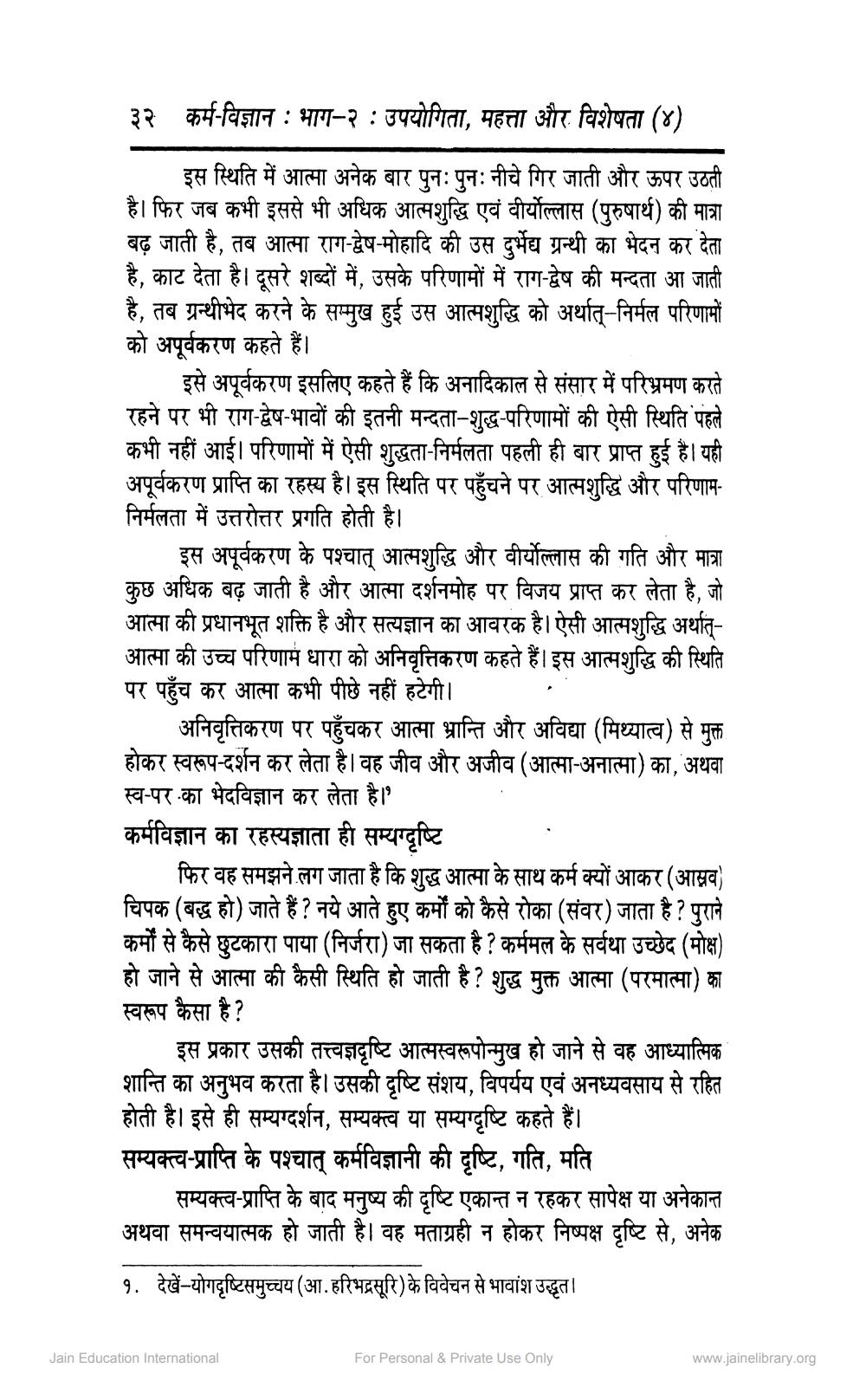________________
३२ कर्म-विज्ञान : भाग - २ : उपयोगिता, महत्ता और विशेषता (४)
इस स्थिति में आत्मा अनेक बार पुनः पुनः नीचे गिर जाती और ऊपर उठती है। फिर जब कभी इससे भी अधिक आत्मशुद्धि एवं वीर्योल्लास (पुरुषार्थ) की मात्रा बढ़ जाती है, तब आत्मा राग-द्वेष- मोहादि की उस दुर्भेद्य ग्रन्थी का भेदन कर देता है, काट देता है। दूसरे शब्दों में, उसके परिणामों में राग-द्वेष की मन्दता आ जाती है, तब ग्रन्थीभेद करने के सम्मुख हुई उस आत्मशुद्धि को अर्थात्-निर्मल परिणामों at अपूर्वकरण कहते हैं।
इसे अपूर्वकरण इसलिए कहते हैं कि अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते रहने पर भी राग-द्वेष-भावों की इतनी मन्दता-शुद्ध- परिणामों की ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। परिणामों में ऐसी शुद्धता-निर्मलता पहली ही बार प्राप्त हुई है। यही अपूर्वकरण प्राप्ति का रहस्य है। इस स्थिति पर पहुँचने पर आत्मशुद्धि और परिणामनिर्मलता में उत्तरोत्तर प्रगति होती है।
इस अपूर्वकरण के पश्चात् आत्मशुद्धि और वीर्योल्लास की गति और मात्रा कुछ अधिक बढ़ जाती है और आत्मा दर्शनमोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो आत्मा की प्रधानभूत शक्ति है और सत्यज्ञान का आवरक है। ऐसी आत्मशुद्धि अर्थात्आत्मा की उच्च परिणाम धारा को अनिवृत्तिकरण कहते हैं । इस आत्मशुद्धि की स्थिति पर पहुँच कर आत्मा कभी पीछे नहीं हटेगी।
अनिवृत्तिकरण पर पहुँचकर आत्मा भ्रान्ति और अविद्या ( मिथ्यात्व) से मुक्त होकर स्वरूप-दर्शन कर लेता है। वह जीव और अजीव (आत्मा-अनात्मा) का, स्व-पर का भेदविज्ञान कर लेता है।'
अथवा
कर्मविज्ञान का रहस्यज्ञाता ही सम्यग्दृष्टि
फिर वह समझने लग जाता है कि शुद्ध आत्मा के साथ कर्म क्यों आकर (आव) चिपक (बद्ध हो जाते हैं ? नये आते हुए कर्मों को कैसे रोका (संवर) जाता है ? पुराने कर्मों से कैसे छुटकारा पाया (निर्जरा) जा सकता है ? कर्ममल के सर्वथा उच्छेद (मोक्ष) हो जाने से आत्मा की कैसी स्थिति हो जाती है ? शुद्ध मुक्त आत्मा (परमात्मा) का स्वरूप कैसा है ?
इस प्रकार उसकी तत्त्वज्ञदृष्टि आत्मस्वरूपोन्मुख हो जाने से वह आध्यात्मिक शान्ति का अनुभव करता है। उसकी दृष्टि संशय, विपर्यय एवं अनध्यवसाय से रहित होती है। इसे ही सम्यग्दर्शन, सम्यक्त्व या सम्यग्दृष्टि कहते हैं।
सम्यक्त्व-प्राप्ति के पश्चात् कर्मविज्ञानी की दृष्टि, गति, मति
सम्यक्त्व-प्राप्ति के बाद मनुष्य की दृष्टि एकान्त न रहकर सापेक्ष या अनेकान्त अथवा समन्वयात्मक हो जाती है। वह मताग्रही न होकर निष्पक्ष दृष्टि से, अनेक
१. देखें- योगदृष्टिसमुच्चय (आ. हरिभद्रसूरि) के विवेचन से भावांश उद्धृत
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org