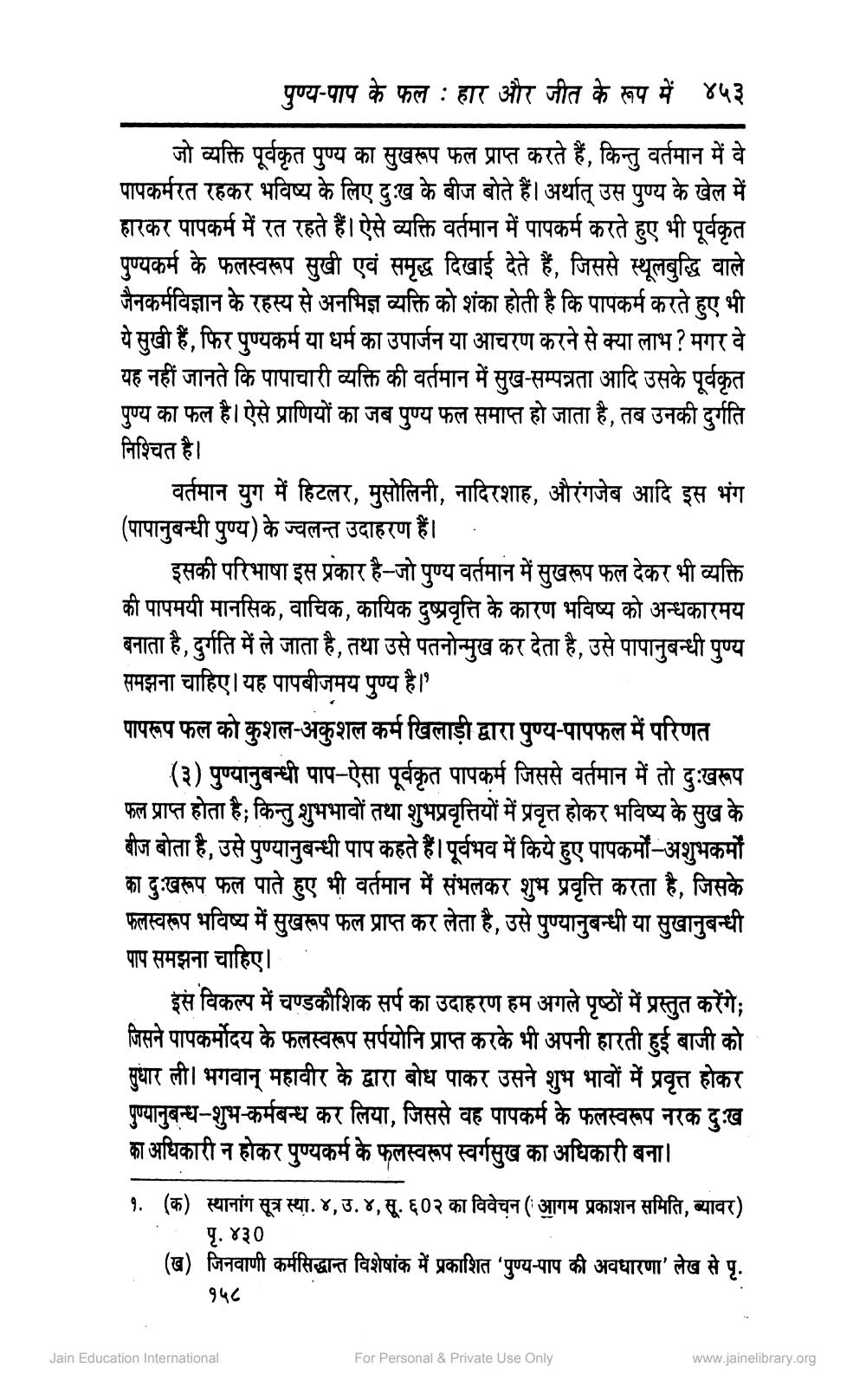________________
पुण्य-पाप के फल : हार और जीत के रूप में ४५३ जो व्यक्ति पूर्वकृत पुण्य का सुखरूप फल प्राप्त करते हैं, किन्तु वर्तमान में वे पापकर्मरत रहकर भविष्य के लिए दुःख के बीज बोते हैं। अर्थात् उस पुण्य के खेल में हारकर पापकर्म में रत रहते हैं। ऐसे व्यक्ति वर्तमान में पापकर्म करते हुए भी पूर्वकृत पुण्यकर्म के फलस्वरूप सुखी एवं समृद्ध दिखाई देते हैं, जिससे स्थूलबुद्धि वाले जैनकर्मविज्ञान के रहस्य से अनभिज्ञ व्यक्ति को शंका होती है कि पापकर्म करते हुए भी ये सुखी हैं, फिर पुण्यकर्म या धर्म का उपार्जन या आचरण करने से क्या लाभ? मगर वे यह नहीं जानते कि पापाचारी व्यक्ति की वर्तमान में सुख-सम्पन्नता आदि उसके पूर्वकृत पुण्य का फल है। ऐसे प्राणियों का जब पुण्य फल समाप्त हो जाता है, तब उनकी दुर्गति निश्चित है।
वर्तमान युग में हिटलर, मुसोलिनी, नादिरशाह, औरंगजेब आदि इस भंग (पापानुबन्धी पुण्य) के ज्वलन्त उदाहरण हैं। .
इसकी परिभाषा इस प्रकार है-जो पुण्य वर्तमान में सुखरूप फल देकर भी व्यक्ति की पापमयी मानसिक, वाचिक, कायिक दुष्प्रवृत्ति के कारण भविष्य को अन्धकारमय बनाता है, दुर्गति में ले जाता है, तथा उसे पतनोन्मुख कर देता है, उसे पापानुबन्धी पुण्य समझना चाहिए। यह पापबीजमय पुण्य है।' पापरूप फल को कुशल-अकुशल कर्म खिलाड़ी द्वारा पुण्य-पापफल में परिणत
(३) पुण्यानुबन्धी पाप-ऐसा पूर्वकृत पापकर्म जिससे वर्तमान में तो दुःखरूप फल प्राप्त होता है; किन्तु शुभभावों तथा शुभप्रवृत्तियों में प्रवृत्त होकर भविष्य के सुख के बीज बोता है, उसे पुण्यानुबन्धी पाप कहते हैं। पूर्वभव में किये हुए पापकर्मों-अशुभकर्मों का दुःखरूप फल पाते हुए भी वर्तमान में संभलकर शुभ प्रवृत्ति करता है, जिसके फलस्वरूप भविष्य में सुखरूप फल प्राप्त कर लेता है, उसे पुण्यानुबन्धी या सुखानुबन्धी पाप समझना चाहिए। __इस विकल्प में चण्डकौशिक सर्प का उदाहरण हम अगले पृष्ठों में प्रस्तुत करेंगे; जिसने पापकर्मोदय के फलस्वरूप सर्पयोनि प्राप्त करके भी अपनी हारती हुई बाजी को सुधार ली। भगवान् महावीर के द्वारा बोध पाकर उसने शुभ भावों में प्रवृत्त होकर पुण्यानुबन्ध-शुभ-कर्मबन्ध कर लिया, जिससे वह पापकर्म के फलस्वरूप नरक दुःख का अधिकारी न होकर पुण्यकर्म के फलस्वरूप स्वर्गसुख का अधिकारी बना। १. (क) स्थानांग सूत्र स्था. ४, उ. ४, सू. ६०२ का विवेचन ( आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर)
पृ. ४३० (ख) जिनवाणी कर्मसिद्धान्त विशेषांक में प्रकाशित 'पुण्य-पाप की अवधारणा' लेख से पृ.
१५८
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org