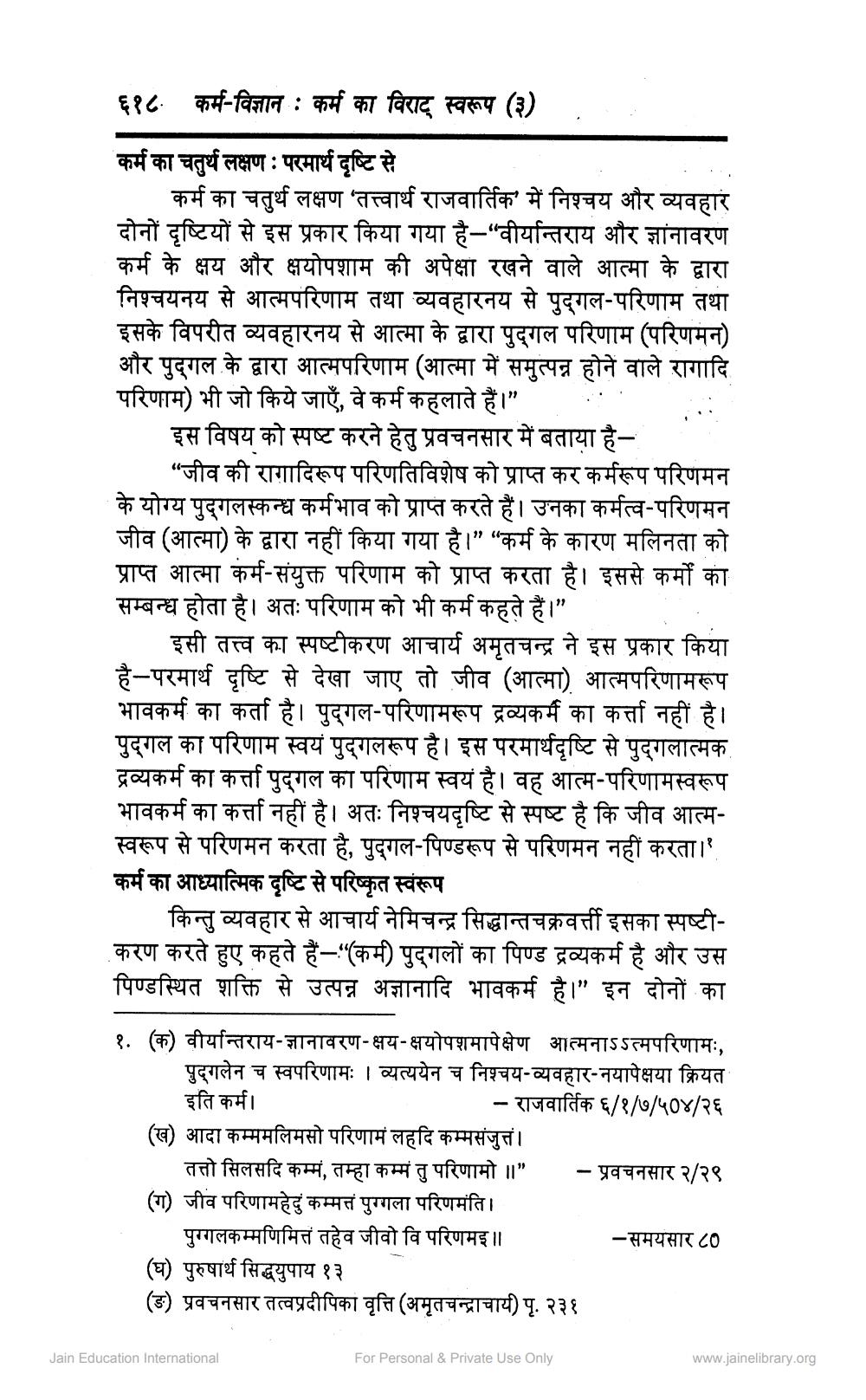________________
६१८. कर्म-विज्ञान : कर्म का विराट् स्वरूप (३)
कर्म का चतुर्थ लक्षण : परमार्थ दृष्टि से __कर्म का चतुर्थ लक्षण 'तत्त्वार्थ राजवार्तिक' में निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों से इस प्रकार किया गया है-“वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षय और क्षयोपशाम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के द्वारा निश्चयनय से आत्मपरिणाम तथा व्यवहारनय से पुद्गल-परिणाम तथा इसके विपरीत व्यवहारनय से आत्मा के द्वारा पुद्गल परिणाम (परिणमन)
और पुद्गल के द्वारा आत्मपरिणाम (आत्मा में समुत्पन्न होने वाले रागादि परिणाम) भी जो किये जाएँ, वे कर्म कहलाते हैं।"
इस विषय को स्पष्ट करने हेतु प्रवचनसार में बताया है
"जीव की रागादिरूप परिणतिविशेष को प्राप्त कर कर्मरूप परिणमन के योग्य पुद्गलस्कन्ध कर्म भाव को प्राप्त करते हैं। उनका कर्मत्व-परिणमन जीव (आत्मा) के द्वारा नहीं किया गया है।" "कर्म के कारण मलिनता को प्राप्त आत्मा कर्म-संयुक्त परिणाम को प्राप्त करता है। इससे कर्मों का सम्बन्ध होता है। अतः परिणाम को भी कर्म कहते हैं।"
इसी तत्त्व का स्पष्टीकरण आचार्य अमृतचन्द्र ने इस प्रकार किया है-परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो जीव (आत्मा) आत्मपरिणामरूप भावकर्म का कर्ता है। पुद्गगल-परिणामरूप द्रव्यकर्म का कर्ता नहीं है। पुद्गल का परिणाम स्वयं पुद्गलरूप है। इस परमार्थदृष्टि से पुद्गलात्मक द्रव्यकर्म का कर्ता पुद्गल का परिणाम स्वयं है। वह आत्म-परिणामस्वरूप भावकर्म का कर्ता नहीं है। अतः निश्चयदृष्टि से स्पष्ट है कि जीव आत्मस्वरूप से परिणमन करता है, पुद्गल-पिण्डरूप से परिणमन नहीं करता।' कर्म का आध्यात्मिक दृष्टि से परिष्कृत स्वरूप
किन्तु व्यवहार से आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं-"(कम) पुद्गलों का पिण्ड द्रव्यकर्म है और उस पिण्डस्थित शक्ति से उत्पन्न अज्ञानादि भावकर्म है।" इन दोनों का १. (क) वीर्यान्तराय-ज्ञानावरण-क्षय-क्षयोपशमापेक्षेण आत्मनाऽऽत्मपरिणामः,
पुद्गलेन च स्वपरिणामः । व्यत्ययेन च निश्चय-व्यवहार-नयापेक्षया क्रियत इति कर्म।
- राजवार्तिक ६/१/७/५०४/२६ (ख) आदा कम्ममलिमसो परिणाम लहदि कम्मसंजुत्तं ।
तत्तो सिलसदि कम्म, तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥" - प्रवचनसार २/२९ (ग) जीव परिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति। पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमइ।
-समयसार८० (घ) पुरुषार्थ सिद्धयुपाय १३ (ङ) प्रवचनसार तत्वप्रदीपिका वृत्ति (अमृतचन्द्राचाय) पृ. २३६
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org