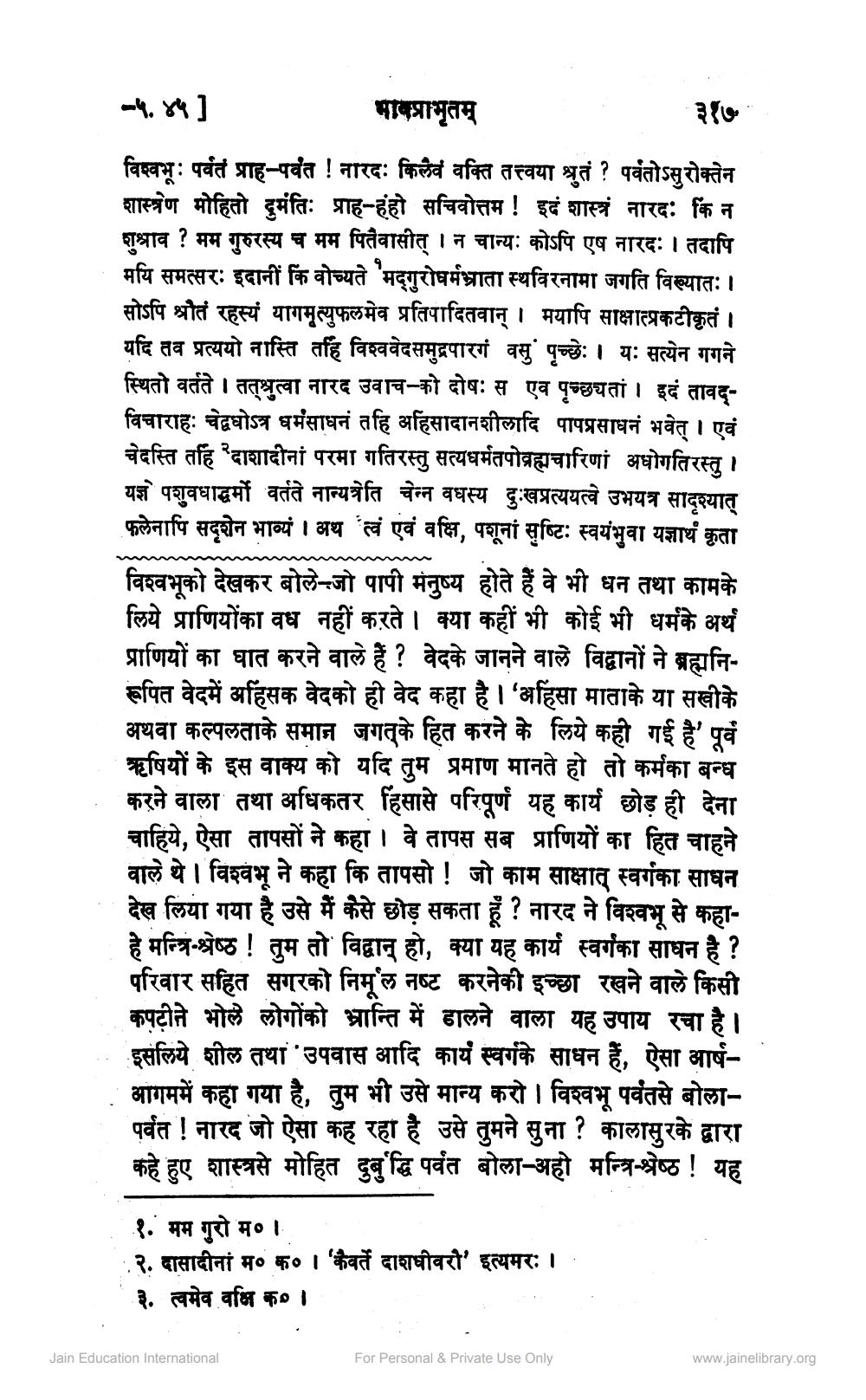________________
-५.४५ ]
भावप्राभृतम्
विश्वभू: पर्वतं प्राह - पर्वत ! नारदः किलेवं वक्ति तत्त्वया श्रुतं ? पर्वतोऽसुरोक्तेन शास्त्रेण मोहितो दुर्मतिः प्राह- हंहो सचिवोत्तम ! इदं शास्त्रं नारदः किं न शुश्राव ? मम गुरुरस्य च मम पितैवासीत् । न चान्यः कोऽपि एष नारदः । तदापि मयि समत्सरः इदानीं कि वोच्यते 'मद्गुरोधर्म भ्राता स्थविरनामा जगति विख्यातः । सोऽपि श्रौतं रहस्यं यागमृत्युफलमेव प्रतिपादितवान् । मयापि साक्षात्प्रकटीकृतं । यदि तव प्रत्ययो नास्ति तहि विश्ववेदसमुद्रपारगं वसुं पृच्छेः । यः सत्येन गगने स्थितो वर्तते । तत्श्रुत्वा नारद उवाच - को दोषः स एव पृच्छयतां । इदं तावद्विचाराहः चेद्वघोऽत्र धर्मसाधनं तहि अहिसादानशीलादि पापप्रसाधनं भवेत् । एवं चेदस्ति तर्हि 'दाशादीनां परमा गतिरस्तु सत्यधर्मतपोब्रह्मचारिणां अधोगतिरस्तु । यज्ञ पशुवधाद्धर्मो वर्तते नान्यत्रेति चेन्न वधस्य दुःखप्रत्ययत्वे उभयत्र सादृश्यात् फलेनापि सदृशेन भाव्यं । अथ त्वं एवं वक्षि, पशूनां सृष्टिः स्वयंभुवा यज्ञार्थं कृता
विश्वभूको देखकर बोले- जो पापी मनुष्य होते हैं वे भी धन तथा कामके लिये प्राणियों का वध नहीं करते। क्या कहीं भी कोई भी धर्मके अर्थ प्राणियों का घात करने वाले हैं ? वेदके जानने वाले विद्वानों ने ब्रह्मनिरूपित वेदमें अहिंसक वेदको ही वेद कहा है । 'अहिंसा माताके या सखीके अथवा कल्पलताके समान जगत् के हित करने के लिये कही गई है' पूर्व ऋषियों के इस वाक्य को यदि तुम प्रमाण मानते हो तो कर्मका बन्ध करने वाला तथा अधिकतर हिंसासे परिपूर्ण यह कार्य छोड़ ही देना चाहिये, ऐसा तापसों ने कहा । वे तापस सब प्राणियों का हित चाहने वाले थे । विश्वंभू ने कहा कि तापसो ! जो काम साक्षात् स्वर्गका साधन देख लिया गया है उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ ? नारद ने विश्वभू से कहाहे मन्त्रि श्रेष्ठ ! तुम तो विद्वान् हो, क्या यह कार्य स्वर्गका साधन है ? परिवार सहित सगरको निर्मूल नष्ट करनेकी इच्छा रखने वाले किसी कपटीने भोले लोगोंको भ्रान्ति में डालने वाला यह उपाय रचा है । इसलिये शील तथा उपवास आदि कार्यं स्वर्गके साधन हैं, ऐसा आर्षआगममें कहा गया है, तुम भी उसे मान्य करो । विश्वभू पर्वतसे बोलापर्वत ! नारद जो ऐसा कह रहा है उसे तुमने सुना? कालासुर के द्वारा कहे हुए शास्त्रसे मोहित दुर्बुद्धि पर्वत बोला- अहो मन्त्रि श्रेष्ठ ! यह
१. मम गुरो म० ।
२. दासादीनां म० क० । 'कैवर्ते दाशधीवरी' इत्यमरः ।
३. त्वमेव वक्षि क० ।
Jain Education International
३१७
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org