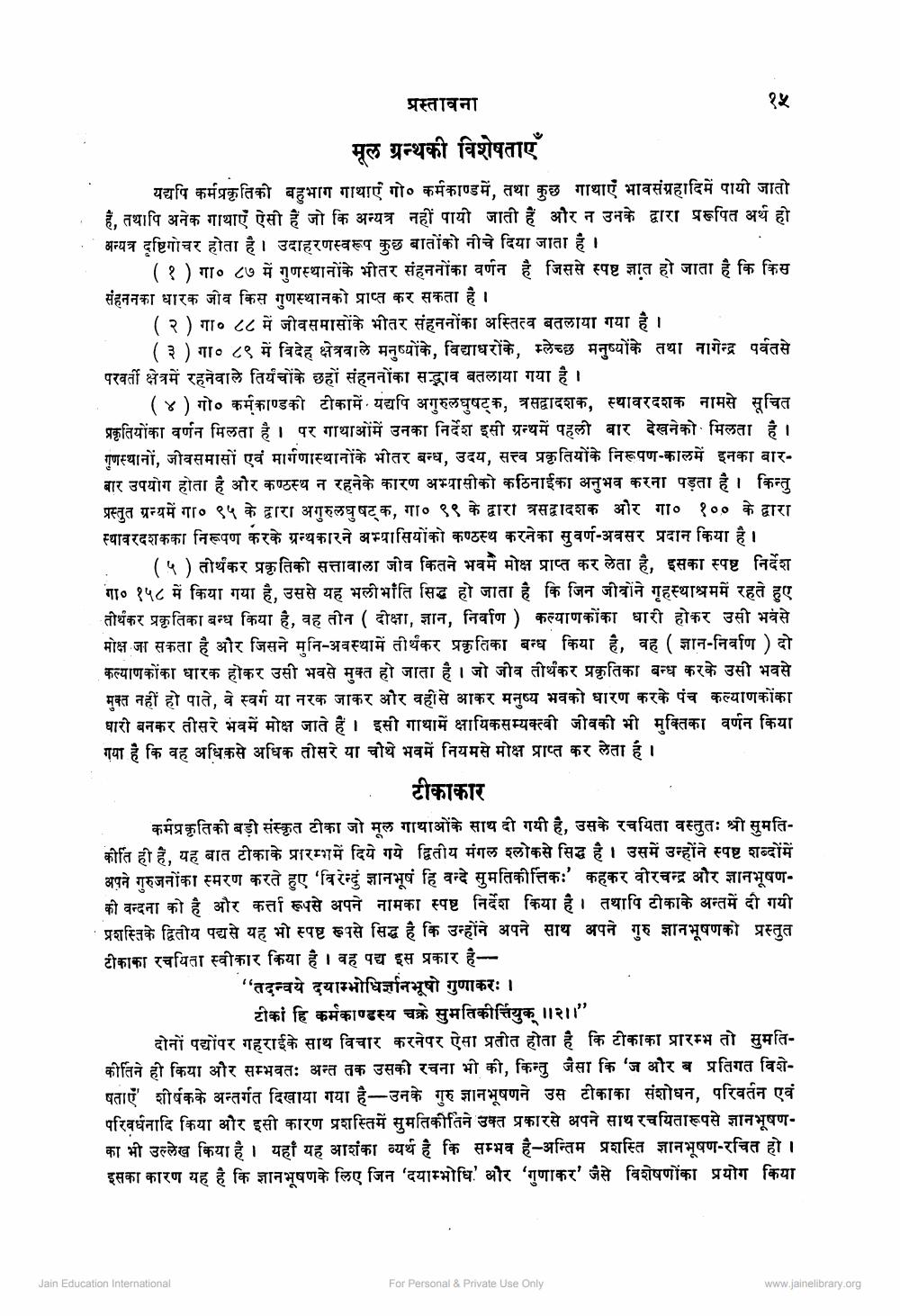________________
प्रस्तावना
मूल ग्रन्थकी विशेषताएँ
कर्मप्रकृतिको बहुभाग गाथाएं गो० कर्मकाण्ड में, तथा कुछ गाथाएँ भावसंग्रहादिमें पायी जातो हैं, तथापि अनेक गाथाएँ ऐसी हैं जो कि अन्यत्र नहीं पायी जाती हैं और न उनके द्वारा प्ररूपित अर्थ हो अन्यत्र दृष्टिगोचर होता है। उदाहरणस्वरूप कुछ बातोंको नीचे दिया जाता है ।
( १ ) गा० ८७ में गुणस्थानोंके भीतर संहननोंका वर्णन है जिससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि किस संहननका धारक जीव किस गुणस्थानको प्राप्त कर सकता है ।
१५
( २ ) गा० ८८ में जीवसमासोंके भीतर संहननोंका अस्तित्व बतलाया गया है ।
( ३ ) गा० ८९ में विदेह क्षेत्रवाले मनुष्योंके, विद्याधरोंके, म्लेच्छ मनुष्योंके तथा नागेन्द्र पर्वत से परवर्ती क्षेत्रमें रहनेवाले तिर्यंचोंके छहों संहननों का सद्भाव बतलाया गया है ।
( ४ ) गो० कर्मकाण्डको टीकामें यद्यपि अगुरुलघुषट्क, त्रसद्वादशक, स्थावरदशक नामसे सूचित प्रकृतियोंका वर्णन मिलता है । पर गाथाओंमें उनका निर्देश इसी ग्रन्थ में पहली बार देखनेको मिलता है । गुणस्थानों, जीवसमासों एवं मार्गणास्थानोंके भीतर बन्ध, उदय, सत्त्व प्रकृतियोंके निरूपण - कालमें इनका बारबार उपयोग होता है और कण्ठस्थ न रहनेके कारण अभ्यासीको कठिनाईका अनुभव करना पड़ता | किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में गा० ९५ के द्वारा अगुरुलघुषट्क, गा० ९९ के द्वारा त्रसद्वादशक और गा० १०० के द्वारा स्थावरदशकका निरूपण करके ग्रन्थकारने अभ्यासियोंको कण्ठस्थ करनेका सुवर्ण अवसर प्रदान किया है ।
(५) तीर्थंकर प्रकृतिको सत्तावाला जीव कितने भवमै मोक्ष प्राप्त कर लेता है, इसका स्पष्ट निर्देश गा० १५८ में किया गया है, उससे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि जिन जीवोंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया है, वह तीन ( दीक्षा, ज्ञान, निर्वाण ) कल्याणकोंका धारी होकर उसी भवंसे मोक्ष जा सकता है और जिसने मुनि-अवस्था में तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया है, वह ( ज्ञान-निर्वाण ) दो कल्याणकोंका धारक होकर उसी भवसे मुक्त हो जाता है। जो जीव तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करके उसी भवसे मुक्त नहीं हो पाते, वे स्वर्ग या नरक जाकर और वहीं से आकर मनुष्य भवको धारण करके पंच कल्याणकोंका धारी बनकर तीसरे भवमें मोक्ष जाते हैं । इसी गाथामें क्षायिकसम्यक्त्वी जीवको भी मुक्तिका वर्णन किया गया है कि वह अधिक से अधिक तीसरे या चौथे भवमें नियमसे मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।
टीकाकार
प्रकृति बड़ी संस्कृत टीका जो मूल गाथाओंके साथ दी गयी है, उसके रचयिता वस्तुतः श्री सुमति
af ही है, यह बात टीकाके प्रारम्भ में दिये गये द्वितीय मंगल श्लोकसे सिद्ध है । उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने गुरुजनों का स्मरण करते हुए 'विरेन्दुं ज्ञानभूषं हि वन्दे सुमतिकीत्तिकः' कहकर वीरचन्द्र और ज्ञानभूषणकी वन्दना को है और कर्त्ता रूपसे अपने नामका स्पष्ट निर्देश किया है । तथापि टीकाके अन्तमें दी गयी प्रशस्तिके द्वितीय पद्यसे यह भी स्पष्ट रूपसे सिद्ध है कि उन्होंने अपने साथ अपने गुरु ज्ञानभूषणको प्रस्तुत टीकाका रचयिता स्वीकार किया है। वह पद्य इस प्रकार है-
“तदन्वये दयाम्भोधिर्ज्ञानभूषो गुणाकरः ।
atri हि कर्मकाण्डस्य चक्रे सुमतिकीर्त्तियुक् ॥ २॥ "
दोनों पद्योंपर गहराई के साथ विचार करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि टीकाका प्रारम्भ तो सुमतिकीर्तिने ही किया और सम्भवतः अन्त तक उसकी रचना भी की, किन्तु जैसा कि 'ज और ब प्रतिगत विशेषताएँ' शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया गया है— उनके गुरु ज्ञानभूषणने उस टीकाका संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धनादि किया और इसी कारण प्रशस्ति में सुमतिकीर्तिने उक्त प्रकारसे अपने साथ रचयितारूपसे ज्ञानभूषणका भी उल्लेख किया है । यहाँ यह आशंका व्यर्थ है कि सम्भव है - अन्तिम प्रशस्ति ज्ञानभूषण-रचित हो । इसका कारण यह है कि ज्ञानभूषण के लिए जिन 'दयाम्भोधि' और 'गुणाकर' जैसे विशेषणों का प्रयोग किया
Jain Education International.
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org