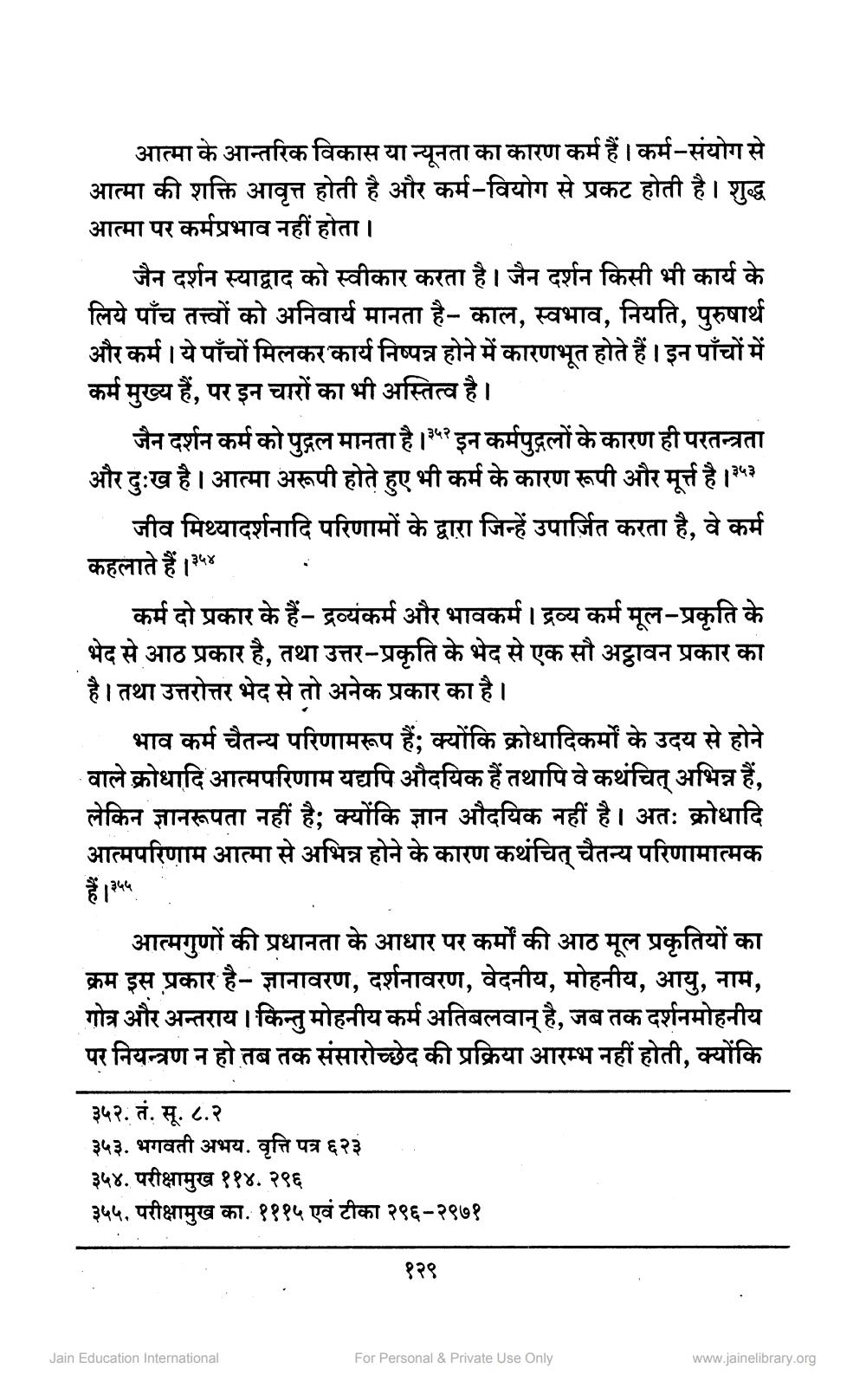________________
आत्मा के आन्तरिक विकास या न्यूनता का कारण कर्म हैं । कर्म-संयोग से आत्मा की शक्ति आवृत्त होती है और कर्म-वियोग से प्रकट होती है। शुद्ध आत्मा पर कर्मप्रभाव नहीं होता।
जैन दर्शन स्याद्वाद को स्वीकार करता है। जैन दर्शन किसी भी कार्य के लिये पाँच तत्त्वों को अनिवार्य मानता है- काल, स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ
और कर्म । ये पाँचों मिलकर कार्य निष्पन्न होने में कारणभूत होते हैं। इन पाँचों में कर्म मुख्य हैं, पर इन चारों का भी अस्तित्व है।
जैन दर्शन कर्म को पुद्गल मानता है ।३५२ इन कर्मपुद्गलों के कारण ही परतन्त्रता और दुःख है । आत्मा अरूपी होते हुए भी कर्म के कारण रूपी और मूर्त है । ३५३ ___ जीव मिथ्यादर्शनादि परिणामों के द्वारा जिन्हें उपार्जित करता है, वे कर्म कहलाते हैं ।३५४ . ___ कर्म दो प्रकार के हैं- द्रव्यंकर्म और भावकर्म । द्रव्य कर्म मूल-प्रकृति के भेद से आठ प्रकार है, तथा उत्तर-प्रकृति के भेद से एक सौ अट्ठावन प्रकार का है। तथा उत्तरोत्तर भेद से तो अनेक प्रकार का है। __भाव कर्म चैतन्य परिणामरूप हैं; क्योंकि क्रोधादिकर्मों के उदय से होने वाले क्रोधादि आत्मपरिणाम यद्यपि औदयिक हैं तथापि वे कथंचित् अभिन्न हैं, लेकिन ज्ञानरूपता नहीं है; क्योंकि ज्ञान औदयिक नहीं है। अतः क्रोधादि आत्मपरिणाम आत्मा से अभिन्न होने के कारण कथंचित् चैतन्य परिणामात्मक हैं।३५५ ___आत्मगुणों की प्रधानता के आधार पर कर्मों की आठ मूल प्रकृतियों का क्रम इस प्रकार है- ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । किन्तु मोहनीय कर्म अतिबलवान् है, जब तक दर्शनमोहनीय पर नियन्त्रण न हो तब तक संसारोच्छेद की प्रक्रिया आरम्भ नहीं होती, क्योंकि
३५२. तं. सू. ८.२ ३५३. भगवती अभय. वृत्ति पत्र ६२३ ३५४. परीक्षामुख ११४. २९६ ३५५, परीक्षामुख का. १११५ एवं टीका २९६-२९७१
-
१२९
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org