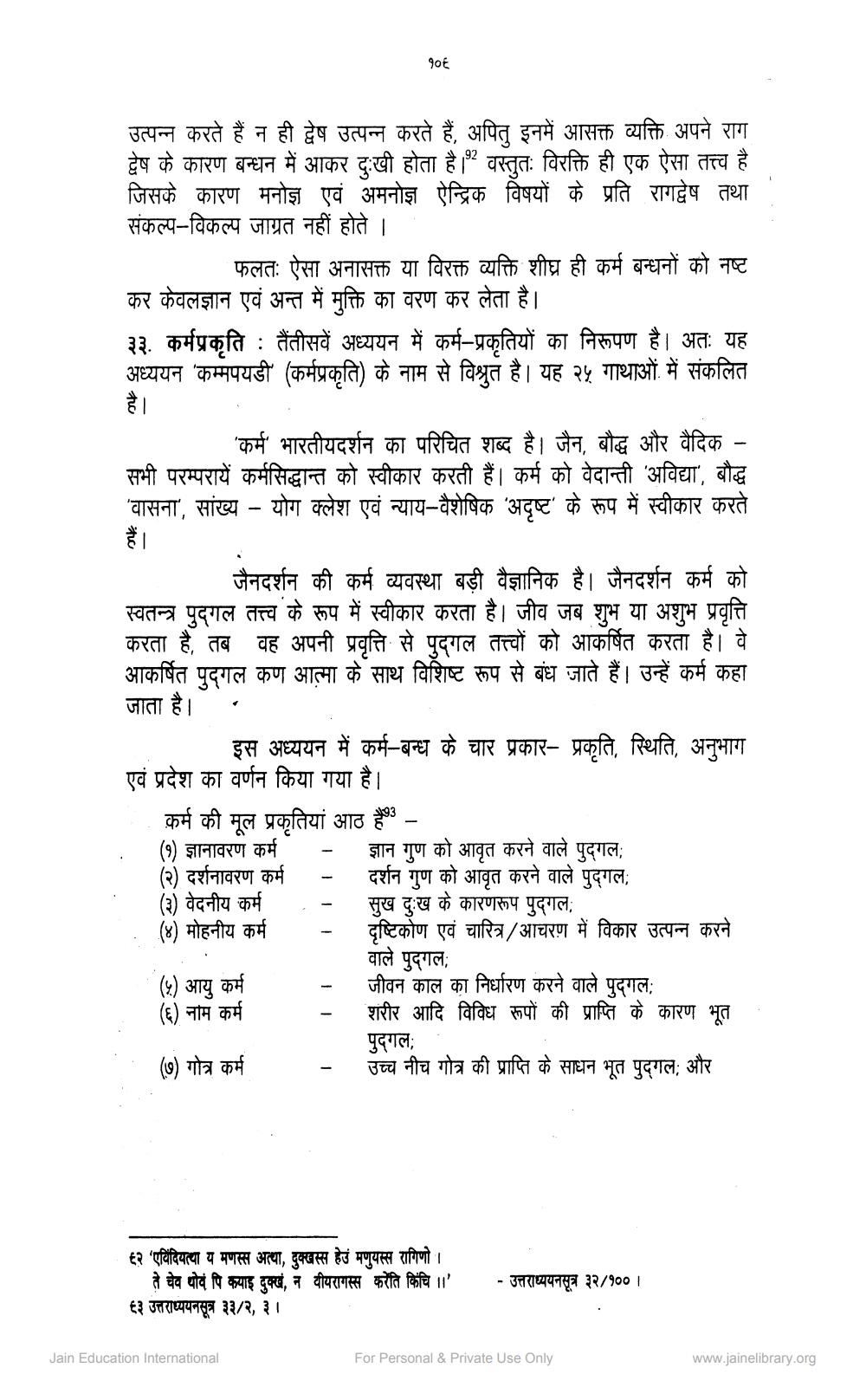________________
उत्पन्न करते हैं न ही द्वेष उत्पन्न करते हैं, अपितु इनमें आसक्त व्यक्ति अपने राग द्वेष के कारण बन्धन में आकर दुःखी होता है।” वस्तुतः विरक्ति ही एक ऐसा तत्त्व है जिसके कारण मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ ऐन्द्रिक विषयों के प्रति रागद्वेष तथा संकल्प - विकल्प जाग्रत नहीं होते ।
फलतः ऐसा अनासक्त या विरक्त व्यक्ति शीघ्र ही कर्म बन्धनों को नष्ट कर केवलज्ञान एवं अन्त में मुक्ति का वरण कर लेता है।
३३. कर्मप्रकृति : तैंतीसवें अध्ययन में कर्म - प्रकृतियों का निरूपण है। अतः यह अध्ययन 'कम्मपयडी' (कर्मप्रकृति) के नाम से विश्रुत है । यह २५ गाथाओं में संकलित है।
१०६
'कर्म' भारतीयदर्शन का परिचित शब्द है। जैन, बौद्ध और वैदिक सभी परम्परायें कर्मसिद्धान्त को स्वीकार करती हैं। कर्म को वेदान्ती 'अविद्या', बौद्ध 'वासना', सांख्य - योग क्लेश एवं न्याय-वैशेषिक 'अदृष्ट' के रूप में स्वीकार करते हैं।
जैनदर्शन की कर्म व्यवस्था बड़ी वैज्ञानिक है। जैनदर्शन कर्म को स्वतन्त्र पुद्गल तत्त्व के रूप में स्वीकार करता है। जीव जब शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करता है, तब वह अपनी प्रवृत्ति से पुद्गल तत्त्वों को आकर्षित करता है। वे आकर्षित पुद्गल कण आत्मा के साथ विशिष्ट रूप से बंध जाते हैं। उन्हें कर्म कहा जाता है।
इस अध्ययन में कर्म-बन्ध के चार प्रकार - प्रकृति, स्थिति, अनुभाग एवं प्रदेश का वर्णन किया गया है।
कर्म की मूल प्रकृतियां आठ
(१) ज्ञानावरण कर्म (२) दर्शनावरण कर्म
(३) वेदनीय कर्म (४) मोहनीय कर्म
(५) आयु कर्म (६) नाम कर्म
(७) गोत्र कर्म
Jain Education International
ज्ञान गुण को आवृत करने वाले पुद्गल; दर्शन गुण
को आवृत करने वाले पुद्गल;
सुख दुःख
कारणरूप पुद्गल;
दृष्टिकोण एवं चारित्र / आचरण में विकार उत्पन्न करने
वाले पुद्गलः
जीवन काल का निर्धारण करने वाले पुद्गल;
शरीर आदि विविध रूपों की प्राप्ति के कारण भूत
पुद्गल;
उच्च नीच गोत्र की प्राप्ति के साधन भूत पुद्गल; और
६२ ‘एविंदियत्था य मणस्स अत्था, दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो । ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्खं न वीयरागस्स करेति किंचि ।।'
६३ उत्तराध्ययनसूत्र ३३ / २, ३ ।
उत्तराध्ययनसूत्र ३२ / १०० |
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org