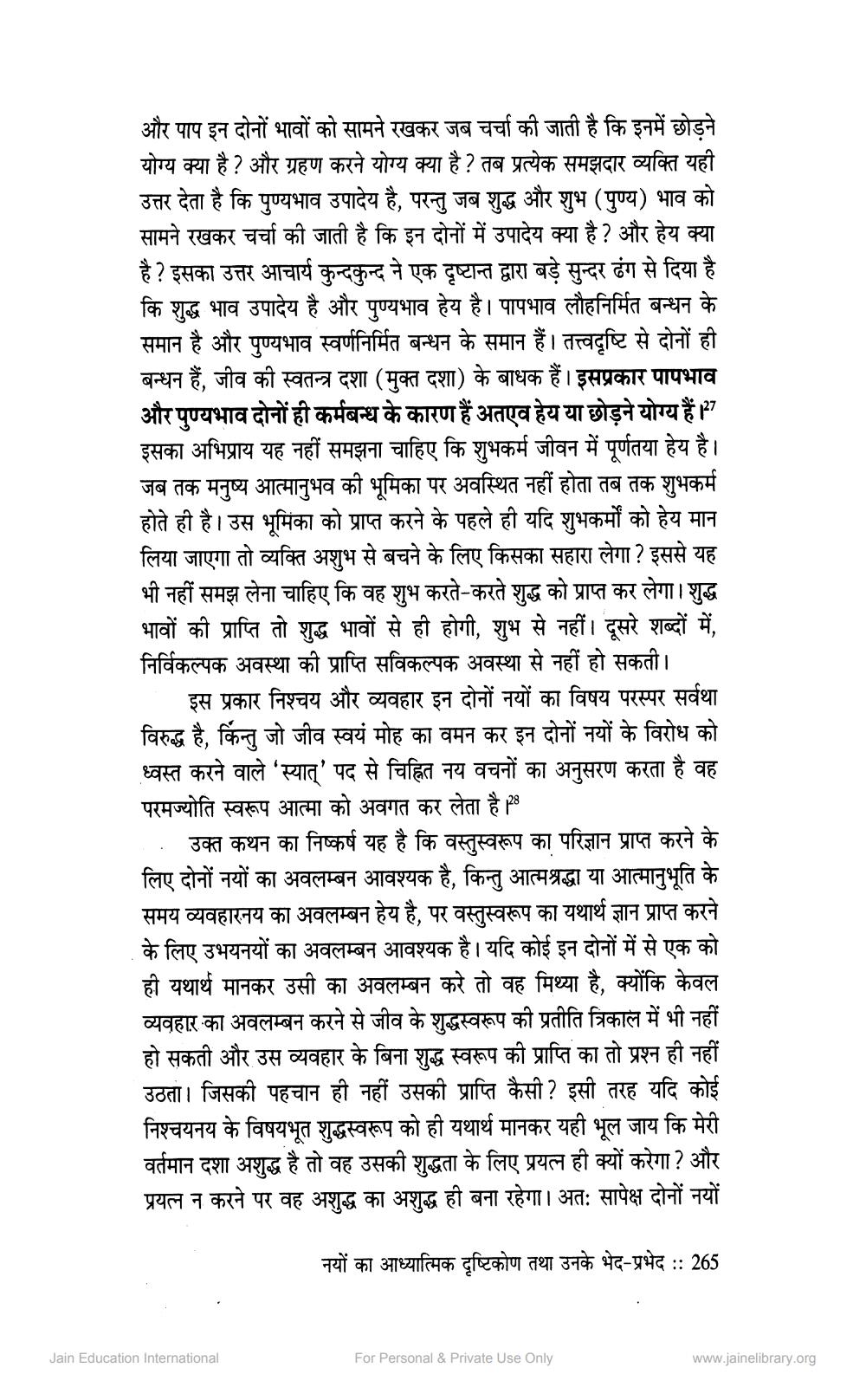________________
और पाप इन दोनों भावों को सामने रखकर जब चर्चा की जाती है कि इनमें छोड़ने योग्य क्या है ? और ग्रहण करने योग्य क्या है ? तब प्रत्येक समझदार व्यक्ति यही उत्तर देता है कि पुण्यभाव उपादेय है, परन्तु जब शुद्ध और शुभ (पुण्य) भाव को सामने रखकर चर्चा की जाती है कि इन दोनों में उपादेय क्या है ? और हेय क्या है ? इसका उत्तर आचार्य कुन्दकुन्द ने एक दृष्टान्त द्वारा बड़े सुन्दर ढंग से दिया है कि शुद्ध भाव उपादेय है और पुण्यभाव हेय है । पापभाव लौहनिर्मित बन्धन के समान है और पुण्यभाव स्वर्णनिर्मित बन्धन के समान हैं । तत्त्वदृष्टि से दोनों ही बन्धन हैं, जीव की स्वतन्त्र दशा (मुक्त दशा) के बाधक हैं । इसप्रकार पापभाव और पुण्यभाव दोनों ही कर्मबन्ध के कारण हैं अतएव हेय या छोड़ने योग्य हैं । 27 इसका अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिए कि शुभकर्म जीवन में पूर्णतया हेय है। जब तक मनुष्य आत्मानुभव की भूमिका पर अवस्थित नहीं होता तब तक शुभकर्म होते ही है। उस भूमिका को प्राप्त करने के पहले ही यदि शुभकर्मों को हेय मान लिया जाएगा तो व्यक्ति अशुभ से बचने के लिए किसका सहारा लेगा? इससे यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि वह शुभ करते-करते शुद्ध को प्राप्त कर लेगा । शुद्ध भावों की प्राप्ति तो शुद्ध भावों से ही होगी, शुभ से नहीं। दूसरे शब्दों में, निर्विकल्पक अवस्था की प्राप्ति सविकल्पक अवस्था से नहीं हो सकती ।
इस प्रकार निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों का विषय परस्पर सर्वथा विरुद्ध है, किन्तु जो जीव स्वयं मोह का वमन कर इन दोनों नयों के विरोध को ध्वस्त करने वाले ‘स्यात्' पद से चिह्नित नय वचनों का अनुसरण करता है वह परमज्योति स्वरूप आत्मा को अवगत कर लेता है 128
उक्त कथन का निष्कर्ष यह है कि वस्तुस्वरूप का परिज्ञान प्राप्त करने के लिए दोनों नयों का अवलम्बन आवश्यक है, किन्तु आत्मश्रद्धा या आत्मानुभूति के समय व्यवहारनय का अवलम्बन हेय है, पर वस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए उभयनयों का अवलम्बन आवश्यक है। यदि कोई इन दोनों में से एक को ही यथार्थ मानकर उसी का अवलम्बन करे तो वह मिथ्या है, क्योंकि केवल व्यवहार का अवलम्बन करने से जीव के शुद्धस्वरूप की प्रतीति त्रिकाल में भी नहीं हो सकती और उस व्यवहार के बिना शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जिसकी पहचान ही नहीं उसकी प्राप्ति कैसी ? इसी तरह यदि कोई निश्चयनय के विषयभूत शुद्धस्वरूप को ही यथार्थ मानकर यही भूल जाय कि मेरी वर्तमान दशा अशुद्ध है तो वह उसकी शुद्धता के लिए प्रयत्न ही क्यों करेगा? और प्रयत्न न करने पर वह अशुद्ध का अशुद्ध ही बना रहेगा। अतः सापेक्ष दोनों नयों
नयों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा उनके भेद-प्रभेद :: 265
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org