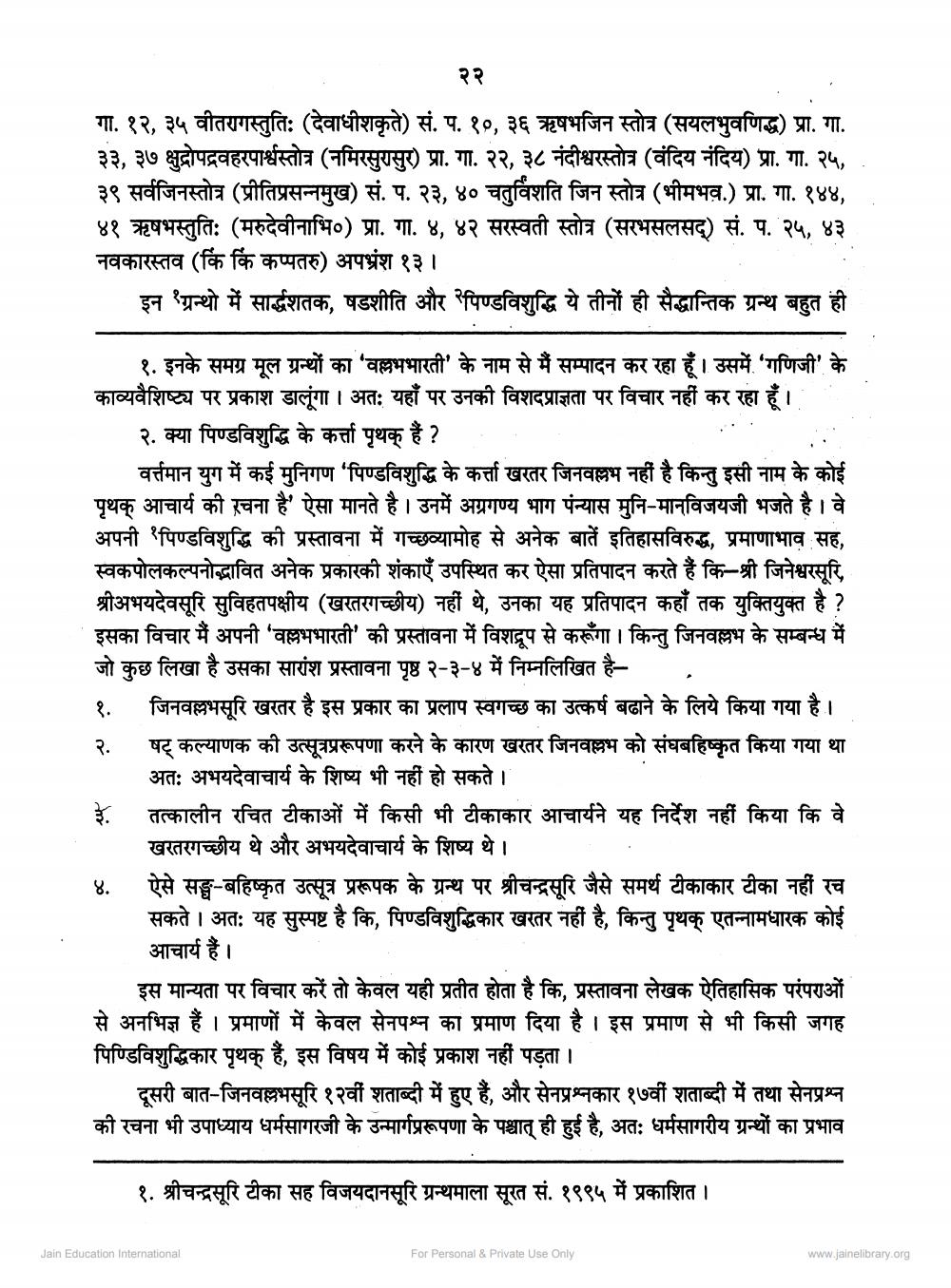________________
२२
गा. १२, ३५ वीतरागस्तुतिः (देवाधीशकृते) सं. प. १०, ३६ ऋषभजिन स्तोत्र (सयलभुवणिद्ध) प्रा. गा. ३३, ३७ क्षुद्रोपद्रवहरपार्श्वस्तोत्र (नमिरसुरासुर) प्रा. गा. २२, ३८ नंदीश्वरस्तोत्र (वंदिय नंदिय) प्रा. गा. २५, ३९ सर्वजिनस्तोत्र (प्रीतिप्रसन्नमुख) सं. प. २३, ४० चतुर्विशति जिन स्तोत्र (भीमभव.) प्रा. गा. १४४, ४१ ऋषभस्तुतिः (मरुदेवीनाभि०) प्रा. गा. ४, ४२ सरस्वती स्तोत्र (सरभसलसद्) सं. प. २५, ४३ नवकारस्तव (किं किं कप्पतरु) अपभ्रंश १३ । ____इन 'ग्रन्थो में सार्द्धशतक, षडशीति और पिण्डविशुद्धि ये तीनों ही सैद्धान्तिक ग्रन्थ बहुत ही
१. इनके समग्र मूल ग्रन्थों का 'वल्लभभारती' के नाम से मैं सम्पादन कर रहा हूँ। उसमें 'गणिजी' के काव्यवैशिष्ट्य पर प्रकाश डालूंगा । अतः यहाँ पर उनकी विशदप्राज्ञता पर विचार नहीं कर रहा हूँ।
२. क्या पिण्डविशुद्धि के कर्ता पृथक् हैं ? ____ वर्तमान युग में कई मुनिगण 'पिण्डविशुद्धि के कर्ता खरतर जिनवल्लभ नहीं है किन्तु इसी नाम के कोई पृथक् आचार्य की रचना है। ऐसा मानते है। उनमें अग्रगण्य भाग पंन्यास मुनि-मानविजयजी भजते है । वे अपनी १पिण्डविशुद्धि की प्रस्तावना में गच्छव्यामोह से अनेक बातें इतिहासविरुद्ध, प्रमाणाभाव सह, स्वकपोलकल्पनोद्भावित अनेक प्रकारकी शंकाएँ उपस्थित कर ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि-श्री जिनेश्वरसूरि, श्रीअभयदेवसूरि सुविहतपक्षीय (खरतरगच्छीय) नहीं थे, उनका यह प्रतिपादन कहाँ तक युक्तियुक्त है ? इसका विचार मैं अपनी 'वल्लभभारती' की प्रस्तावना में विशद्रूप से करूँगा। किन्तु जिनवल्लभ के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसका सारांश प्रस्तावना पृष्ठ २-३-४ में निम्नलिखित है- , १. जिनवल्लभसूरि खरतर है इस प्रकार का प्रलाप स्वगच्छ का उत्कर्ष बढाने के लिये किया गया है। २. षट् कल्याणक की उत्सूत्रप्ररूपणा करने के कारण खरतर जिनवल्लभ को संघबहिष्कृत किया गया था
अतः अभयदेवाचार्य के शिष्य भी नहीं हो सकते। तत्कालीन रचित टीकाओं में किसी भी टीकाकार आचार्यने यह निर्देश नहीं किया कि वे खरतरगच्छीय थे और अभयदेवाचार्य के शिष्य थे। ऐसे सङ्घ-बहिष्कृत उत्सूत्र प्ररूपक के ग्रन्थ पर श्रीचन्द्रसूरि जैसे समर्थ टीकाकार टीका नहीं रच सकते । अत: यह सुस्पष्ट है कि, पिण्डविशुद्धिकार खरतर नहीं है, किन्तु पृथक् एतन्नामधारक कोई आचार्य हैं।
इस मान्यता पर विचार करें तो केवल यही प्रतीत होता है कि, प्रस्तावना लेखक ऐतिहासिक परंपराओं से अनभिज्ञ हैं । प्रमाणों में केवल सेनपश्न का प्रमाण दिया है । इस प्रमाण से भी किसी जगह पिण्डिविशुद्धिकार पृथक् हैं, इस विषय में कोई प्रकाश नहीं पड़ता। __ दूसरी बात-जिनवल्लभसूरि १२वीं शताब्दी में हुए हैं, और सेनप्रश्नकार १७वीं शताब्दी में तथा सेनप्रश्न की रचना भी उपाध्याय धर्मसागरजी के उन्मार्गप्ररूपणा के पश्चात् ही हुई है, अत: धर्मसागरीय ग्रन्थों का प्रभाव
१. श्रीचन्द्रसूरि टीका सह विजयदानसूरि ग्रन्थमाला सूरत सं. १९९५ में प्रकाशित ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org