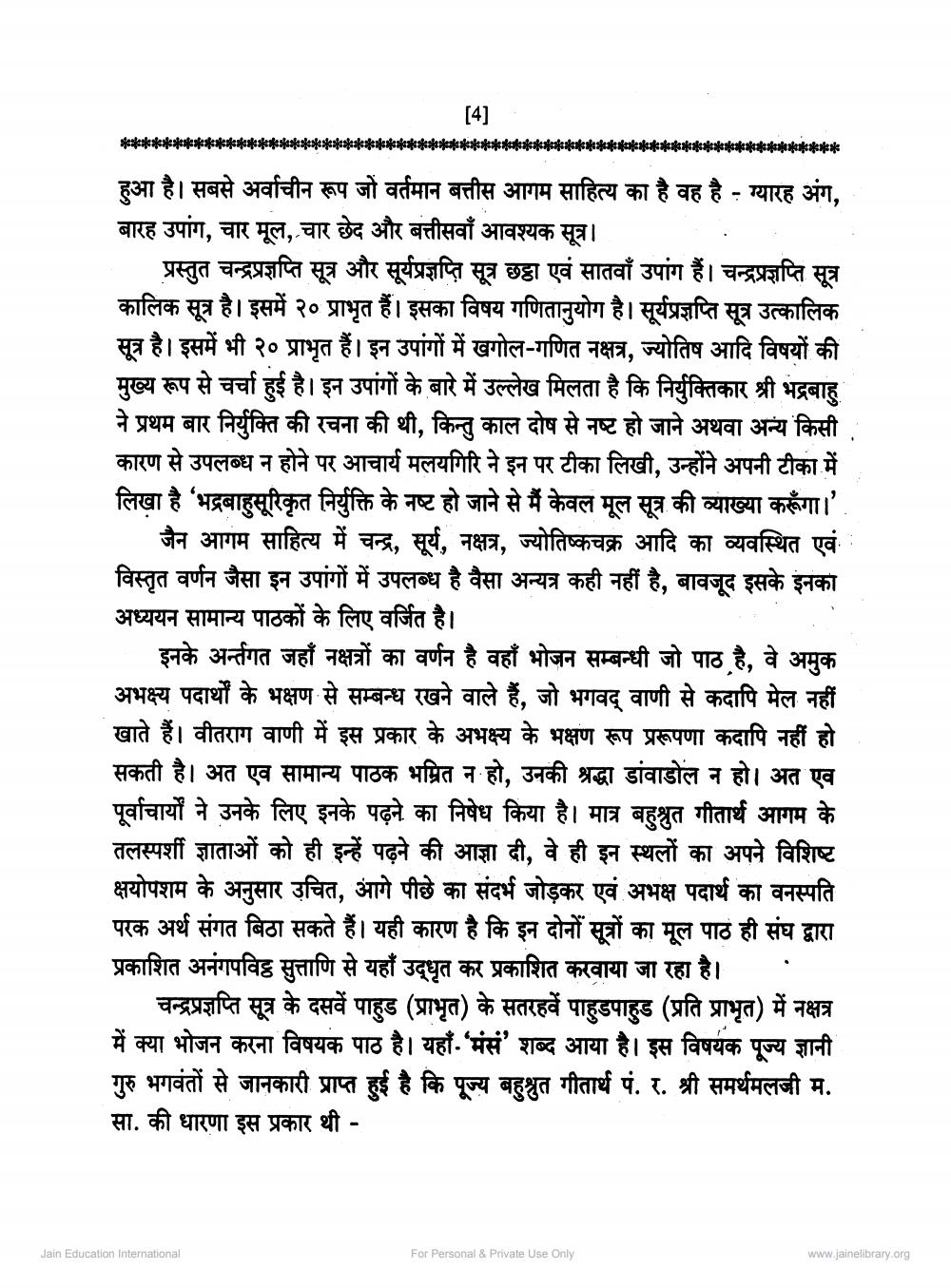________________
[4] 牲本來平平平平平本來來來牛牛牛牛牛****本本中韩将本书本來來來來來粹來本來本中******* हुआ है। सबसे अर्वाचीन रूप जो वर्तमान बत्तीस आगम साहित्य का है वह है - ग्यारह अंग, बारह उपांग, चार मूल, चार छेद और बत्तीसवाँ आवश्यक सूत्र।
प्रस्तुत चन्द्रप्रज्ञप्ति सूत्र और सूर्यप्रज्ञप्ति सूत्र छट्ठा एवं सातवाँ उपांग हैं। चन्द्रप्रज्ञप्ति सूत्र कालिक सूत्र है। इसमें २० प्राभृत हैं। इसका विषय गणितानुयोग है। सूर्यप्रज्ञप्ति सूत्र उत्कालिक सूत्र है। इसमें भी २० प्राभृत हैं। इन उपांगों में खगोल-गणित नक्षत्र, ज्योतिष आदि विषयों की मुख्य रूप से चर्चा हुई है। इन उपांगों के बारे में उल्लेख मिलता है कि नियुक्तिकार श्री भद्रबाहु ने प्रथम बार नियुक्ति की रचना की थी, किन्तु काल दोष से नष्ट हो जाने अथवा अन्य किसी, कारण से उपलब्ध न होने पर आचार्य मलयगिरि ने इन पर टीका लिखी, उन्होंने अपनी टीका में लिखा है 'भद्रबाहुसूरिकृत नियुक्ति के नष्ट हो जाने से मैं केवल मूल सूत्र की व्याख्या करूँगा।'
जैन आगम साहित्य में चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, ज्योतिष्कचक्र आदि का व्यवस्थित एवं विस्तृत वर्णन जैसा इन उपांगों में उपलब्ध है वैसा अन्यत्र कही नहीं है, बावजूद इसके इनका अध्ययन सामान्य पाठकों के लिए वर्जित है।
इनके अर्न्तगत जहाँ नक्षत्रों का वर्णन है वहाँ भोजन सम्बन्धी जो पाठ है, वे अमुक अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण से सम्बन्ध रखने वाले हैं, जो भगवद् वाणी से कदापि मेल नहीं खाते हैं। वीतराग वाणी में इस प्रकार के अभक्ष्य के भक्षण रूप प्ररूपणा कदापि नहीं हो सकती है। अत एव सामान्य पाठक भम्रित न हो, उनकी श्रद्धा डांवाडोल न हो। अत एव पूर्वाचार्यों ने उनके लिए इनके पढ़ने का निषेध किया है। मात्र बहुश्रुत गीतार्थ आगम के तलस्पर्शी ज्ञाताओं को ही इन्हें पढ़ने की आज्ञा दी, वे ही इन स्थलों का अपने विशिष्ट क्षयोपशम के अनुसार उचित, आगे पीछे का संदर्भ जोड़कर एवं अभक्ष पदार्थ का वनस्पति परक अर्थ संगत बिठा सकते हैं। यही कारण है कि इन दोनों सूत्रों का मूल पाठ ही संघ द्वारा प्रकाशित अनंगपविट्ठ सुत्ताणि से यहाँ उद्धृत कर प्रकाशित करवाया जा रहा है। ___चन्द्रप्रज्ञप्ति सूत्र के दसवें पाहुड (प्राभृत) के सतरहवें पाहुडपाहुड (प्रति प्राभृत) में नक्षत्र में क्या भोजन करना विषयक पाठ है। यहाँ. मंसं' शब्द आया है। इस विषयक पूज्य ज्ञानी गुरु भगवंतों से जानकारी प्राप्त हुई है कि पूज्य बहुश्रुत गीतार्थ पं. र. श्री समर्थमलजी म. सा. की धारणा इस प्रकार थी -
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org