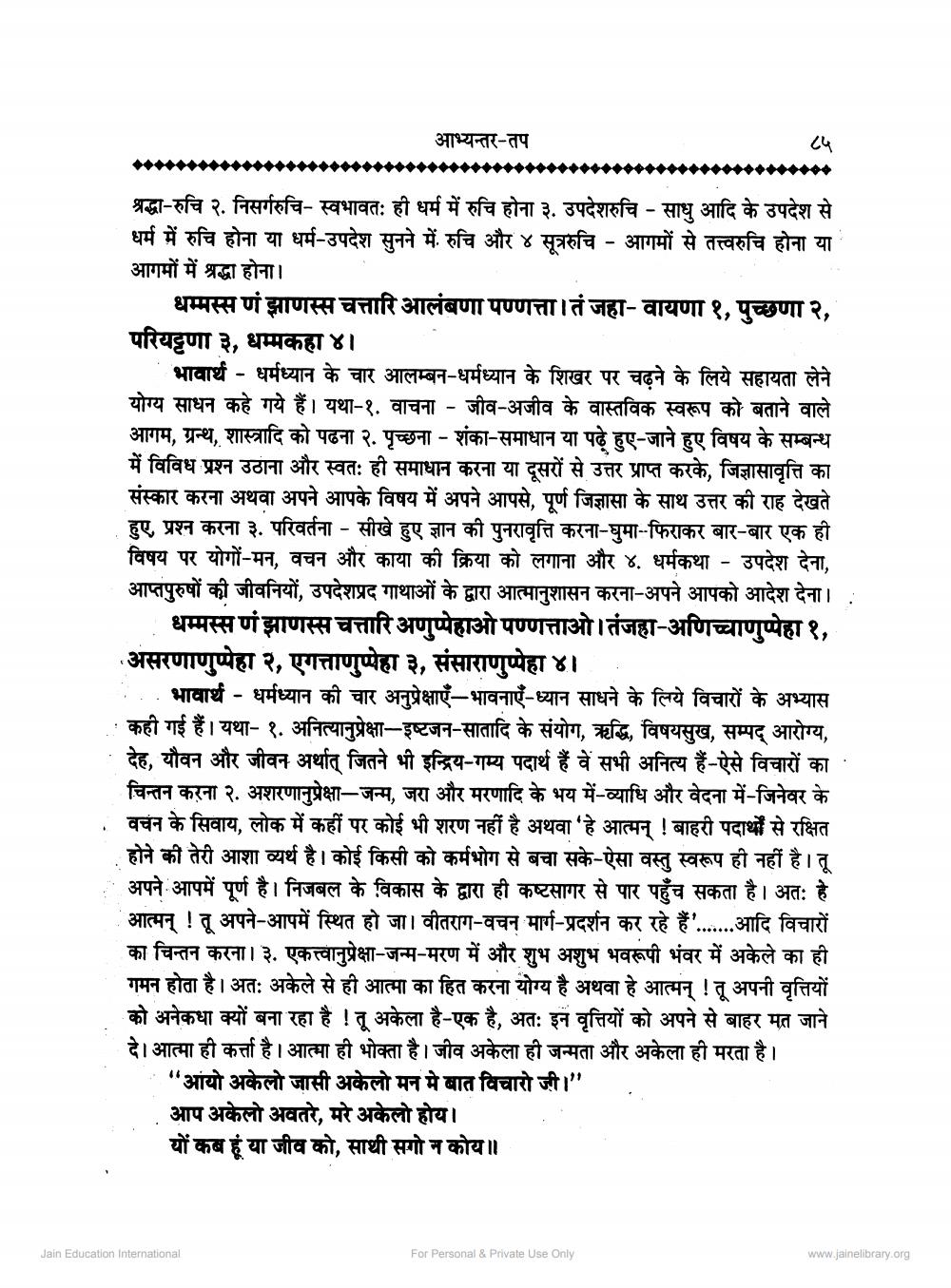________________
आभ्यन्तर-तप
श्रद्धा-रुचि २. निसर्गरुचि- स्वभावतः ही धर्म में रुचि होना ३. उपदेशरुचि - साधु आदि के उपदेश से धर्म में रुचि होना या धर्म-उपदेश सुनने में रुचि और ४ सूत्ररुचि - आगमों से तत्त्वरुचि होना या आगमों में श्रद्धा होना।
धम्मस्स णं झाणस्स चत्तारि आलंबणा पण्णत्ता।तं जहा- वायणा १, पुच्छणा २, परियट्टणा ३, धम्मकहा ४।
भावार्थ - धर्मध्यान के चार आलम्बन-धर्मध्यान के शिखर पर चढ़ने के लिये सहायता लेने योग्य साधन कहे गये हैं। यथा-१. वाचना - जीव-अजीव के वास्तविक स्वरूप को बताने वाले आगम, ग्रन्थ, शास्त्रादि को पढना २. पृच्छना - शंका-समाधान या पढ़े हुए-जाने हुए विषय के सम्बन्ध में विविध प्रश्न उठाना और स्वतः ही समाधान करना या दूसरों से उत्तर प्राप्त करके, जिज्ञासावृत्ति का संस्कार करना अथवा अपने आपके विषय में अपने आपसे, पूर्ण जिज्ञासा के साथ उत्तर की राह देखते हुए, प्रश्न करना ३. परिवर्तना - सीखे हुए ज्ञान की पुनरावृत्ति करना-घुमा-फिराकर बार-बार एक ही विषय पर योगों-मन, वचन और काया की क्रिया को लगाना और ४. धर्मकथा - उपदेश देना, आप्तपुरुषों की जीवनियों, उपदेशप्रद गाथाओं के द्वारा आत्मानुशासन करना-अपने आपको आदेश देना। .
. धम्मस्सणं झाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पण्णत्ताओ।जहा-अणिच्चाणुप्पेहा १, असरणाणुप्पेहा २, एगत्ताणुप्पेहा ३, संसाराणुप्पेहा ४। . . . भावार्थ - धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ-भावनाएँ-ध्यान साधने के लिये विचारों के अभ्यास : कही गई हैं। यथा- १. अनित्यानुप्रेक्षा-इष्टजन-सातादि के संयोग, ऋद्धि, विषयसुख, सम्पद् आरोग्य,
देह, यौवन और जीवन अर्थात् जितने भी इन्द्रिय-गम्य पदार्थ हैं वें सभी अनित्य हैं-ऐसे विचारों का चिन्तन करना २. अशरणानुप्रेक्षा-जन्म, जरा और मरणादि के भय में-व्याधि और वेदना में-जिनेवर के वचन के सिवाय, लोक में कहीं पर कोई भी शरण नहीं है अथवा 'हे आत्मन् ! बाहरी पदार्थों से रक्षित होने की तेरी आशा व्यर्थ है। कोई किसी को कर्मभोग से बचा सके-ऐसा वस्तु स्वरूप ही नहीं है। तू अपने आपमें पूर्ण है। निजबल के विकास के द्वारा ही कष्टसागर से पार पहुंच सकता है। अत: हे आत्मन् ! तू अपने-आपमें स्थित हो जा। वीतराग-वचन मार्ग-प्रदर्शन कर रहे हैं'.......आदि विचारों का चिन्तन करना। ३. एकत्त्वानुप्रेक्षा-जन्म-मरण में और शुभ अशुभ भवरूपी भंवर में अकेले का ही गमन होता है। अतः अकेले से ही आत्मा का हित करना योग्य है अथवा हे आत्मन् ! तू अपनी वृत्तियों को अनेकधा क्यों बना रहा है ! तू अकेला है-एक है, अत: इन वृत्तियों को अपने से बाहर मत जाने दे। आत्मा ही कर्ता है। आत्मा ही भोक्ता है। जीव अकेला ही जन्मता और अकेला ही मरता है।
"आयो अकेलो जासी अकेलो मन मे बात विचारो जी।" . आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होय। यों कब हूं या जीव को, साथी सगो न कोय॥
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org