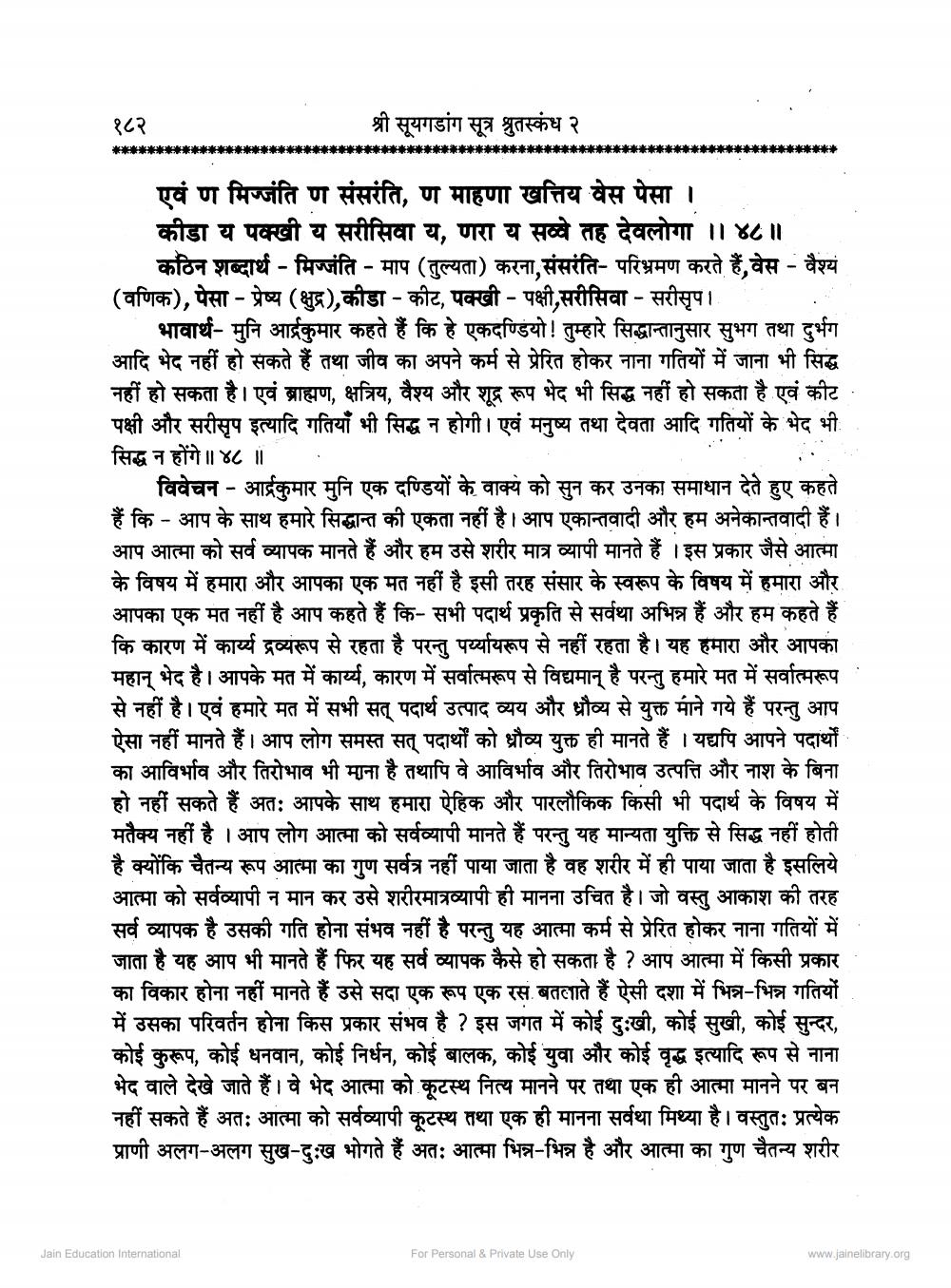________________
१८२
श्री सूयगडांग सूत्र श्रुतस्कंध २
एवं ण मिज्जंति ण संसरंति, ण माहणा खत्तिय वेस पेसा । कीडा य पक्खी य सरीसिवा य, णरा य सव्वे तह देवलोगा ॥४८॥
कठिन शब्दार्थ - मिजंति - माप (तुल्यता) करना, संसरंति- परिभ्रमण करते हैं,वेस - वैश्यं (वणिक), पेसा - प्रेष्य (क्षुद्र),कीडा - कीट, पक्खी - पक्षी,सरीसिवा - सरीसृप।
भावार्थ- मुनि आर्द्रकुमार कहते हैं कि हे एकदण्डियो! तुम्हारे सिद्धान्तानुसार सुभग तथा दुर्भग आदि भेद नहीं हो सकते हैं तथा जीव का अपने कर्म से प्रेरित होकर नाना गतियों में जाना भी सिद्ध नहीं हो सकता है। एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रूप भेद भी सिद्ध नहीं हो सकता है एवं कीट पक्षी और सरीसृप इत्यादि गतियाँ भी सिद्ध न होगी। एवं मनुष्य तथा देवता आदि गतियों के भेद भी सिद्ध न होंगे॥ ४८ ॥
विवेचन - आर्द्रकुमार मुनि एक दण्डियों के वाक्य को सुन कर उनका समाधान देते हुए कहते हैं कि - आप के साथ हमारे सिद्धान्त की एकता नहीं है। आप एकान्तवादी और हम अनेकान्तवादी हैं। आप आत्मा को सर्व व्यापक मानते हैं और हम उसे शरीर मात्र व्यापी मानते हैं । इस प्रकार जैसे आत्मा के विषय में हमारा और आपका एक मत नहीं है इसी तरह संसार के स्वरूप के विषय में हमारा और आपका एक मत नहीं है आप कहते हैं कि- सभी पदार्थ प्रकृति से सर्वथा अभिन्न हैं और हम कहते हैं कि कारण में कार्य द्रव्यरूप से रहता है परन्तु पर्यायरूप से नहीं रहता है। यह हमारा और आपका महान् भेद है। आपके मत में कार्या, कारण में सर्वात्मरूप से विद्यमान् है परन्तु हमारे मत में सर्वात्मरूप से नहीं है। एवं हमारे मत में सभी सत् पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से युक्त माने गये हैं परन्तु आप ऐसा नहीं मानते हैं। आप लोग समस्त सत् पदार्थों को ध्रौव्य युक्त ही मानते हैं । यद्यपि आपने पदार्थों का आविर्भाव और तिरोभाव भी माना है तथापि वे आविर्भाव और तिरोभाव उत्पत्ति और नाश के बिना हो नहीं सकते हैं अतः आपके साथ हमारा ऐहिक और पारलौकिक किसी भी पदार्थ के विषय में मतैक्य नहीं है । आप लोग आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं परन्तु यह मान्यता युक्ति से सिद्ध नहीं होती है क्योंकि चैतन्य रूप आत्मा का गुण सर्वत्र नहीं पाया जाता है वह शरीर में ही पाया जाता है इसलिये आत्मा को सर्वव्यापी न मान कर उसे शरीरमात्रव्यापी ही मानना उचित है। जो वस्तु आकाश की तरह सर्व व्यापक है उसकी गति होना संभव नहीं है परन्तु यह आत्मा कर्म से प्रेरित होकर नाना गतियों में जाता है यह आप भी मानते हैं फिर यह सर्व व्यापक कैसे हो सकता है ? आप आत्मा में किसी प्रकार का विकार होना नहीं मानते हैं उसे सदा एक रूप एक रस. बतलाते हैं ऐसी दशा में भिन्न-भिन्न गतियों में उसका परिवर्तन होना किस प्रकार संभव है ? इस जगत में कोई दुःखी, कोई सुखी, कोई सुन्दर, कोई कुरूप, कोई धनवान, कोई निर्धन, कोई बालक, कोई युवा और कोई वृद्ध इत्यादि रूप से नाना भेद वाले देखे जाते हैं। वे भेद आत्मा को कूटस्थ नित्य मानने पर तथा एक ही आत्मा मानने पर बन नहीं सकते हैं अतः आत्मा को सर्वव्यापी कूटस्थ तथा एक ही मानना सर्वथा मिथ्या है। वस्ततः प्रत्येक प्राणी अलग-अलग सुख-दुःख भोगते हैं अतः आत्मा भिन्न-भिन्न है और आत्मा का गुण चैतन्य शरीर
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org