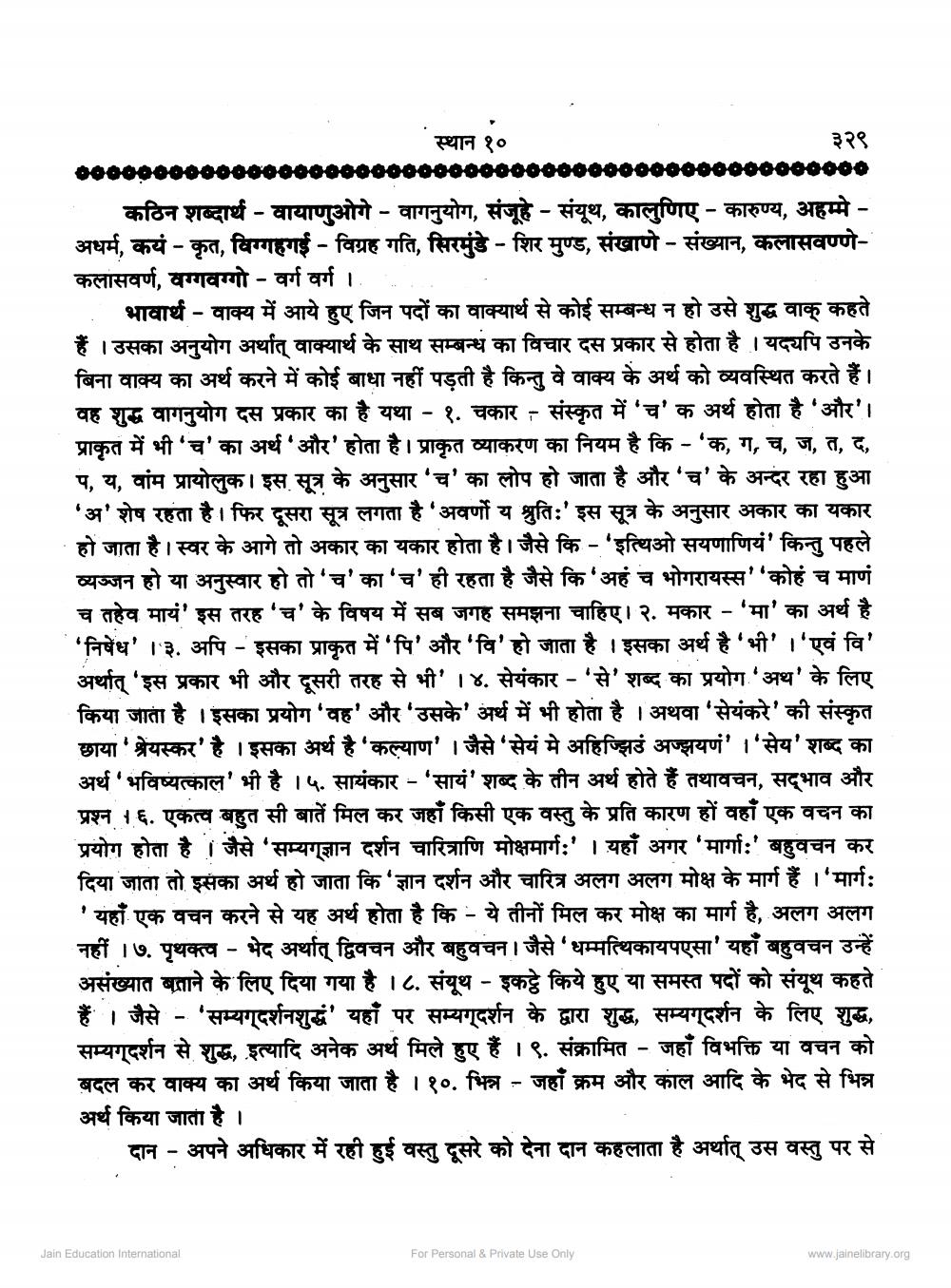________________
स्थान १०
३२९
कठिन शब्दार्थ - वायाणुओगे - वागनुयोग, संजूहे - संयूथ, कालुणिए - कारुण्य, अहम्मे - अधर्म, कयं - कृत, विग्गहगई - विग्रह गति, सिरमुंडे - शिर मुण्ड, संखाणे - संख्यान, कलासवण्णेकलासवर्ण, वग्गवग्गो - वर्ग वर्ग । .
भावार्थ - वाक्य में आये हुए जिन पदों का वाक्यार्थ से कोई सम्बन्ध न हो उसे शुद्ध वाक् कहते हैं । उसका अनुयोग अर्थात् वाक्यार्थ के साथ सम्बन्ध का विचार दस प्रकार से होता है । यदयपि उनके बिना वाक्य का अर्थ करने में कोई बाधा नहीं पड़ती है किन्तु वे वाक्य के अर्थ को व्यवस्थित करते हैं। वह शुद्ध वागनुयोग दस प्रकार का है यथा - १. चकार - संस्कृत में 'च' क अर्थ होता है 'और'। प्राकृत में भी 'च' का अर्थ 'और' होता है। प्राकृत व्याकरण का नियम है कि - 'क, ग, च, ज, त, द, प, य, वांम प्रायोलुक। इस सूत्र के अनुसार 'च' का लोप हो जाता है और 'च' के अन्दर रहा हुआ 'अ' शेष रहता है। फिर दूसरा सूत्र लगता है 'अवर्णो य श्रुतिः' इस सूत्र के अनुसार अकार का यकार हो जाता है। स्वर के आगे तो अकार का यकार होता है। जैसे कि - 'इथिओ सयणाणियं' किन्तु पहले व्यञ्जन हो या अनुस्वार हो तो 'च' का 'च' ही रहता है जैसे कि 'अहं च भोगरायस्स' 'कोहं च माणं च तहेव माय' इस तरह 'च' के विषय में सब जगह समझना चाहिए। २. मकार - 'मा' का अर्थ है 'निषेध' । ३. अपि - इसका प्राकृत में 'पि' और 'वि' हो जाता है । इसका अर्थ है 'भी' । 'एवं वि' अर्थात् 'इस प्रकार भी और दूसरी तरह से भी' । ४. सेयंकार - 'से' शब्द का प्रयोग अथ' के लिए किया जाता है । इसका प्रयोग 'वह' और 'उसके' अर्थ में भी होता है । अथवा 'सेयंकरे' की संस्कृत छाया 'श्रेयस्कर' है । इसका अर्थ है 'कल्याण' । जैसे 'सेयं मे अहिज्झिउं अज्झयणं' । 'सेय' शब्द का अर्थ 'भविष्यत्काल' भी है । ५. सायंकार - 'सायं' शब्द के तीन अर्थ होते हैं तथावचन, सद्भाव और प्रश्न १६. एकत्व बहुत सी बातें मिल कर जहाँ किसी एक वस्तु के प्रति कारण हों वहाँ एक वचन का प्रयोग होता है । जैसे 'सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्षमार्गः' । यहाँ अगर 'मार्गाः' बहुवचन कर दिया जाता तो इसका अर्थ हो जाता कि 'ज्ञान दर्शन और चारित्र अलग अलग मोक्ष के मार्ग हैं । 'मार्गः ' यहाँ एक वचन करने से यह अर्थ होता है कि - ये तीनों मिल कर मोक्ष का मार्ग है, अलग अलग नहीं । ७. पृथक्त्व - भेद अर्थात् द्विवचन और बहुवचन । जैसे 'धम्मत्थिकायपएसा' यहाँ बहुवचन उन्हें असंख्यात बताने के लिए दिया गया है । ८. संयूथ - इकट्ठे किये हुए या समस्त पदों को संयूथ कहते हैं । जैसे - 'सम्यग्दर्शनशुद्ध' यहाँ पर सम्यग्दर्शन के द्वारा शुद्ध, सम्यग्दर्शन के लिए शुद्ध, सम्यग्दर्शन से शुद्ध, इत्यादि अनेक अर्थ मिले हुए हैं । ९. संक्रामित - जहाँ विभक्ति या वचन को बदल कर वाक्य का अर्थ किया जाता है । १०. भिन्न - जहाँ क्रम और काल आदि के भेद से भिन्न अर्थ किया जाता है।
दान - अपने अधिकार में रही हुई वस्तु दूसरे को देना दान कहलाता है अर्थात् उस वस्तु पर से
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org