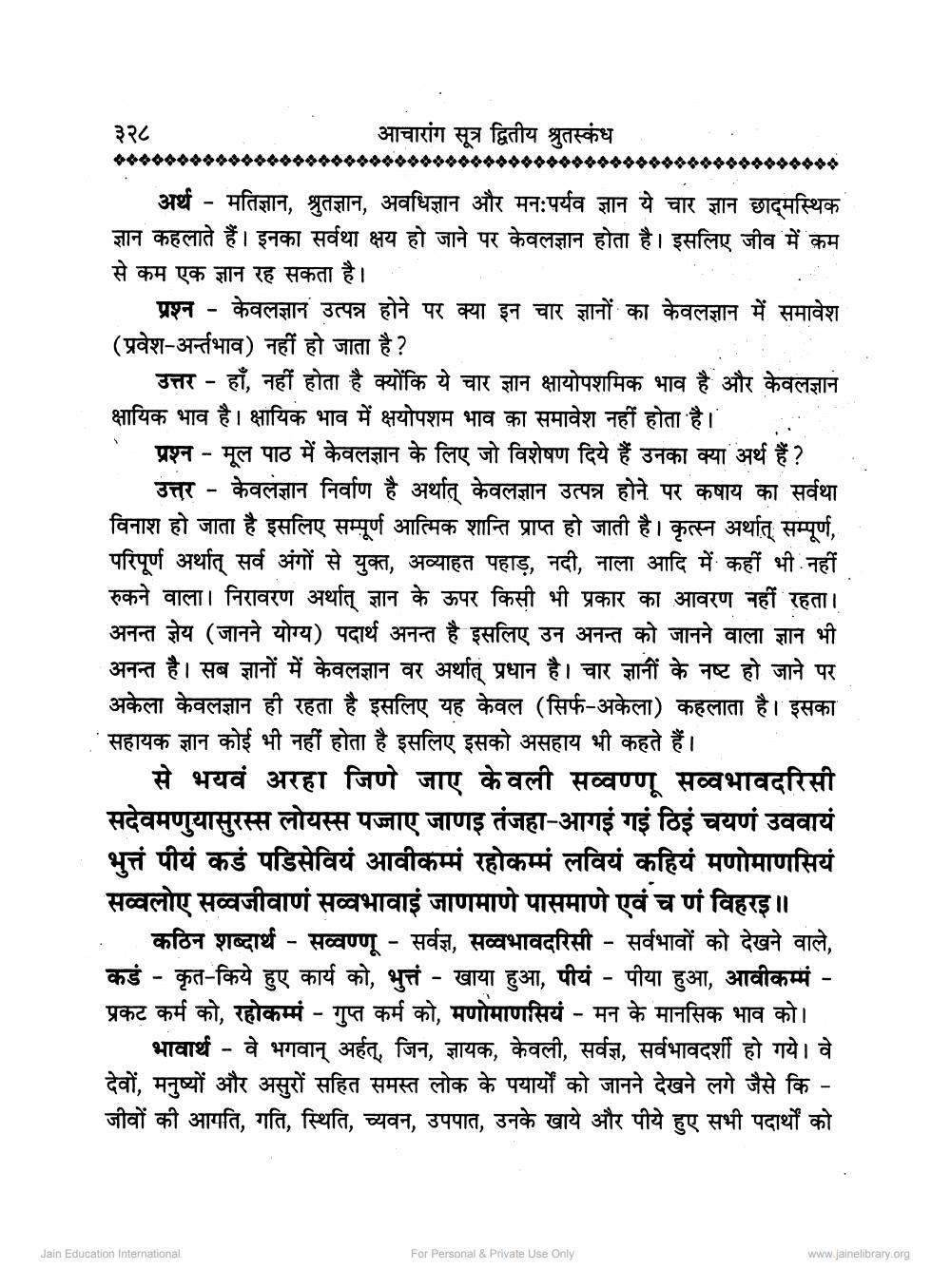________________
३२८
आचारांग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कंध .000000000000000000..................................
अर्थ - मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यव ज्ञान ये चार ज्ञान छाद्मस्थिक ज्ञान कहलाते हैं। इनका सर्वथा क्षय हो जाने पर केवलज्ञान होता है। इसलिए जीव में कम से कम एक ज्ञान रह सकता है।
प्रश्न - केवलज्ञान उत्पन्न होने पर क्या इन चार ज्ञानों का केवलज्ञान में समावेश (प्रवेश-अतभाव) नहीं हो जाता है ?
उत्तर - हाँ, नहीं होता है क्योंकि ये चार ज्ञान क्षायोपशमिक भाव है और केवलज्ञान क्षायिक भाव है। क्षायिक भाव में क्षयोपशम भाव का समावेश नहीं होता है। ____ प्रश्न - मूल पाठ में केवलज्ञान के लिए जो विशेषण दिये हैं उनका क्या अर्थ हैं?
उत्तर - केवलज्ञान निर्वाण है अर्थात् केवलज्ञान उत्पन्न होने पर कषाय का सर्वथा विनाश हो जाता है इसलिए सम्पूर्ण आत्मिक शान्ति प्राप्त हो जाती है। कृत्स्न अर्थात् सम्पूर्ण, परिपूर्ण अर्थात् सर्व अंगों से युक्त, अव्याहत पहाड़, नदी, नाला आदि में कहीं भी नहीं रुकने वाला। निरावरण अर्थात् ज्ञान के ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं रहता। अनन्त ज्ञेय (जानने योग्य) पदार्थ अनन्त है इसलिए उन अनन्त को जानने वाला ज्ञान भी अनन्त है। सब ज्ञानों में केवलज्ञान वर अर्थात् प्रधान है। चार ज्ञानी के नष्ट हो जाने पर अकेला केवलज्ञान ही रहता है इसलिए यह केवल (सिर्फ-अकेला) कहलाता है। इसका सहायक ज्ञान कोई भी नहीं होता है इसलिए इसको असहाय भी कहते हैं।
से भयवं अरहा जिणे जाए के वली सव्वण्णू सव्वभावदरिसी सदेवमणुयासुरस्स लोयस्स पज्जाए जाणइ तंजहा-आगई गई ठिइं चयणं उववायं भुत्तं पीयं कडं पडिसेवियं आवीकम्मं रहोकम्मं लवियं कहियं मणोमाणसियं सव्वलोए सव्वजीवाणं सव्वभावाइं जाणमाणे पासमाणे एवं च णं विहरइ॥ .. कठिन शब्दार्थ - सव्वण्णू - सर्वज्ञ, सव्वभावदरिसी - सर्वभावों को देखने वाले,
कडं - कृत-किये हुए कार्य को, भुत्तं - खाया हुआ, पीयं - पीया हुआ, आवीकम्मं - प्रकट कर्म को, रहोकम्मं - गुप्त कर्म को, मणोमाणसियं - मन के मानसिक भाव को।
भावार्थ - वे भगवान् अर्हत्, जिन, ज्ञायक, केवली, सर्वज्ञ, सर्वभावदर्शी हो गये। वे देवों, मनुष्यों और असुरों सहित समस्त लोक के पयार्यों को जानने देखने लगे जैसे कि - जीवों की आगति, गति, स्थिति, च्यवन, उपपात, उनके खाये और पीये हुए सभी पदार्थों को
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org