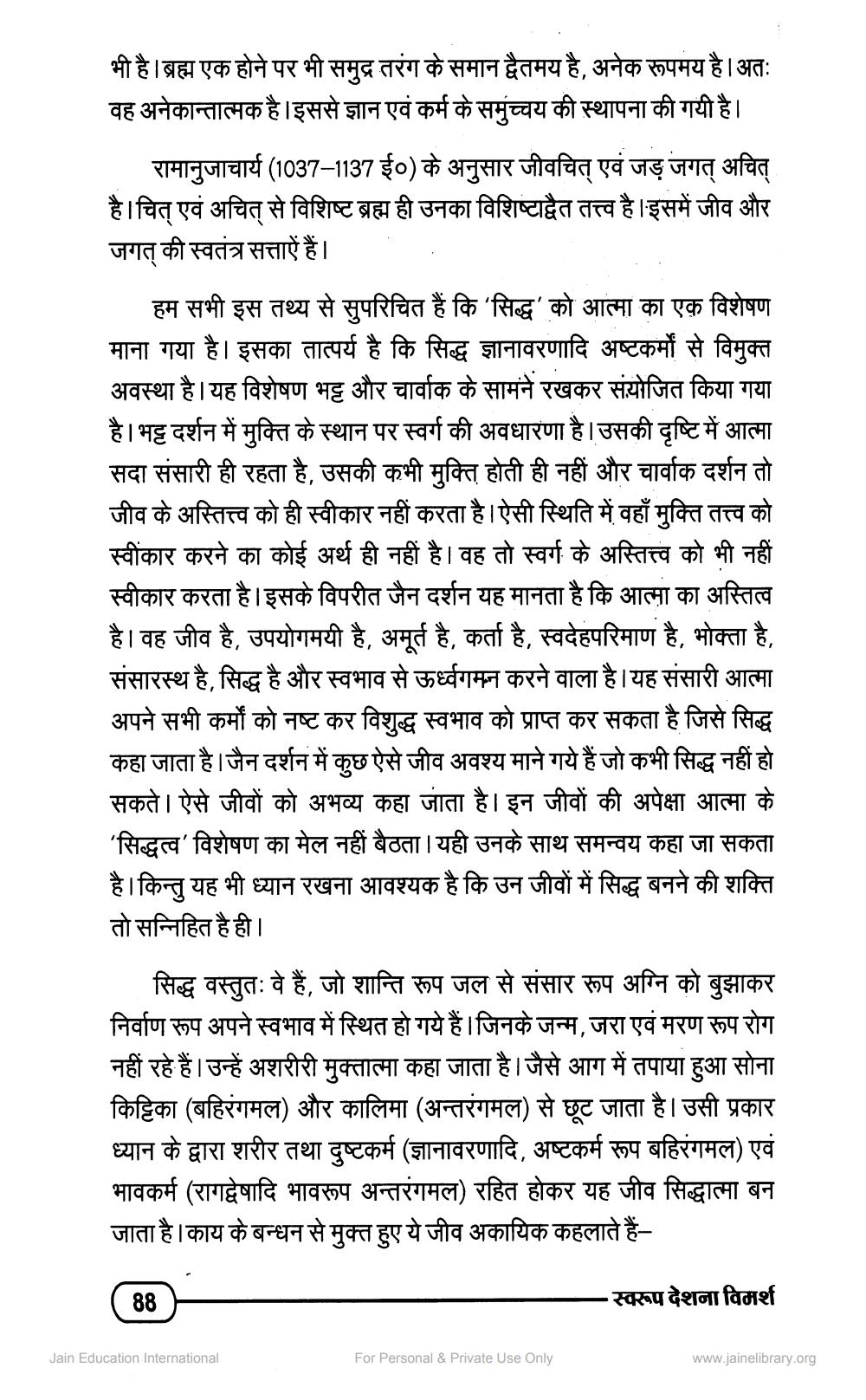________________
भी है। ब्रह्म एक होने पर भी समुद्र तरंग के समान द्वैतमय है, अनेक रूपमय है। अतः वह अनेकान्तात्मक है। इससे ज्ञान एवं कर्म के समुच्चय की स्थापना की गयी है।
रामानुजाचार्य (1037-1137 ई०) के अनुसार जीवचित् एवं जड़ जगत् अचित् है। चित् एवं अचित् से विशिष्ट ब्रह्म ही उनका विशिष्टाद्वैत तत्त्व है। इसमें जीव और जगत् की स्वतंत्र सत्ताएं हैं।
हम सभी इस तथ्य से सुपरिचित हैं कि 'सिद्ध' को आत्मा का एक विशेषण माना गया है। इसका तात्पर्य है कि सिद्ध ज्ञानावरणादि अष्टकर्मों से विमुक्त अवस्था है। यह विशेषण भट्ट और चार्वाक के सामने रखकर संयोजित किया गया है। भट्ट दर्शन में मुक्ति के स्थान पर स्वर्ग की अवधारणा है। उसकी दृष्टि में आत्मा सदा संसारी ही रहता है, उसकी कभी मुक्ति होती ही नहीं और चार्वाक दर्शन तो जीव के अस्तित्त्व को ही स्वीकार नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वहाँ मुक्ति तत्त्व को स्वीकार करने का कोई अर्थ ही नहीं है। वह तो स्वर्ग के अस्तित्त्व को भी नहीं स्वीकार करता है। इसके विपरीत जैन दर्शन यह मानता है कि आत्मा का अस्तित्व है। वह जीव है, उपयोगमयी है, अमूर्त है, कर्ता है, स्वदेहपरिमाण है, भोक्ता है, संसारस्थ है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। यह संसारी आत्मा अपने सभी कर्मों को नष्ट कर विशुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर सकता है जिसे सिद्ध कहा जाता है। जैन दर्शन में कुछ ऐसे जीव अवश्य माने गये हैं जो कभी सिद्ध नहीं हो सकते। ऐसे जीवों को अभव्य कहा जाता है। इन जीवों की अपेक्षा आत्मा के 'सिद्धत्व' विशेषण का मेल नहीं बैठता । यही उनके साथ समन्वय कहा जा सकता है। किन्तु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उन जीवों में सिद्ध बनने की शक्ति तो सन्निहित है ही।
सिद्ध वस्तुतः वे हैं, जो शान्ति रूप जल से संसार रूप अग्नि को बुझाकर निर्वाण रूप अपने स्वभाव में स्थित हो गये हैं। जिनके जन्म, जरा एवं मरण रूप रोग नहीं रहे हैं। उन्हें अशरीरी मुक्तात्मा कहा जाता है। जैसे आग में तपाया हुआ सोना किट्टिका (बहिरंगमल) और कालिमा (अन्तरंगमल) से छूट जाता है। उसी प्रकार ध्यान के द्वारा शरीर तथा दुष्टकर्म (ज्ञानावरणादि, अष्टकर्म रूप बहिरंगमल) एवं भावकर्म (रागद्वेषादि भावरूप अन्तरंगमल) रहित होकर यह जीव सिद्धात्मा बन जाता है। काय के बन्धन से मुक्त हुए ये जीव अकायिक कहलाते हैं
-स्वरूप देशना विमर्श
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org